प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन | Class 10Th Chemistry Chapter – 6 Notes | Model Question Paper | प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन Solutions
प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन | Class 10Th Chemistry Chapter – 6 Notes | Model Question Paper | प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन Solutions
प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन (Management of Natural Resources)
स्मरणीय तथ्य : एक दृष्टिकोण
(MEMORABLE FACTS: ATA GLANCE)
- मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंध सुधार की प्रक्रिया पर्यावरण प्रबंधन है।
- पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है, प्राकृतिक संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग, उनकी सुरक्षा एवं उनका संवर्द्धन।
- कम उपयोग, पुन: उपयोग एवं पुनः चक्रण’ की नीति अपनाकर हमें पर्यावरण पर पड़नेवाले दबाव को कम कर सकते हैं।
- अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में जिन्होंने लगभग 300 साल पहले दुर्लभ ‘खेजरी’ पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर 363 लोगों के साथ जान दी थी, भारत सर में जीव संरक्षण हेतु ‘अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार’ की व्यवस्था की है।
- कोयला, पेट्रोलियम एवं तेल जीवाश्म ईंधन के प्रकार हैं जो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। संसार में जीवाश्म ईंधनों के भंडार सीमित हैं, अतः इनके विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है।
- चिपको आंदोलन पेड़ के काटे जाने के विरोध में किया गया था।
- स्रोत पर उपयोग कम करके, जहाँ संभव हो सके वहाँ पुनर्चालन और पुनरूपयोग करके तथा कचरा का सही निष्पादन करके पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है।
- जल में उपस्थित मल के कॉलिफॉर्म सूक्ष्मजीवों की संख्या को नदी के प्रदूषण का मानदंड माना गया।
- जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल यातायात तथा उद्योग के लिए किया जाता है।
- वनों की सघनता घटने तथा उनके क्षेत्रफल के कम होने से वन्य प्राणी संकट में है।
- वन हमारे आर्थिक विकास के साधन मात्र ही नहीं बल्कि प्राणियों के अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होते हैं।
- 1992 में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन निर्माताओं के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड जैसे—युरो – I तथा 1995 में युरो-II लागू किया गया था।
- औद्योगिक क्रांति तथा जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधन (जल, वन, वन्यजीव, कोयला, पेट्रोलियम आदि) क्षीण होने से हम सबों का ध्यान इनके संरक्षण एवं प्रबंधन की ओर आकृष्ट हुआ है।
- वन कटाई से हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण (प्रकाश संश्लेषण के लिए) की क्षमता घट जाती है। प्रकाशसंश्लेषण की दर घटने से पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
- क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था।
- ऋषिकेश से कोलकाता तक गंगा नदी को स्वच्छ करने के लक्ष्य से गंगा कार्यान्वयन योजना की शुरुआत की गई थी ।
- कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन की मात्रा पृथ्वी के अंदर सीमित है। अतएव जीवाश्म ईंधन की खपत सावधानीपूर्वक करनी चाहिए ।
- वर्षाजल के सामान्य उपयोग के लिए, भूमिगत जल स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए तथा जल के संरक्षण के लिए किए जाने वाले संग्रहण को जल संचयन कहते हैं ।
- उन क्षेत्रों में जहाँ जल की कमी होती है वहाँ ड्रिप इरिगेशन या बूँद-बूँद सिंचाई तकनीक अपनायी जाती है।
- गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रीत (सौर, ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि) का उपयोग अधिक-से-अधिक होना चाहिए।
- वातावरण के जैविक, भौतिक, रासायनिक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। मुख्यतः प्रदूषण तीन प्रकार का होता है – भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण ।
- वन सम्पदा का प्रबंधन सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए।
अभ्यासार्थ प्रश्न
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
I. सही उत्तर का संकेताक्षर ( क, ख, ग या घ) लिखे।
1. बाँध बनाने का मुख्य कारण है
(क) पीने का जल उपलब्ध कराना
(ख) बिजली उत्पन्न करना
(ग) वर्षा जल के बहाव को रोकना
(घ) इनमें कोई नहीं
उत्तर – (ख)
2. वर्षा जल का संचयन कहलाता है
(क) भूमिगत जल का परिपूरण
(ख) जल शोधन
(ग) जल संचयन
(घ) इनमें कोई नहीं
उत्तर – (ग)
3. यूरो-II का संबंध है
(क) मृदा प्रदूषण से
(ख) वायु प्रदूषण से
(ग) जल प्रदूषण से
(घ) इनमें कोई नहीं
उत्तर – (ख)
4. वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है
(क) वनों का इस्तेमाल नहीं करके
(ख) बाढ़ रोककर
(ग) पेड़ लगाकर
(घ) पेड़ काटकर
उत्तर – (ग)
5. विश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था ?
(क) मेधा पाटकर
(ख) अमृता देवी विश्नोई
(ग) गंगा राम विश्नोई
(घ) महाराजा अभय सिंह
उत्तर – (ख)
6. निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है ?
(क) लकड़ी
(ख) मिट्टी
(ग) पवन
(घ) पत्थर
उत्तर – (ग)
7. चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था
(क) मिट्टी के अपरदन को रोकना
(ख) वन कटाई को रोकना
(ग) जल प्रदूषण को रोकना
(घ) बिजली उत्पादन
उत्तर – (ख)
8. कोयला तथा पेट्रोलियम है
(क) नाभिकीय ईंधन
(ख) जीवाश्म ईंधन
(ग) नवीकरणीय ईंधन
(घ) बायोगैस ईंधन
उत्तर – (ख)
9. बड़े-बड़े बाँधों से होता है
(क) गरीबी
(ख) सूखा
(ग) वनों का विकास
(घ) सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता
उत्तर – (घ)
10. क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था ?
(क) ओजोन
(ख) कार्बन डाइऑक्साइड
(ग) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
(घ) सल्फर डाइऑक्साइड
उत्तर – (ख)
11. सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुँचाने की विधि कहलाता है
(क) यांत्रिक छिड़काव
(ख) टपकन सिंचाई
(ग) वर्षा जल से सिंचाई
(घ) नहर से सिंचाई
उत्तर – (ख)
12. इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है ?
(क) पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी
(ख) वनरोपण
(ग) हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग
(घ) इनमें सभी
उत्तर – (घ)
13. निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है ?
(क) अधिक हरे पौधों का उगना
(ख) वनरोपण
(ग) जैवविविधता
(घ) बढ़ती मानव जनसंख्या
उत्तर – (घ)
14. गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत
(क) कोयला
(ख) पेट्रोल
(ग) डीजल
(घ) पवन ऊर्जा
उत्तर – (घ)
II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
1.वन …………. संसाधने है।
उत्तर – नवीकरणीय
2. कोयला तथा पेट्रोलियम ………..प्राकृतिक संसाधन हैं।
उत्तर – अनवीकरणीय
3. भारत में वर्षा सभी जगहों पर ……… रूप से नहीं होती।
उत्तर – समान
4. प्रदूषण फैलानेवाले पदार्थ ……….. कहलाते हैं।
उत्तर – प्रदूषक
5. ………… से बचाने के लिए नदी पर बाँध बनाए जाते हैं।
उत्तर – बाढ़
6. बाँध का जल आसपास के ……….. में फैलकर भारी तबाही करता है।
उत्तर – क्षेत्र
7. बाँध के जल का समता और ………… से वितरण नहीं हो पाता।
उत्तर – न्याय
8. राजस्थान के ……. ग्राम में पेड़ों से चिपककर स्त्रियों ने वनकटाई के विरोध में जान दे दी थी ।
उत्तर – खेजरी
9. रसोईघर के नम कचरों का पुनर्चालन कर ……….. बनाया जाता है।
उत्तर – कम्पोस्ट
10 ………. ऊर्जा का निरंतर स्रोत है।
उत्तर – सूर्य
11. बायोगैस का उपयोग ……… के रूप में किया जाता है ।
उत्तर – ईंधन
12. कोयला तथा पेट्रोलियम ……….. ईंधन कहलाते हैं।
उत्तर – जीवाश्म
III. सही / गलत का चयन करें।
1. इंदिरा गाँधी नहर ने दिल्ली को हरित किया है।
उत्तर – गलत
2. चिपको आंदोलन का समर्थन सुन्दर लाल बहुगुणा ने किया था।
उत्तर – सही
3. वनों द्वारा वर्षा की मात्रा में कमी होती है।
उत्तर – गलत
4. वन मिट्टी कटाव को रोकने में सहायक होता है।
उत्तर – सही
5. ग्रीनहाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होता है।
उत्तर – सही
6. गंगा नदी को इलाहाबाद से कोलकाता तक स्वच्छ बनाने के लक्ष्य से गंगा कार्यान्वयन योजना को लागू किया गया था।
उत्तर – गलत
7. रसोईघर के नम कचरों का पुनर्चालन कर कम्पोस्ट बनाया जाता है।
उत्तर – सही
8. हमें जैवअनिम्नीकरणीय (non-biodegradable) वस्तुओं के उपयोग से बचना चाहिए।
उत्तर – सही
9. जहाँ जल की कमी होती है वहाँ ड्रिप इरिगेशन सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
उत्तर – गलत
10. कॉलिफॉर्म जीवाणुओं की वृद्धि से पेट और आंत के रोग होते हैं।
उत्तर – सही
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर
1. चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे ?
उत्तर – चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुन्दरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे।
2. ऊर्जा के दो परम्परागत स्रोतों के नाम लिखें।
उत्तर – ऊर्जा के दो परम्परागत स्रोत निम्न हैं- (1) कोयला (ii) पेट्रोलियम ।
3. ह्रास हुए भूमिगत जल का पुनः परिपूरण किससे होता है ?
उत्तर – ह्रास हुए भूमिगत जल का पुनः परिपूरण वर्षा जल से होता है।
4. जल उपलब्धता में गिरावट के क्या कारण हैं ?
उत्तर – जल की उपलब्धता में कमी का मुख्य कारण जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव है।
5. पृथ्वी पर ग्रीनहाउस प्रभाव डालनेवाली सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस कौन-सी है ?
उत्तर – पृथ्वी पर ग्रीनहाउस प्रभाव डालने वाली सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) है।
6. पुनर्चालन के एक लाभ बताएँ।
उत्तर – नम कचरों का पुनर्चालन कर कम्पोस्ट बनाते हैं जिसका जैविक खाद के रूप में उपयोग होता है।
7. कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए।
उत्तर – कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमें उनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि उनकी गुणवत्ता एवं उपलब्धता बनी रहे तथा विकास कार्य भी न रुके साथ ही पर्यावरण भी संतुलित बना रहे ।
8. ऊर्जा के दो गैर-परंपरागत स्रोतों के नाम लिखें।
उत्तर – ऊर्जा के दो गैर-परंपरागत स्रोत ये हैं
(i) सौर ऊर्जा (Solar energy )
(ii) पवन ऊर्जा (Wind energy ) ।
9. चिपको आंदोलन का लक्ष्य क्या था ?
उत्तर – चिपको आंदोलन का लक्ष्य वनों के विनाश को रोककर वनों का संरक्षण करना था।
10. भारत के दो राष्ट्रीय उद्यानों का नाम बताएँ।
उत्तर – भारत के दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम निम्न हैं- (i) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (ii) कान्हा नेशनल पार्क।
11. दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताएँ।
उत्तर – दो जीवाश्म ईंधनों के नाम हैं- (i) कोयला (ii) पेट्रोलियम ।
12. रसोईघर के नम कचरों का पुनर्चालन कर क्या बनाया जाता है ?
उत्तर – कम्पोस्ट बनाया जा सकता है।
13. जल की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई की कौन-सी तकनीक अपनायी जाती है।
उत्तर – ड्रिप इरिगेशन या बूँद-बूँद सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
14. क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया या था ?
उत्तर – कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लिए बनाया गया था।
15. भूमिगत जल स्तर तक वर्षाजल को पहुँचाने के लिए की गई दो व्यवस्थाओं नाम बताएँ।
उत्तर – भूमिगत जल स्तर तक वर्षाजल को पहुँचाने के लिए ‘बोर वेल’ (bore well) एवं ‘डग वेल’ (dug well) व्यवस्थाएँ की जाती हैं। Come
16. अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है ?
उत्तर – किसी वस्तु का कमी, पुनर्चालन तथा पुनरूपयोग अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा है।
17. प्लैस्टिक के थैलों के बदले में किस प्रकार के थैले इस्तमाल की जानी चाहिए ?
उत्तर – प्लैस्टिक के थैलों के बदले जूट या कपड़ों से बने थैले का इस्तेमाल करना चाहिए ।
लघु उत्तरीय प्रश्न
1. ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है
उत्तर – वैसे क्षेत्र जहाँ जल अपर्याप्त होते हैं अर्थात बारिश की कमी होती है वहाँ सिंचाई की समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि भारत में अधिकतम सिंचाई वर्षा के जल अथवा बारिश से होती है। उन क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ वर्षा के जल का संरक्षण कर उसका अधिकतम उपयोग किया जाता है। इस संरक्षित जल को खेतों में पानी के फव्वारों अथवा बूँद-बूँद करके सिंचाई की जाती है। इसलिए इस विधि को ड्रिप सिंचाई या बूँद-बूंद सिंचाई व्यवस्था कहा जाता है।
2. जल संचयन क्या है ?
उत्तर – धरातलीय तथा भूमिगत जल भंडारों में जल की कभी काफी अधिक हो गई है। भूमिगत जल का निष्कासन अधिकतम सीमा से ज्यादा होने से तथा उस अनुपात में उसका पुनः परिपूरण नहीं होने से भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। भूमिगत जल का परिपूरण वर्षा जल से होता है। वर्षा जल के अधिक से अधिक उपयोग और संचयन कर भूमिगत जल स्तर को बनाये रख सकते हैं। हमें नदियों, तालाबों, गडढों आदि में पानी का संचयन करना चाहिए। इनके संचयन से भूमिगत जल का भंडारण अधिक होगा। वर्षा के दिनों में वर्षा जल का अधिक उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार भूमिगत जल के स्तर को बनाये रखना जल संचयन कहलाता है।
3. कूड़े-कचरों का पुनर्चालन से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर – प्लास्टिक, कागज, काँच, धातु के टुकड़े आदि यानी कूड़े-कचरों का पुनर्चालन आसानी से किया जा सकता है। इन वस्तुओं को गलाकर नई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। रसोई घर के नम कचरे का पुनर्चालन कर कम्पोस्ट बनाते हैं जिसका जैविक खाद के रूप में उपयोग होता है। कुछ सूखे कचरों का पुनर्चालन कर नई वस्तुएँ प्राप्त करते हैं। धातुओं के कचरे को अलग-अलग छाँटकर पुनर्चालन कर संबंधित धातु के सामान बनाये जाते हैं। बड़े-बड़े शहरों में ऐसे कचरे के पुनर्चालन करने वाले बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ संचालित हैं।
4. वाहनों के लिये उत्सर्जन संबंधी मानदण्ड क्या हैं?
उत्तर – वाहनों की भारी संख्या और यातायात वाले कुछ शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि पायी गयी है। जैसे—दिल्ली तथा कोलकाता के कुछ क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने वाहनों को वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में एक बताया है। इस कारण 1989 में केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम को संशोधित किया गया। इस संशोधन के बाद वाहन मालिकों के लिये धुएँ के उत्सर्जन संबंधी नियम अधिसूचित किये गये और 1991 में पहली बार वाहन निर्माताओं के लिये उत्सर्जन संबंधी मानदण्ड, जैसे— युरो- I (Euro-I) लागू किया गया। इन मानदण्डों को 2000 में फिर संशोधित कर युरो-II (Euro-II) लागू किया गया जिससे दिल्ली तथा अन्य शहरों में ईंधन के दहन से निकले गैसों की मात्रा में कमी आयी है, तथा वायु की गुणवत्ता बढ़ी है जिससे पर्यावरण पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है।
5. वन तथा वन्यजीव हमारे लिये किस प्रकार से लाभदायक हैं ?
उत्तर – वन तथा वन्यजीव हमारे लिये बहुत ही लाभदायक हैं। इससे हमारा अस्तित्व है। वनों से हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे—आवास निर्माण सामग्री, ईंधन त तथा भोजन का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपूर्ति करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हमें वनों से कंद-मूल, फल-फूल इत्यादि चीज़ों की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर वन्यजीव हमारे जीवन को सुखमय बनाने में अपना योगदान देते हैं। इनसे हमारा मनोरंजन होता है। इनको चिड़ियाघरों या अभ्यारण्यों में रखकर विदेशी पर्यटकों या देशी पर्यटकों को लुभाया जाता है। इनसे हमें खाल, दाँत, सींग, कस्तूरी आदि जैसे बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती है। कुछ लोग वन्यजीव को अपना व्यवसाय बना चुके हैं जिससे उनका और उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। लिये बहुत ही उपयोगी
अतः इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वन तथा वन्यजीव हमारे होते हैं। इनसे हमारा जीवन खुशहाल और सुखमय बना रहता है। इसलिये इनका संरक्षण करना आवश्यक है।
6. वन एवं वन्यजीव के संरक्षण के उपायों का उल्लेख करें।
उत्तर – वन्य सम्पदा या वन की सुरक्षा के अग्रलिखित उपाय हैं- 1. वृक्षों का काटना बन्द होना चाहिए। 2. केवल वे ही वृक्ष काटे जाएँ जो सूख जाएँ या जिन्हें कोई गंभीर बीमारी लग जाए और उनके स्थान पर नये वृक्ष लगाये जाने चाहिए। 3. वृक्षों की प्रति वर्ष गिनती की जानी चाहिए और वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए। 4. वन महोत्सव मनाया जाना चाहिए। यह हमारे देश की वृक्षारोपण की परम्परा है जिसके अनुसार वन महोत्सव में हजारों नये वृक्ष लगाये जाते हैं। 5. नये लगाये गये वृक्षों की देखभाल करनी चाहिए। 6. पुनर्वनरोपण की योजना लागू होनी चाहिए। 7. वन सम्पदा को दावानल से बचाने के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। वृक्षों को बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए।
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीव का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित दो उपाय किए जा सकते हैं-
1. सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे शिकारियों को प्रतिबन्धित वन्य पशु का शिकार करने पर दंड मिलना चाहिए।
2. राष्ट्रीय पार्क और पशु-पक्षी विहार स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ पर वन्य पशु सुरक्षित रह सकें।
7. चिपको आन्दोलन पर टिप्पणी लिखें।
उत्तर – आज भी तेजी से वनों का कटाव जारी है। वनों के कटाव से जंगली जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जंगल के तेजी करने से मानव को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल के पहाड़ों पर स्थित रेनी ग्राम में इमारती लकड़ी के ठेकेदारों के हाथों वनों का विनाश रोकने के लिए स्थानीय स्त्रियों ने पेड़ों से चिपक कर एक जन-आन्दोलन किया था। इसी तरह राजस्थान के खेजरी ग्राम में पेड़ों से चिपककर स्त्रियों के जान देने की घटना की याद में लोगों ने इस आन्दोलन को चिपको आन्दोलन का नाम दिया। इस आन्दोलन का समर्थन जाने-माने समाजसेवी सुन्दरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने किया। वन विनाश के विरोध में इनके कार्यकर्त्ताओं ने हिमालय क्षेत्र में लम्बी-लम्बी पद यात्राएँ कीं। इसने वन काटने वाले ठेकेदारों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी वनों के महत्व को समझाया।
8. जल संचयन क्यों जरूरी है ?
उत्तर – जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकीकरण के कारण धरातलीय तथा भूमिगत जल के भंडारों में जल की कमी हो गयी है। इस कारण जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गयी है। बड़ी आबादी को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए जल संचयन आवश्यक है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट के कारण जलीय जीवों के साथ-साथ स्थलीय जीवों पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। हमें जल संग्रहण एवं संचयन के लिए आगे बढ़कर कार्य करना होगा। इसके लिए वनों, तालाबों, नदियों आदि को संरक्षित करना होगा। ताकि जल-स्तर बना रहे। पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जल संचयन आवश्यक है।
9. बाँध से क्या लाभ होता है ? बतायें।
उत्तर – बाँध सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को ही बरकरार नहीं रखता बल्कि इससे बिजली भी उत्पन्न की जाती है। सिंचाई के लिए बाँध के जल को नहर द्वारा दूर-दूर तक ले जाया जाता है। उदाहरण के लिए ‘इंदिरा गाँधी’ नहर ने राजस्थान के बड़े क्षेत्र को हरित किया है। यद्यपि बाँध के जल से सिंचाई व्यवस्था सुधरी है तथापि बाँध के जल का समता और न्याय से वितरण नहीं हो पाता। बाँध के नजदीक बसे लोग धान व ईख की खेती कर जल का अधिक-से-अधिक उपयोग कर लेते हैं तथा बाँध से दूर विस्थापित लोगों को बाँध का जल नहीं मिल पाता। कभी-कभार बड़े-बड़े बाँध के निर्माण के विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे देश की दो विवादास्पद परियोजनाएँ हैं-टिहरी बाँध परियोजना एवं सरदार सरोवर बाँध परियोजना।
10. बाँध से क्या हानि होती हैं ? बतायें।
उत्तर – बाँध से बहुत अधिक हानि होती है। बाँध के निर्माण के फलस्वरूप हजारों लोगों को पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में बसना पड़ता है। पर्वतीय लोगों को पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्रों में बसना पड़ता है जिससे उनकी जीवन-शैली में परिवर्तन आता है और उन लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विस्थापितों को जल, लकड़ी, फल अपेक्षाकृत महँगे मिलने लगते हैं तथा सरकार द्वारा समुचित मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। बाँध के टूटने पर आस-पास के क्षेत्रों में जल फैलकर भारी तबाही मचाता है जिससे लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार बाँध से बहुत सारी हानियाँ होती हैं।
11. ” चिपको आन्दोलन” क्या है ? हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिये ?
उत्तर – चिपको आन्दोलन- वनों की अत्यधिक कटाई होने के कारण 1970 के दशक में उत्तराखण्ड के गढ़वाल के पहाड़ों पर स्थित रेनी ग्राम में इमारती लकड़ी ठेकेदारों के हाथों वनों का विनाश रोकने के लिये स्थानीय स्त्रियों ने पेड़ों से चिपक कर एक जन-आन्दोलन किया था। इसी तरह राजस्थान के खेजरी ग्राम में पैड़ों से चिपककर स्त्रियों के जान देने की घटना की याद में लोगों ने इस आन्दोलन को चिपको आन्दोलन का नाम दिया। इस आन्दोलन के समर्थक जाने-माने समाजसेवी सुन्दरलाल बहुगुणा और चण्डी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने किया। उस समय इस आन्दोलन ने जनवादी रूप ले लिया था। लोग इकट्ठे होकर नारा देने लगे और दोषियों को सजा दिलाने की माँग करने लगे। इस प्रकार उनका चिपको आन्दोलन सफल हुआ और प्रकृति का संरक्षण हुआ।
वनों का संरक्षण–वनों का संरक्षण हमें निम्नलिखित कारणों से करना चाहिये—
- वनों से हमें फल, मेवे, सब्जियाँ तथा औषधियाँ प्राप्त होती हैं।
- हमें वर्ना से इमारती लकड़ी तथा जलानेवाली लकड़ी (ईंधन) प्राप्त होती है।
- वन पर्यावरण में गैसीय सन्तुलन बनाने में सहयोग देते हैं।
- वृक्षों के वन्यजीव भागों से पर्याप्त मात्रा में जल का वाष्पन होता है जो वर्षा के एक स्रोत का कार्य करते हैं।
- ये मृदा अपरदन एवं बाढ़ पर नियंत्रण करने में सहायक होते हैं।
- वन वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं।
- ये धन प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं।
12. अपनी आयु के विद्यार्थियों की जीवन-शैली के परिवर्तन में आप कौन-से चार सुझाव देना चाहेंगे जिससे हमारे उपलब्ध संसाधनों के संपोषण को प्रोत्साहन मिल सके।
उत्तर – छात्र स्वयं करें।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
1. जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिये क्या किया जाना चाहिये ?
उत्तर – जल जीवजंतु एवं पेड़-पौधों के जीवन के पोषण का मुख्य आधार है। इसके अभाव में जीवन संभव नहीं है। इसी कारण जल को जीवन सार ( essence of life) कहते हैं। हमारे दैनिक कार्य जैसे-स्नान, बरतन, कपड़े धोने व पीने तथा भोजन पकाने, जल के उपयोग के साथ ही प्रारंभ होते हैं। हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएँ, जैसे— भोजन का पचना, रक्त संचार, मलोत्सर्ग आदि जल की सहायता से ही पूरी होती है। पेड़-पौधों के जीवन में जल बीजों के अंकुरण से लेकर उनकी वृद्धि तक में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा आधुनिक समय में तकनीकी विकास के कारण जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल यातायात तथा उद्योग आदि के लिए किया जाता रहा है। जल की माँग में काफी वृद्धि हुई है, परंतु उसकी उपलब्धता में कमी आई है।
जल की उपलब्धता में कमी का मुख्य कारण उसके संरक्षण एवं प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव है। अतः, जल संसाधन का उपयोग सुनियोजित ढंग से करके तथा जलस्रोतों का उचित प्रबंधन करके हम जल प्रणाली का संरक्षण कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य पीने तथा सिंचाई के लिए जल भंडार (बाँध), तालाब व बावड़ी बनाता आ रहा है। भूमिगत जल स्तर बनाए रखने के लिए मानव छोटे-छोटे मिट्टी के बाँध बनाकर, खाई बनाकर, बालू एवं संगमरमर से जलाशय बनाकर तथा मकान के छत पर जल संचयन तंत्र लगाकर जल का संचयन करते आ रहा है। घरों में जल संरक्षण के बड़े सचेष्ट प्रयास किए जाते थे तथा उसके दुरूपयोग को रोका जाता था। आज भी जल-संचयन की प्राचीन पद्धति को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। साथ ही, कृषि के प्रसार और हरित क्रांति के लिए बड़े-बड़े बाँध बनाने की भी आवश्यकता है। सिंचाई के लिए बाँध के जल को नहर द्वारा दूर-दूर तक ले जाया जाता है। बाँध सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को ही बरकरार नहीं रखता बल्कि इससे बिजली भी उत्पन्न की जाती है। बाँध के जल का वितरण समता एवं न्यायपूर्ण तरीके से करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से मिल सके।
2. वनों के ह्रास के कारणों का उल्लेख करें।
उत्तर – वन हमारे जीवन के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। इससे हमें बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति होती है। इसके अभाव में हमारा जीवन शून्य हो जाता है।
वैनों के हास के कारण–वनों के ह्रास के निम्नलिखित कारण हैं-
- आधुनिकीकरण- आज का मानव विलासी होता जा रहा है। उसे हर तरह की ऐशो-आराम की जरूरत होती है। वह विलासितापूर्ण वस्तुओं को अधिक पसंद करता है। वह अच्छे-से-अच्छे मकानों में रहना पसंद करता है। इन सभी जरूरतों की पूर्ति करने के लिये वनों की कटाई करनी पड़ती है जिससे वनों का ह्रास होता है।
- जनसंख्या की वृद्धि – जनसंख्या की वृद्धि ने भी वनों के ह्रास को प्रोत्साहित किया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों की कटाई की जा रही है। आज मनुष्यों की आबादी इतनी बढ़ रही है कि मनुष्य वनों को काटने पर अमादा है जिससे वनों का ह्रास होता है।
- जलावन का अत्यधिक उपयोग- जलावन के व्यापक प्रयोग ने वनों के ह्रास को निश्चित किया है। लोग जलावन के लिये अधिक-से-अधिक वनों को काटते हैं जिससे वनों का ह्रास होना तय है।
- खनन कार्य — खनन कार्य के लिये भी वनों को काटा जा रहा है। खनिजों की प्राप्ति के लिये लोग वनों को काटते जा रहे हैं। इसके कारण वनों का ह्रास हो रहा है।
- बाँधों का निर्माण- बाँधों के निर्माण ने भी वनों को काटने पर मजबूर किया है। बाँधों के निर्माण से नदियों के पानी को नियंत्रित किया जाता है। इसके निर्माण के लिये लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। बाँधों की लकड़ियों की प्राप्ति के लिये वनों को काटा जा रहा है। जिससे वनों का ह्रास होता है।
- अवैधानिक रूप से जंगलों की कटाई- वनों को काटने के गैर-कानूनी ढंग से भी वनों के ह्रास को बल प्रदान किया है। बहुत सारे लोग कुछ रुपयों की लालच में चोरी-छिपे वनों को काटते हैं जिससे वनों की संख्या घटती है और वनों का ह्रास होता है।
- कागज की बढ़ती माँग- आज का मानव शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दे रहा है। सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ा-लिखाकर एक इन्सान बनाना चाहते हैं। इसी कारण कागजों की माँग बढ़ती जा रही है। बढ़ती कागजों की माँग के कारण वनों को काटा जा रहा है जिससे वनों का ह्रास दोनों तय है।
इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं जो वनों की ह्रास को प्रोत्साहित करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि वनों के ह्रास से मानव जीवन प्रभावित होता है और उसका विनाश होता है।
3. वन्यजीवों के संरक्षण के उद्देश्य क्या हैं ?
उत्तर – वन्यजीवों के संरक्षण से तात्पर्य वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण और उनका समुचित विकास करने से है। इससे वन्यजीवों का समुचित विकास और उनकी संख्या में वृद्धि होती है। इससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है।
वन्यजीवों के संरक्षण के उद्देश्य वन्यजीवों के संरक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
- पारिस्थितिक सन्तुलन को बनाये रखना- वन्यजीवों के संरक्षण का प्रमुख उहे पारिस्थितिक सन्तुलन को बनाये रखना है। इससे जीवों की संख्या में सन्तुलन बना रहता है
- लुप्तप्राय वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि – वन्यजीवों के संरक्षण का उद्देश्य लुप्तप्राय वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि करना है। इससे वन्यजीवों का समुचित विकास और उनकी संख्या में समुचित वृद्धि होती है।
- जीन पूलों की रक्षा — वन्यजीवों के संरक्षण का उद्देश्य वन्यजीवों में जीन पूलों की रक्षा करना है। इससे वन्यजीवों के जीनों की रक्षा होती है और उनका समुचित विकास होता है।
- पृथ्वी पर अत्यधिक जंगलों का सफाया- वन्यजीवों के संरक्षण का उद्देश्य पृथ्वी पर जरूरत से ज्यादा जंगलों का सफाया करना है। अगर पृथ्वी पर अत्यधिक जंगलों की वृद्धि हो जायेगी तो पृथ्वी पर मनुष्य के रहने के लिये जगह नहीं बचेगी। वन्यजीवों के समुचित संरक्षण से इस समस्या का निपटारा किया जाता है।
- बहुमूल्य वन्यजीवों का विकास – वन्यजीवों के संरक्षण का उद्देश्य बहुमूल्य वन्यजीवों जैसे— शेर, हाथी, घड़ियाल इत्यादि का विकास करना है। वन्यजीबों के संरक्षण करने से इन बहुमूल्य वन्यजीवों का संरक्षण और उनका समुचित विकास किया जाता है।
इसके अलावा वन्यजीवों के संरक्षण के लिये और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको पूरा कर वन्यजीवों का संरक्षण किया जाता है।
4. ऊर्जा संकट क्या है ? इसके समाधान के उपायों का उल्लेख करें।
उत्तर – ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला एवं पेट्रोलियम हैं पृथ्वी के अंदर इनकी मात्रा भी सीमित है। औद्योगीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण इनकी माँग भी कई गुना तेजी से बढ़ी है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनका निर्ममतापूर्वक दोहन कर रहे हैं। ऊर्जा के इन स्रोतों का उपयोग हम अपनी दैनिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा जीवनोपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु कर रहे हैं। चूँकि इनके भंडार सीमित हैं, अतः इनके एक बार समाप्त हो जाने पर निकट भविष्य में इनकी पूर्ति संभव नहीं होगी। इसका कारण है कि इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। इस प्रकार देश में ऊर्जा की कमी हो जाएगी जिससे उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अतः देश को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा।
ऊर्जा के महत्त्व को ध्यान में रखकर ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करने की आवश्यकता है ताकि आनेवाले अधिक-से-अधिक समय तक हम इनका उपयोग कर सकें। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की उपलब्धता सीमित होने के कारण इसके वैकल्पिक स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता भी महसूस की जाती है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं— सौर ऊर्जा (solar energy), पवन ऊर्जा (wind energy) तथा जैव स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा अर्थात बायोगैस आदि । ऊर्जा के इन स्रोतों के विकास से अनेक कार्यों के लिए ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। आजकल परमाणु ऊर्जा की चर्चा जोरों पर है। इसके उत्पादन की क्षमता विकसित करके भी हम देश को ऊर्जा संकट से काफी हद तक उबार सकते हैं।
5. पर्यावरण संरक्षण के लिये चलाये गये चिपको आन्दोलन का संक्षिप्त विवरण दें।
उत्तर – आज भी तेजी से वनों का कटाव जारी है। वनों के कटाव से जंगली जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जंगल के तेजी से कटने से मानव को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल के पहाड़ों पर स्थित रेनी ग्राम में इमारती लकड़ी के ठेकेदारों के हाथों वनों का विनाश रोकने के लिए स्थानीय स्त्रियों ने पेड़ों से चिपक कर एक जन-आन्दोलन किया था। इसी तरह राजस्थान के खेजरी ग्राम में पेड़ों से चिपककर स्त्रियों के जान देने की घटना की याद में लोगों ने इस आन्दोलन को चिपको आन्दोलन का नाम दिया। इस आन्दोलन का समर्थन जाने-माने समाजसेवी सुन्दरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने किया। वन विनाश के विरोध में इनके कार्यकर्त्ताओं ने हिमालय क्षेत्र में लम्बी-लम्बी पद यात्रा की। इसने वन काटने वाले ठेकेदारों का ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी वनों के महत्व को समझाया।
इस प्रकार चिपको आन्दोलन उस समय जनवादी रूप धारण कर चुका था। इस आन्दोलन ने पर्यावरण संरक्षण में अपना अहम योगदान दिया था।
6. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर – प्राकृतिक संसाधन (जल, मृदा, वन, खनिज, पेट्रोलियम, वन्य जीव आदि) असीमित नहीं होते हैं। औद्योगिक क्रांति तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का निर्ममतापूर्वक दोहन किया जा रहा है जिससे त्रे क्षीण होते जा रहे हैं। अतः हम सबों का ध्यान इनके संरक्षण एवं प्रबंधन की ओर गया है। संसाधन प्रबंधन का अर्थ होता है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ताकि उनकी गुणवत्ता तथा उपलब्धता बनी रहे तथा विकास कार्य भी न रुके और पर्यावरण भी संतुलित बना रहे । पृथ्वी के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्रों के विभिन्न अवयवों के बीच का संतुलन स्थापित करने में मनुष्य की भूमिका इस युग की सबसे बड़ी चुनौती है। इस संतुलन के स्थापित रहने में मदद देकर ही हम भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ सुनिश्चित कर पाएँगे। पर्यावरण
7. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख करें।
उत्तर – प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय प्रयासों के साथ-साथ समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास किये गये हैं। इन प्रयासों में कुछ निम्नलिखित है जो इस प्रकार हैं –
क्योटो प्रोटोकॉल — 1977 में जापान के क्योटो (Kyoto) शहर में भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के 141 देशों ने भाग लिया। इस क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार सभी औद्योगिक देशों के 2008 से 2012 तक के पाँच वर्षों की अवधि में 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन के स्तर में 1990 के स्तर से कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य है कि ग्रीनहाउस गैस छोड़नेवाली तकनीकों का उपयोग सीमित रखा जाए। इससे संबंधित नियम सरल बनाया जाए तथा पारम्परिक ऊर्जा के इस्तेमाल में कमी लाई जाए। हमारे देश में ग्रीनहाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि के उपयोग में होता है। इसके अलावा लकड़ी और उपले जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।
उत्सर्जन संबंधी मानदंड – वाहनों की भारी संख्या और यातायात वाले कुछ शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि पाई गयी है। जैसे—दिल्ली तथा कोलकाता के कुछ क्षेत्रों में। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वाहनों को वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में एक बताया है। इस कारण 1989 में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित किया गया। इस संशोधन के बाद वाहन मालिकों के लिए धुएँ के उत्सर्जन संबंधी नियम अधिसूचित किए गए और 1991 में पहली बार वाहन निर्माताओं के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड, जैसे— युरो – I (Euro-I) लागू किया गया। इन मानदंडों को 2000 में फिर संशोधित कर युरो-II (Euro-II) लागू किया गया जिससे दिल्ली में ईंधन के दहन से निकले गैसों की मात्रा में कमी आयी है तथा वायु की गुणवत्ता बढ़ी है। इन उत्सर्जन संबंधी मानदंडों को समय-समय पर बदल कर सख्त कर दिया जाता है तथा वाहनों से निकले धुओं में विभिन्न गैसों की मात्रा को सीमित कर दिया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारे देश को जल प्रदूषण की रोकथाम में सहायता दे रहा है। गंगा को स्वच्छ बनाने का जो अभियान चालू हुआ है उससे अब विश्वास होने लगा है कि देश की अन्य नदियाँ भी स्वच्छ हो सकेगीं।
8. वर्षा जल के संचयन के लाभ का संक्षिप्त विवरण दें।
उत्तर – भूमिगत जल का परिपूरण वर्षा के जल से होता है। किंतु हमारे देश में वर्षा की अवधि वर्ष कं कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है। अत: वर्षाजल का अधिक से अधिक संचयन कर उसे भूमिगत जल-स्तर तक पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है ताकि भूमिगत जल स्तर बना रहे। भूमिगत जल-स्तर तक वर्षाजल को पहुँचाने के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएँ की जाती हैं—(i) बोर वेल (bore well) और (ii) डग वेल (dug well) । भूमिगत जल के अनेक लाभ हैं। इसका जल वाष्पीकृत नहीं होता। भूमिगत जल फैलकर कुएँ के जल को परिपूर्ण करते हैं तथा खेतों में नमी बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त इससे मच्छरों के जनन की समस्या भी नहीं होती। भूमिगत जल मनुष्य तथा जानवरों के अपशिष्ट से झीलों, तालाबों आदि में ठहरे जल के विपरीत संदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। स्थानीय स्तर पर वर्षाजल के संचयन के फलस्वरूप लोगों को पीने एवं सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बनी रहती है।
अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
I. सही उत्तर का संकेताक्षर ( क, ख, ग या घ) लिखें।
1. बाँध का उपयोग है
(क) उद्योगों में
(ख) सिंचाई व बिजली उत्पादन में
(ग) स्कूलों व कॉलेजों में
(घ) सभी में
उत्तर – (ख)
2. जल संभर प्रबंधन से क्या फायदे हैं ?
(क) इससे भूजल स्तर नीचे हो जाता है
(ख) इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है
(ग) इससे वैश्विक ऊष्मा बढ़ जाती है
(घ) कोई नहीं
उत्तर – (ख)
3. हिमाचल प्रदेश में कौन-सी प्राचीन जल संग्रहण तथा जल संरचनाएँ प्रयोग में थीं –
(क) कुल्ह
(ख) तालाब
(ग) एरिस
(घ) कट्टा
उत्तर – (क)
4. जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं
(क) समुद्र
(ख) शहर
(ग) गाँव
(घ) वन
उत्तर – (घ)
5. कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है
(क) रेड हाऊस गैस
(ख) ग्रीन हाऊस गैस
(ग) ब्लू हाऊस गैस
(घ) ब्लैक हाऊस गैस
उत्तर – (ख)
6. निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है ?
(क) कोयला
(ख) नदी
(ग) मोटरगाड़ी
(घ) वन
उत्तर – (ग)
7. पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ गहराई पर स्थित जल स्तर कहलाता है
(क) सतही जल – स्तर
(ख) भूमिगत जल – स्तर
(ग) मृदु जल – स्तर
(घ) समुद्री जल – स्तर
उत्तर – (ख)
8. कीट, कवक, बैक्टीरिया जैसे जीवों के उपयोग से पीड़कों के नियंत्रण की विधि कहलाती है।
(क) रासायनिक नियंत्रण
(ख) जैविक नियंत्रण
(ग) पीड़क नियंत्रण
(घ) यांत्रिक नियंत्रण
उत्तर – (ख)
9. वह कृषि पद्धति जिसके अंतर्गत एक से ज्यादा फसलों का उत्पादन एवं भोजन उत्पादन के लिए पशुधनों का पालन-पोषण साथ-साथ किया जाता है, कहलाती है –
(क) मिश्रित कृषि
(ख) अंतर- फसल उत्पादन
(ग) फसल-चक्रण
(घ) सह- फसल उत्पादन
उत्तर – (क)
10. वह कृषि प्रणाली जिसमें अधिक उत्पादकता के साथ-साथ पर्यावरण के प्रदूषित होने की संभावना कम-से-कम हो, कहलाती है
(क) मिश्रित कृषि
(ख) पारिस्थितिकी – प्रतिकूल कृषि
(ग) पारिस्थितिकी – अनुकूल कृषि
(घ) प्राचीन कृषि
उत्तर – (ग)
11. पारिस्थितिकी- अनुकूल कृषि के लिए की जानेवाली अनुशंसा है
(क) जैव उर्वरकों का उपयोग
(ख) एकीकृत पीड़क प्रबंधन
(ग) कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग
(घ) इनमें सभी
उत्तर – (घ)
12. गोबर तथा मृत पौधों के अपघटन एवं मल-मूत्र से तैयार किया गया है
(क) जैव उर्वरक
(ग) हरित उर्वरक
(ख) कंपोस्ट
(घ) रासायनिक खाद
उत्तर – (ख)
13. निम्नांकित में किसकी मदद से तैयार होनेवाला खाद वर्मी कम्पोस्ट कहलाता है ?
(क) हुकवर्म
(ख) टेपवर्म
(ग) केंचुआ
(घ) घोंघा
उत्तर – (ग)
14. फसलों का वह किस्म जिसपर पीड़कों का आक्रमण नहीं होता है, कहलाता है
(क) अवरोधी किस्म
(ख) उन्नत किस्म
(ग) प्रतिरोधी किस्म
(घ) संकर किस्म
उत्तर – (ग)
15. निम्नलिखित में कौन संश्लेषित पॉलीमर है ?
(क) जूट
(ख) ऐक्रिलिक
(ग) रेयॉन
(घ) ऊन
उत्तर – (ग)
16. ‘राज्य, देश के पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार का और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा ।” यह भारतीय संविधान की किस धारा में वर्णित है ?
(A) धारा 48 A
(ख) धारा 51 A
(ग) धारा 42
(घ) धारा 46
उत्तर – (क)
17. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है ?
(क) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(ख) वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(घ) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
उत्तर – (क)
18. पशुओं पर होनेवाले अत्याचार के निवारण के लिए बनाया गया अधिनियम है
(क) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(ग) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1990
उत्तर – (ग)
19. उत्पादनकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से शुरू किया गया पुरस्कार है
(क) राजीव गाँधी गुणवत्ता पुरस्कार
(ख) संजय गाँधी गुणवत्ता पुरस्कार
(ग) इंदिरा गाँधी गुणवत्ता पुरस्कार
(घ) नेहरू गुणवत्ता पुरस्कार
उत्तर – (क)
20. उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है
(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
(ख) भारतीय मानक ब्यूरो
(ग) उपभोक्ता कल्याण कोष
(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम
उत्तर – (क)
21. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है
(क) 8 दिसंबर
(ख) 24 दिसंबर
(ग) 30 जनवरी
(घ) 5 जून
उत्तर – (ख)
22. पाप-तौल में एकरूपता तथा समान मानक स्थापित रखने के उद्देश्य से बनाया गया कानून हैसीरीज
(क) ISO 9000 सीरीज
(ख) ISO 14000
(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
(घ) माप-तौल मानक अधिनियम, 1976
उत्तर – (घ)
23. सरसों के तेल में आर्जीमोन या कटैया के बीज के तेल के अपमिश्रण से होनेवाला रोग है-
(क) ड्रॉप्सी
(ख) लेथाइरिज्म
(ग) मंदबुद्धि
(घ) पेचिश
उत्तर – (क)
24. वाहनों को चलाने में पारंपरिक डीजल की अपेक्षा CNG बेहतर है, क्योंकि ऐसे वाहनों से –
(क) उत्सर्जित धुएँ में सल्फर तथा सीसा की मात्रा नहीं होती है
(ख) उत्सर्जित धुएँ में CO तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है
(ग) बेंजीन तथा अन्य जहरीले पदार्थों का निष्कासन अत्यंत कम मात्रा में होता है
(घ) उपर्युक्त सभी
उत्तर – (घ)
25. चिपको आंदोलन के प्रवर्तक है –
(क) अमृता देवी
(ख) सुंदरलाल बहुगुणा
(ग) हेमवती नंदन बहुगुणा
(घ) अमृत कौर
उत्तर – (ख)
26. शांत घाटी (silent valley) स्थित है –
(क) तमिलनाडु में
(ख) केरल में
(ग) कर्नाटक में
(घ) मेघालय में
उत्तर – (ख)
27. वायुमंडल में संतुलन बनता है –
(क) उत्पादकों द्वारा
(ख) अपघटकों द्वारा
(ग) उत्पादक और उपभोक्ता द्वारा
(घ) उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक द्वारा
उत्तर – (घ)
28. कारखाने के दूषित पदार्थों को सीधे नदी में गिराने से –
(क) जलवायु दूषित होती है
(ख) जलीय जीव नष्ट हो जाएँगे
(ग) पानी का सिर्फ रंग बदल जाएगा
(घ) पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
उत्तर – (ख)
29. एक भूमि पर प्रतिवर्ष एक ही फसल उगाना कहलाता है-
(क) सिल्वीकल्चर
(ख) हार्टिकल्चर
(ग) मोनोकल्चर
(घ) बहुफसली खेती
उत्तर – (ग)
30. निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ज्य पदार्थ अनिम्नीकरणीय है ?
(क) गाय का गोबर
(ख) खाद
(ग) प्लास्टिक
(घ) रसोईघर का कूड़ा
उत्तर – (ग)
31. निम्नलिखित में से कौन-सी गैस आदि- पृथ्वी पर तो उपस्थित थी, परन्तु अब नहीं है ?
(क) नाइट्रोजन
(ख) कार्बन मोनोक्साइड
(ग) कार्बन डाइऑक्साइड
(घ)अमोनिया
उत्तर – (घ)
32. भारत सरकार ने यह निश्चित किया है कि भारत की भूमि में जंगल होने चाहिए लगभग –
(क) 10%
(ख) 20%
(ग) 30%
(घ) 40%
उत्तर – (ग)
33. कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है —
(क) मध्य प्रदेश में
(ख) महाराष्ट्र में
(ग) उत्तरांचल में
(घ) मद्रास में
उत्तर – (ग)
34. भारतीय चीता किस कारण लुप्त हो गया है ?
(क) पालतू बनाने से
(ख) वर्षा के कारण
(ग) शिकार करने से
(घ) गर्मी के कारण
उत्तर – (ग)
35. सबसे खतरनाक प्रदूषण का प्रकार निम्नांकित में से कौन है ?
(क) ध्वनि प्रदूषण
(ख) मोटर गाड़ियों का धुआँ
(ग) औद्योगिक अनुपयोगी वस्तुओं का जल में मिलना
(घ) घरेलू अपमार्जक
उत्तर – (ग)
36. निम्नलिखित में से किसके कारण भूमि से पौधों के पोषक तत्त्व की हानि होती है ?
(क) लगातार एक ही फसल उगाने से
(ख) उर्वरक डालने से
(ग) जन्तुओं के चरने से
(घ) रेतीली मिट्टी से
उत्तर – (क)
37. भूमि अपरदन का मुख्य कारण है-
(क) वनों की कटाई
(ख) पहाड़ों का टूटना
(ग) सूखा पड़ना
(घ) भूमि अधिग्रहण
उत्तर – (क)
II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
1. नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड ……… गैसें हैं ।
उत्तर – विषैली
2. बस में यात्रा करने की जगह पैदल या साइकिल से चलना ……….. है ।
उत्तर – पर्यावरणानुकूल
3. बड़े बाँध का उपयोग …….. और ………. के लिए किया जाता है।
उत्तर – सिंचाई, विद्युत उत्पादन
4. गंगा गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर …………. तक यात्रा करती है।
उत्तर – 2500 km
5. गंगा की सफाई के लिए ………..में एक वृहत योजना प्रारंभ की गई थी।
उत्तर – 1985
6. बेकार कहे जानेवाले वन का मूल्य ………..करोड़ आँका गया है।
उत्तर – 125
7. उपभोक्ता जागरूकता के प्रशिक्षण संबंधी सुविधा के लिए ………… स्थापित किया गया
उत्तर – उपभोक्ता कल्याण कोष
8. ………….. के अनुसार, खाद्य पदार्थों में मिलावट करना एक दंडनीय अपराध है।
उत्तर – खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम
9. वनक्षेत्र के ऐसे भाग जो मानवीय क्रियाकलाप से पूर्णत: अछूते होते हैं; ………….कहलाते हैं।
उत्तर – पवित्र वाटिका (sacred groves
10. सी. एन.जी. का पूरा नाम …..…….. है।
उत्तर – कंप्रेस्ड नेचुरल गैस
11. भूमिगत जल के पुनः परिपूरण या पुनर्भरण के लिए ………….की आवश्यकता होती है।
उत्तर – वर्षाजल
12. झूमिंग या स्थानांतरीय कृषि प्रणाली से असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम तथा उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में ………….का विनाश हुआ है।
उत्तर – वनों
13. मानव द्वारा प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि प्रकृति में उनका ………….. होता रहे।
उत्तर – परिपूरण
14. पीड़कनाशी (पेस्टीसाइड्स) के अधिक उपयोग ………… प्रभाव फसलों एवं मृदा पर का पड़ता है।
उत्तर – प्रतिकूल
15. एक ही कृषिभूमि पर बदल-बदलकर अनुक्रम में एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया ………… कहलाती है।
उत्तर – फसल-चक्रण / फसल – आवर्तन
16. रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक इस्तेमाल से पर्यावरण में ……….. फैलता है।
उत्तर – प्रदुषण
17. ……….. नाइट्रोजन स्थायीकर बैक्टीरिया है।
उत्तर – राइजोबियम
18. वर्मी कंपोस्ट ……….. तकनीक से तैयार किया जाता है।
उत्तर – चर्मी कल्चर
19. कीट, कवक, बैक्टीरिया जैसे जीवों के उपयोग से पीड़कों के नियंत्रण की विधि ……….. कहलाती है।
उत्तर – जैविक नियंत्रण
20. एक्रिलिक …….. श्रेणी का रेशा है।
उत्तर – संश्लेषित पॉलीमर
21. भारतीय संविधान की धारा ……….पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित प्रमुख धारा है।
उत्तर – 48 A
22. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम ………. में अस्तित्व में आया।
उत्तर – 1972
23. जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के निदेशों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए धारा ……….. में दंड का प्रावधान है।
उत्तर – 42-49
24. पशुओं के दुःख और पीड़ा के निवारण के लिए …………1960 बनाया गया है।
उत्तर – पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
25. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ………. को मनाया जाता है।
उत्तर – 24 दिसंबर
26. हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि ……….. की भाँति होती है।
उत्तर – कीट है
27. ओजोन प्रकाश में उपस्थित ……… को अवशोषण कर लेता है।
उत्तर – पराबैंगनी
28. ……….. “किरणें मनुष्य में कैंसर रोग का कारण है।
उत्तर – पराबैंगनी
29. पृथ्वी के चारों ओर करीब उत्तर – पराबैंगनी ………… किमी की ऊँचाई तक वायुमंडल का विस्तार है।
उत्तर – 60 किलोमीटर
30. फसल चक्रण से ………..को पुनः पूरित किया जाता है।
उत्तर – मिट्टी
31. जनसंख्या की वृद्धि …………. श्रेणी में बढ़ती है ।
उत्तर – गुणोत्तर
32. ………… जैव अनिम्नीकरणीय वर्ज्य का एक उदाहरण है।
उत्तर – प्लास्टिक
33. वन्य जीव सुरक्षा कानून ……….. में बनी थी।
उत्तर – 1972
34. वनों को पुनः पूरण के लिए ………. कार्यक्रम चलाना चाहिए।
उत्तर – वनवर्धन
35. आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों से गुजरकर हानिकारक रसायनों के सांद्रण को ……….. कहते हैं।
उत्तर – जैव आवर्धन
III. सही / गलत का चयन करें।
1. चिपको आन्दोलन घर के तोड़े जाने के विरोध में किया जाता है।
उत्तर – गलत
2. सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा गैर-परंपरागत स्रोत है।
उत्तर – सही
3. वनों के ह्रास से कई प्रकार की जैव प्रजातियाँ लुप्त हो जाती हैं।
उत्तर – सही
4. पहली बार वाहन निर्माताओं के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड 1981 में लागू किया गया था।
उत्तर – गलत
5. वन एक नवीकरणीय संसाधन है।
उत्तर – सही
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
1. प्रदूषण क्या है ?
उत्तर – प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अथवा शुद्ध रूप में पाए जाने वाले पदार्थों में धूल कण तथा अन्य नुकसानदेह पदार्थों का मिश्रण प्रदूषण कहलाता है।
2. किन्हीं पाँच प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताएँ।
उत्तर – 1. वन 2. वन्य जीव 3. जल 4. कोयला 5. पेट्रोलियम ।
3. पर्यावरण को बचाने के लिए तीन R के नाम बताएँ।
उत्तर – 1. Reduce (कम करो), 2. Recycle ( पुन: चक्रण), 3. Reuse (पुन: प्रयोग ) ।
4. CFC का पूरा नाम बताएँ।
उत्तर – क्लोरो फ्लोरो कार्बन ।
5. स्वस्थ सेवाओं का संसाधनों से किस प्रकार संबंध है ?
उत्तर – स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण संसाधनों की माँग बढ़ती है।
6. जैव विविधिता के लिए उत्तरदायी जीवों के नाम बताएँ।
उत्तर – जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी, पादप, निमेटोडस, कीट, पक्षी, सरीसृप ।
7. गंगा सफाई योजना किस सन् में अपनाई गई थी ?
उत्तर – सन् 19851
8. Rs में Reduce (कम करो ) का क्या अर्थ है ?
उत्तर – कम करो का अर्थ है कि हमें कम से कम वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए ।
9. कोलिफार्म क्या है ?
उत्तर – कोलिफार्म, जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आँत में पाया जाता है ।
10. गंगा के उद्गम स्थान एवं मार्ग के बारे में बताएँ।
उत्तर – गंगा अपने उद्गम गंगोत्री, बंगाल की खाड़ी से होते हुए 2500 km की यात्रा कर समुद्र में मिलती है।
11. तीन विषैली गैसों के नाम बताएँ ।
उत्तर – नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं।
12. वायु प्रदूषण के मानकों के नाम बताएँ।
उत्तर – युरो I, युरो II, एवं युरो III वायु प्रदूषक के मानक हैं।
13. चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई ?
उत्तर – सन् 1970 में हिमालय की ऊँची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के ‘रेनी’ नामक गाँव में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई।
14. खुदाई में प्रदूषण क्यों होता है ?
उत्तर – क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ-साथ बड़ी मात्रा में स्लैग भी निष्कर्षित होता है।
15. वन क्या हैं ?
उत्तर – वन ‘जैव विविधता’ के तप्त स्थल हैं।
16. जैव विविधता का क्या आधार है ?
उत्तर – जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या पर है। परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप भी महत्वपूर्ण हैं।
17. भारत की वर्षा किस पर निर्भर करती है ?
उत्तर – मॉनसून पर। इसका अर्थ है कि वर्षा की अवधि वर्ष कुछ महीनों तक ही सीमित है।
18. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीनकाल से किसका प्रयोग किया जाता है ?
उत्तर – बाँध, जलाशय एवं नहरों का प्रयोग किया जाता है।
19. बाँध की दो आवश्यकताएँ बताइए।
उत्तर – 1. बड़े बाँध से जल का संग्रह पर्याप्त मात्रा में किया जाता है।
2. बाँध विद्युत् उत्पादन में भी सहायता करते हैं।
20. ‘कुल्ह’ किसे कहते हैं ?
उत्तर – 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय व्यवस्था का विकास किया गया था। इन्हें ‘कुल्ह’ कहते हैं।
21. अपशिष्ट पदार्थों को किन दो वर्गों में रखा जा सकता है ? इनमें से कौन सा अधिक घातक होता है ?
उत्तर – (i) जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ ।
(ii) जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ ।
इन दोनों में से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ अधिक घातक है।
22. बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना से स्थानीय जलवायु पर होने वाले कोई दो प्रभाव बताइए।
उत्तर – 1. वायु प्रदूषण, 2. आस-पास के वायुमंडल के ताप में वृद्धि |
23. वनों के पुनः पूर्ण के लिए कौन-सा कार्यक्रम है ?
उत्तर – वनों के पुनः पूर्ण के लिए वन महोत्सव एक मुख्य कार्यक्रम है।
24. रंध्राकाश क्या है ?
उत्तर – मृदा कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है जो सामान्यतः जल तथा वायु दोनों से भरे होते हैं, रंध्राकाश कहलाते हैं।
25. प्रदूषण के किन्हीं तीन प्रमुख व बड़े कारणों के नाम लिखें।
उत्तर – (i) जनसंख्या विस्फोट (ii) औद्योगीकरण तथा (iii) शहरीकरण ।
26. ओजोन की परत को नष्ट करनेवाले यौगिकों के समूह का नाम दें तथा इस परत के क्षीण होने पर पृथ्वी में जीवन पर पड़नेवाले प्रभाव भी बताइए।
उत्तर – यौगिक समूह का नाम – ऐरोसॉल ।
प्रभाव – त्वचा कैंसर की उत्पत्ति ।
27. पारिस्थितिक संतुलन क्या है ?
उत्तर – पर्यावरण के जैव व अजैव घटकों के बीच होनेवाली वह पारस्परिक क्रियाएँ जिससे दोनों घटकों के बीच साम्यावस्था की स्थिति बनी रहती है— पारिस्थितिक संतुलन कहलाता है।
28. नवीकरण साधन क्या है ?
उत्तर – वे प्राकृतिक साधन जिनका नवीकरण किया जा सकता है नवीकरण साधन कहे जाते हैं। जैसे—मृदा, वायु, जल आदि ।
29. अनवीकरण साधन क्या है ?
उत्तर – वे प्राकृतिक साधन जिनका नवीकरण किया जा सकता है अनवीकरण साधन कहलाते हैं। जैसे—फॉसिल ईंधन, कोयला, खनिज आदि।
30. वनवर्धन क्या है ?
अथवा, सिल्वीकल्चर से क्या समझते हैं ?
उत्तर – वनों में वृक्ष लगाना, उसकी देखभाल करना तथा उनका प्रबन्ध करना आदि क्रियाएँ वनवर्द्धन या सिल्वीकल्चर कहलाती है।
31. पर्यावरण के मौसम संबंधी किन्हीं तीन घटकों के नाम लिखें।
उत्तर – सूर्य प्रकाश, वर्षा तथा ताप या पवन वेग।
32. जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं ?
उत्तर – वे अपशिष्ट पदार्थ जो अपघटकों द्वारा निराविषी (Non-toxic) रूप में अवक्रमित हो सकते हैं जैव निम्नीकरणीय (Biodegradable) पदार्थ कहे जाते हैं। जैसे—मानव अपशिष्ट आदि ।
33. अपमार्जक किसे कहते हैं ?
उत्तर – वे जीव जो मृत शरीरों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, अपमार्जक कहे जाते हैं। जैसे— चील तथा गिद्ध
34. पर्यावरण में हानिकारक प्रभावों से ओजोन सतह किस प्रकार हमें सुरक्षा प्रदान करती है ?
उत्तर – ओजोन सतह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर इसके घातक कुप्रभावों से हमें बचाती है।
35. आयल स्लिक किसे कहते हैं ?
उत्तर – पानी में गिरने पर तेल हल्का होने के कारण पानी के ऊपर एक पतली परत बना लेता है इसे चिक्कण या आयन स्लिक (Oil slick) कहते हैं।
36. भौम जलस्तर क्या है ?
उत्तर – भूमि में कुछ गहराई के नीचे समस्त रंध्राकाश केवल जल से भरे होते हैं। भूमि की इसी गहराई को भौम जल स्तर कहा जाता है।
37. प्राकृतिक संसाधन क्या है ? प्राकृतिक संसाधनों के स्वधारणीय उपयोग से क्या समझते हैं ?
उत्तर – प्रकृति प्रदत्त वैसी वस्तुएँ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख-सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं।
प्राकृतिक संसाधनों के स्वधारणीय उपयोग का अभिप्राय संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करने से है कि उन्हें लंबे समय तक प्रकृति में कायम रखा जा सके।
38. एकीकृत पीड़क प्रबंधन क्या है ?
उत्तर – पीड़कों के नियंत्रण के लिए जब एक से अधिक नियंत्रण विधियों को उनके गुणों एवं अवगुणों के आधार पर सम्मिलित कर उनका उपयोग साथ-साथ किया जाए तब उसे एकीकृत पीड़क प्रबंधन कहा जाता है।
39. पवित्र वाटिका किसे कहते हैं ?
उत्तर – वनक्षेत्र के ऐसे भाग जो मानवीय क्रियाकलापों से पूर्णत: अछूते होते हैं, पवित्र वाटिका कहलाते हैं। भारत में ऐसे क्षेत्र केरल की नीलगिरि पहाड़ियों के बीच, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एवं मणिपुर, सिक्किम तथा अंडमान-निकोबार में स्थित है।
40. खाद्य अपमिश्रण से क्या समझते हैं ?
उत्तर – मुनाफाखोरी के उद्देश्य से खाद्यान्नों में ऐसी वस्तुओं की मिलावट, जो सस्ती होने के साथ-साथ खाने के अयोग्य, निम्न गुणवत्तावाली तथा कभी-कभी खाद्यान्नों को विषाक्त बनानेवाली हों, को खाद्य अपमिश्रण कहते हैं।
41. पर्यावरण के दृष्टिकोण से वाहनों में डीजल की जगह सी.एन.जी. का उपयोग किस प्रकार लाभदायक है ?
उत्तर – सी.एन.जी. द्वारा चालित वाहनों से निकलनेवाले धुएँ में कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा विविक्त पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। इसमें सल्फर तथा सीसा की मात्रा नहीं होती।
42. भूमिगत जल के पुनःभरण के लिए कौन-सा कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ?
उत्तर – रेन वाटर हार्वेस्टिंग नामक विधि से भूमिगत जल का पुनःभरण किया जाना चाहिए। इस विधि में वर्षाजल को भवनों की छतों व ऐसे स्थानों पर इकट्ठा कर पाइप की सहायता से धरती के नीचे भूमिगत जल स्तर की सतह तक पहुँचा दिया जाता है।
43. शांत घाटी (साइलेंट वैली) क्या है ?
उत्तर – यह प्रशासकीय आदेश द्वारा सुरक्षित एक वनक्षेत्र है जहाँ वन्य जीव अपने प्राकृतिक वासस्थानों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। यह केरल राज्य की पश्चिमी घाटी की कुंडली पहाड़ियों (नीलगिरि) के बीच स्थित है। यह मानवीय गतिविधियों से अछूता है।
44. नेशनल ग्रीन कॉर्प्स के विषय में क्या जानते हैं ?
उत्तर – स्कूली बच्चों के विभिन्न पर्यावरणीय संरक्षण गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन कॉर्प्स की स्थापना की है। इसके अंतर्गत स्कूलों में परि-क्लब या इको क्लब स्थापित किए गए हैं।
45. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कौन-सा अधिनियम बनाया गया है ? इसका क्या उद्देश्य है ?
उत्तर – उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, उनकी शिकायतों को दर्ज करने तथा उनसे राहत दिलाने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 बनाया गया है।
46. एक खनिज का नाम बताएँ जिसके उपयोग से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है।
उत्तर – पेट्रोलियम।
47. सर्वप्रथम वाहन निर्माताओं के लिए धुएँ के उत्सर्जन संबंधी कौन-सा मानदंड लागू
उत्तर – 1991 में पहली बार वाहननिर्माताओं के लिए धुएँ के उत्सर्जन संबंधी मानदंड, जैसे युरो – I (Euro-I) लागू किया गया।
48. एक संगठन का नाम बताएँ जो हमारे देश को जल प्रदूषण की रोकथाम में सहायता दे रहा है।
उत्तर – विश्व स्वास्थ्य संगठन।
49. कोलिफॉर्म जीवाणु मानव के किस अंग में पाए जाते हैं ?
उत्तर – कोलिफॉर्म जीवाणु मानव की आँत में पाए जाते हैं।
50. पीने के जल में कोलिफॉर्म की मात्रा कितनी होनी चाहिए ?
उत्तर – पीने के जल में प्रति 100 mL जल में कोलिफॉर्म की संख्या शून्य होनी चाहिए।
51. गंगा जल को प्रदूषित करनेवाले मानव के तीन क्रियाकलापों की चर्चा करें।
उत्तर – गंगा जल को प्रदूषित करनेवाले मानव के तीन क्रियाकलाप हैं—(i) नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल जल को प्रवाहित करना, (ii) पशुओं को स्नान कराना और (iii) मृत व्यक्तियों के शवों को बहाना एवं अस्थित विसर्जन करना।
52. भूमिगत जल के दो लाभ बताएँ।
उत्तर – भूमिगत जल फैलकर कुएँ के जल को परिपूर्ण करते हैं तथा खेतों में नमी बनाए रखते हैं। भूमिगत जल मनुष्य तथा जानवरों द्वारा दूषित नहीं होते।
53. वर्षाजल के संचयन की परंपरागत पद्धतियाँ कौन-कौन-सी हैं ?
उत्तर – वर्षाजल के संचयन की परंपरागत पद्धतियाँ निम्नांकित हैं—(i) छोटे-छोटे मिट्टी के बाँध बनाना, (ii) छोटे-छोटे गड्ढे खोदना, (iii) बालू तथा संगमरमर के जलाशय बनाना तथा (iv) मकान के छत पर जल का संचयन तंत्र लगाना ।
54. पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन-कौन से परिवर्तन ला सकते हैं ?
उत्तर – पर्यावरण – मित्र बनने के लिए किसी वस्तु का कम-से-कम उपयोग करने, अनुपयोगी वस्तुओं को गलाकर उपयोगी वस्तुएँ बनाने एवं वस्तुओं के पुनर्चालन और पुनरूपयोग करने की आदत डालनी चाहिए।
55. दो वस्तुओं के नाम बताएँ जिन्हें हम पुनरूपयोग में ला सकते हैं ?
उत्तर – अचार या जेली के खाली प्लास्टिक डिब्बा एवं पुराना लिफाफा ।
56. क्या आपके विचार में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए ?
उत्तर – हाँ, संसाधनों का वितरण सभी वर्गों में समान रूप से होना चाहिए।
57. संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन-कौन-सी ताकतें कार्य कर सकती हैं ?
उत्तर – मुट्ठी भर अमीर एवं शक्तिशाली लोग संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कार्य कर हैं।
58. संसाधनों की सावधानीपूर्वक उपयोग की क्यों आवश्यकता है ?
उत्तर – संसाधनों के विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग की आवश्यकता इसलिए है कि संसाधन सीमित हैं तथा जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की माँग में कई गुना तेजी से वृद्धि हुई है।
59. हम जल प्रणाली का संरक्षण कैसे कर सकते हैं ?
उत्तर – जल संसाधन का उपयोग सुनियोजित ढंग से करके तथा जलस्रोतों का उचित प्रबंधन करके हम जल प्रणाली का संरक्षण कर सकते हैं।
60. प्रदूषित जल से होने वाली बिमारियों के नाम लिखें।
उत्तर – हैजा, पीलिया, यइफाइड ।
61. चिपको आन्दोलन का संबंध किससे है ?
उत्तर – वनों के संरक्षण से,
62. टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है ?
उत्तर – भागीरथी नदी |
63. वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है ?
उत्तर – पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए।
64. वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए ?
उत्तर – वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करने का कारण यह है कि प्राणियों के अस्तित्व बनाए रखने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है तथा उनके नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट हो सकता है।
65. भारत में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कौन-कौन-से उपाय किए गए हैं ?
उत्तर – भारत में वन्यजीवों के संरक्षण हेतु वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान तथा अन्य प्राकृतिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है। इसके लिए बाघ परियोजना एवं कुछ अन्य परियोजनाएँ भी प्रारंभ की गई हैं।
लघु उत्तरीय प्रश्न
1. प्राकृतिक संसाधन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए।
उत्तर – प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources) – प्रकृति में पाए जाने वाले मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं कदाहरण- वायु, जल, मिट्टी, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि प्राकृतिक संसाधन हैं।
2. तीन Rs में से पहले ‘R’ के नियम को समझाइए।
उत्तर – पहले ‘R’ का अर्थ है Reduce अर्थात् कम करना। इसका यह अर्थ है कि हमें कम-से-कम वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम बिजली के पंखे तथा बल्ब के स्विच बंद करके विद्युत् के अपव्यय को रोक सकते हैं। इसी प्रकार कम-से-कम जल का उपयोग करके तथा लीक होने वाले नल तथा पाइप की मरम्मत करवा के भी हम जल के अपव्यय को रोक सकते हैं।
3. तीन Rs में से दूसरे ‘R’ का क्या अर्थ है ?
उत्तर – दूसरे ‘R’ का अर्थ है Recycle अर्थात् पुनः चक्रण। इसका अर्थ है कि हमें प्लास्टिक, कागज, काँच, धातु की वस्तुएँ आदि पदार्थों का पुनः चक्रण करके इनसे उपयोगी वस्तुएँ बनानी चाहिए। हमें ऐसी चीजों को कचरे के डिब्बे में नहीं डालना चाहिए बल्कि इन्हें अपने कचरे से अलग करना होगा ताकि यह दुबारा उपयोगी बनाई जा सके।
4. तीन Rs में तीसरे ‘R’ का क्या महत्त्व हैं ?
उत्तर – तीसरा ‘R’ है Reuse अर्थात् पुनः उपयोग। यह पुनःचक्रण से भी अच्छा क्योंकि पुनःचक्रण से भी कुछ न कुछ ऊर्जा व्यर्थ जाती है। पुनः उपयोग के तरीके ही वस्तु का बार-बार उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण—विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आए डिब्बे तथा केन हम अन्य सामान रखने में प्रयोग कर सकते हैं।
5. गंगा कहाँ से कहाँ तक यात्रा करती है तथा इसे नाले में कैसे परिवर्तित कर दिया गया है ?
उत्तर – गंगा हिमालय में स्थित गंगोत्री बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 तक की यात्रा करती है। इसके किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के 100 से अधिक नगरों ने इसे एक नाले में परिवर्तित कर दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरे एवं मल को इसमें प्रवाहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलापों जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, मृत और व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना भी इसके प्रदूषण का कारण है और फिर उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा का प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा दिया है कि इसके विषैले जल में मछलियाँ मरने लगी हैं।
6. चनों के कुछ उपयोग बताइए।
उत्तर – वनों के उपयोग– वनों के उपयोग निम्नलिखित हैं—
- वन मकान तथा फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं।
- वन वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात को बनाए रखते हैं।
- वन पृथ्वी पर जलचक्र का नियमन करते हैं।
- वन पेपर उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं।
- वन सौर विकिरणों से हमारी रक्षा करते हैं।
- वन हमें दवाइयाँ, फल तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ देते हैं।
- वन वन्य जीवन की रक्षा करते हैं।
7. बड़े बाँध बनाने के विरोध में कौन-सी तीन समस्याओं की चर्चा विशेष रूप से होती है।
उत्तर –
- सामाजिक समस्याएँ- इससे बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होते हैं। उन्हें अपना बसा – बसाया घर छोड़ना पड़ता है।
- आर्थिक समस्याएँ- इनमें सामान्य जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ अपेक्षित नहीं है।
- पर्यावरणीय समस्याएँ — इससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है। जैव विविधता को अपूर्णीय क्षति होती है। पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
8. जल संभर प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है ?
उत्तर – जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है ताकि ‘जैव-मात्रा’ उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीय संसाधन पौधों एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा न हो।
9. भौम जल के क्या लाभ हैं ?
उत्तर –
- यह जल वाष्पित होकर वायुमंडल में मिलता नहीं है।
- इसमें जीव जंतु तथा पादपों का जनन नहीं हो पाता।
- यह भौम स्तर में सुधार लाता है।
- यह पौधों को नमी प्रदान करता है।
- यह जीव-जंतुओं के कारण प्रदूषित और संदूषित नहीं हो पाता ।
10. “जल जीवन के लिए आवश्यक है। “- इस कथन को सिद्ध कीजिए।
उत्तर – जल निम्नलिखित कारणों से जीवन के लिए आवश्यक है-
- जल हमारे शरीर की सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है।
- जल शरीर में तापमान को स्थिर रखता है।
- जल पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है।
- जल मल-मूत्र के विसर्जन में सहायता करता है।
- जल पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है।
- कृषि, कारखानों तथा विद्युत के लिए भी जल आवश्यक है।
11. जल संरक्षण के कुछ प्रमुख उपाय लिखिए।
उत्तर – जल के संरक्षण हेतु उपाय –
- जल को सिंचाई के लिए उपयोग करना।
- बाढ़ नियंत्र तथा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और बाँध निर्माण करना ।
- भूमिगत जल की रिचार्जिंग तथा व्यय को रोकना।
- अधिक जल तथा कम जल वाले स्थानों को स्थानांतरण करना।
- मृदा अपरदन को रोकने के लिए बाह्य मृदा को बनाए रखना ।
12. वनों के कटने से क्या हानि होती है ?
उत्तर – यदि वृक्षों के कटने की दर उनकी वृद्धि से अधिक हो तो वृक्षों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जाएगी। वृक्ष वाष्पण की क्रिया से बड़ी मात्रा में जल मुक्त करते हैं। इससे वर्षा वाले बादल आसानी से बनते हैं। जब वन कम हो जाते हैं तब उस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। इससे वृक्ष कम संख्या में उग पाते हैं। इस प्रकार एक दुष्चक्र आरंभ हो जाता है और वह क्षेत्र रेगिस्तान भी बन सकता है। वृक्षों के बहुत अधिक मात्रा में कटने से जैव पदार्थों से समृद्ध मिट्टी की सबसे ऊपरी परत वर्षा के पानी के साथ बहकर लुप्त होने लगती है।
13. ‘कुल्ह’ क्या है ? इनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाता था ?
उत्तर – लगभग 400 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ जिसे ‘कुल्ह’ कहा जाता है। झरनों के बहने वाले जल को मानव द्वारा बनाई गई छोटी-छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गाँवों तक ले जाता है। इनसे मिलने वाले जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गाँवों की आपसी सहमति से किया जाता था। कृषि के मौसम में
जल सबसे पहले दूरस्थ गाँव को दिया जाता था। कुल्ह की देख-रेख एवं प्रबंध के लिए दो या तीन लोग रखे जाते थे, जिन्हें गाँव वाले वेतन देते थे। सिंचाई के अतिरिक्त इन कुल्ह से जल का भूमि में अंत: स्रवण भी होता रहता था जो विभिन्न स्थानों पर झरने को भी जल प्रदान करता रहता था। सरकार द्वारा इनके अधिग्रहण के बाद ये प्रायः निष्क्रिय हो गए।
14. वन एवं वन्यजीव के संरक्षण में आदिवासियों की क्या भूमिका है ? उल्लेख करें।
उत्तर – आदिवासियों के निम्नलिखित क्रियाकलापों में वन एवं वन्यजीव के संरक्षण की भावना स्पष्ट दिखती है।
- कई वृक्षों जैसे पीपल, वट आदि पर ईश्वर का आवास मानकर उनकी पूजा करना, उन्हें कटने न देना।
- वन के किसी विशेष क्षेत्र को पवित्र उपवन (sacred groves) मानना तथा उसे मानव गतिविधियों से वर्जित रखना।
- गर्भधारण कर चुके मादा पशुओं का शिकार न करना ।
- प्रजननकाल में जंतुओं को आश्रय तथा सुरक्षा देना।
15. वन्य जीव किसे कहते हैं ? वन्य जीवों के संरक्षण का क्या आशय है ?
उत्तर – जंतुओं और वनस्पतियों की वैसी असंवर्धित प्रजातियाँ जो अपने प्राकृतिक वास स्थानों में पाई जाती है, वन्य जीव कहलाती हैं।
वन्य जीवों की सामान्य तथा संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखना तथा उन्हें लुप्त होने से बचाना वन्य जीव संरक्षण कहलाते हैं।
16. वन्य जीवों के संरक्षण के क्या उद्देश्य हैं ?
उत्तर –
- वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखना तथा उन्हें लुप्त होने से बचाना।
- लुप्त होने के कगार पर पहुँचे वन्य जीवों के नस्ल को सुरक्षित रखना।
- प्राकृतिक वातावरण में जंतुओं और वनस्पतियों के बीच तथा उनकी अलग-अलग प्रजातियों के बीच के पारिस्थितियकी संबंधों को स्थापित रखना।
17. अतिसंकटापन्न / अतिसंकटग्रस्त वन्य जंतुओं के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई जानेवाली कुछ परियोजनाओं का उल्लेख करें।
उत्तर –
- भारतीय बाघ के संरक्षण हेतु भारत के विभिन्न राज्यों में बाघ परियोजना के अंतर्गत अब तक 28 बाघ रिजर्व स्थापित किए गए हैं।
- भारतीय हाथी के संरक्षण के उद्देश्य से 17 हाथी रिजर्व स्थापित किए गए हैं।
- घड़ियालों के संरक्षण के लिए घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है।
- हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ परियोजना चलाई जा रही है।
18. वन तथा वन्य जीव हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं ?
उत्तर – वन पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। स्थानीय निवासियों के लिए वन जलावन एवं छाजन के लिए लकड़ी तथा झोपड़ी बनाने, भोजन एकत्र करने एवं उसके भंडारण के लिए बाँस की आपूर्ति करते हैं। खेती के औजार, मछली पकड़ने एवं शिकार के औजार मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं जो वनों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त वन मछली पकड़ने एवं शिकार-स्थल भी होते हैं। वन पशुओं के चारा, औषधि हेतु वनस्पति, फल, काष्ठ- फल (nut), रेजिन, रबर आदि की आपूर्ति करते हैं। वनों द्वारा वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है तथा वातावरण के ताप में कमी आती है। पेड़-पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को बाँधकर रखते हैं, जिससे तेज वर्षा तथा वायु के झोंके से होनेवाले भूमि अपरदन रुकता है। वन मिट्टी कटाव रोकने में सहायक होते हैं। जल चक्र के पूर्ण होने तथा वातावरण में CO2 और O2 के संतुलन को कायम रखने में पेड़-पौधे सहायक होते हैं। वनों के ह्रास से कई प्रकार की जैव-प्रजातियाँ लुप्त हो जाती हैं। अनेक उद्योग इमारती लकड़ी, कागज, लाख, खेल के सामान, औषधीय पौधों आदि के लिए वनों पर निर्भर करते हैं।
19. पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन-से परिवर्त्तन ला सकते हैं ?
उत्तर – (क) धुआँरहित वाहनों का प्रयोग करके । (ख) पॉलीथीन का उपयोग न करना । (ग) जल संरक्षण को बढ़ावा देकर । (घ) वनों की कटाई पर रोक लगाकर। (ङ) वृक्षारोपण | (च) तेल से चालित वाहनों का कम-से-कम उपयोग करके |
उपर्युक्त विभिन्न विधियों को अपनाकर हम पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं।
20. क्या आपके विचार में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए ? संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन-कौन-सी ताकतें कार्य कर सकती हैं?
उत्तर – आर्थिक विकास का पर्यावरण संरक्षण के साथ सीधा संबंध है। संसार में संसाधनों का असमान वितरण गरीबी का एक मुख्य कारण है। संसाधनों का समान वितरण एक शांतिपूर्ण संसार की स्थापना कर सकता है।
21. हमें वन एवं वन्यजीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए ?
उत्तर – वन्यजीव को निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित रखना चाहिए— 1. प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने के लिए। 2. जीन पूल की सुरक्षा के
लिए ।
वन्यजीव का संरक्षण राष्ट्रीय पार्क तथा पशुओं और पक्षियों के लिए शरण स्थल बनाने से किया जा सकता है। यह पशुओं का शिकार करने की निषेधाज्ञा का कानून प्राप्त करके किया जा सकता है।
22. संरक्षण के लिए कुछ उपाय बताएँ ।
उत्तर – पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने के लिए वन्यजीव का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित दो उपाय किये जा सकते हैं 1. सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे शिकारियों को प्रतिबंधित वन्य पशु का शिकार करने पर दण्ड मिलना चाहिए। 2. राष्ट्रीय पार्क और पशु-पक्षी विहार स्थापित किये जाने चाहिए जहाँ पर वन्य पशु सुरक्षित रह सकें।
23. इस अध्याय में उठाये बिन्दुओं (समस्याओं) के आधार पर अपने जीवन-शैली में क्या परिवर्त्तन लाना चाहेंगे जिससे हमारे संसाधनों के संप्रदूषण बढ़ावा मिल सके ?
उत्तर –
- हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम एक समाज में रहते हैं, अकेले नहीं ।
- हमें अपने संसाधनों का कम-से-कम उपयोग करना चाहिए तथा किसी भी तरह उन्हें व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
- हमें तीन (R’s) के नियमों का पालन करना चाहिए – (Reduce, Recycle, Reuse ) ।
- हमें निजी वाहनों की अपेक्षा सरकारी वाहनों का उपयोग करना चाहिए।
- हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को अपने जीवन में महत्त्व देकर हम अपने संसाधनों के संप्रदूषण को बढ़ावा दे सकते हैं।
24. जल का संरक्षण एवं प्रबंधन की उपयोगिता को समझाएँ ।
उत्तर – जल मानव तथा वन्य जीवों के जीवन का मुख्य आधार है। जल के बिना जीवन संभव नहीं। हमारी दिनचर्या जल के उपयोग के साथ ही प्रारंभ होती है। शौच क्रिया, स्नान, बर्तन, कपड़े धोने व पीने तथा भोजन बनाने में जल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आधुनिक समय में तकनीकी विकास के कारण जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल यातायात तथा उपयोग आदि के लिए किया जाता रहा है। जल की माँग में काफी वृद्धि हुई है. परन्तु जल की उपलब्धता में कमी आई है। जल की उपलब्धता में कमी के मुख्य कारण जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव है। अतः, जल संसाधन का उपयोग सुनियोजित ढंग से करके तथा जल स्रोतों का उचित प्रबंधन करके हम जल प्रणाली का संरक्षण कर सकते हैं।
25. बाँध निर्माण से होने वाले पर्यावरणीय समस्याओं का विवेचन करें।
उत्तर – बाँध निर्माण से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएँ :
पुनर्वास की समस्या – टिहरी बाँध के निर्माण के फलस्वरूप हजारों लोगों की पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में बसना पड़ा। पर्वतीय लोगों को पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्रों में बसने से उनकी जीवन-शैली में परिवर्तन आया जिससे उन लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विस्थापितों को जल, लकड़ी, फल अपेक्षाकृत महँगे मिलने लगे तथा सरकार द्वारा समुचित मुआवजा भी नहीं मिल पाया।
सुरक्षा की समस्या – चूँकि टिहरी बाँध भूकम्पीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है अतः भूकम्प से टिहरी बाँध के टूटने का डर बना रहेगा। टिहरी बाँध के टूटने से ऋषिकेश और हरिद्वार नगर प्रभावित हो सकते हैं तथा बाँध का जल आस-पास के क्षेत्र में फैलकर भारी तबाही मचा सकता है।
26. वायुमण्डल का निर्माण कैसे हुआ तथा इसमें परिवर्तन कैसे हुआ ?
उत्तर – प्रारंभिक काल में पृथ्वी का आकार काफी बड़ा था और वह काफी ठण्डी थी। तब पृथ्वी का कोई वायुमण्डल नहीं था। इसके बाद पृथ्वी ने सिकुड़ना शुरू किया जिस कारण यह छोटी तथा गर्म होती गयी। इस दौरान गैस विमोचित हुई तथा वायुमण्डल बना। वायुमण्डल में कई प्रकार की गैसें इकट्ठी हुईं। जब परपोषी से स्वपोषी का निर्माण हुआ तो ऑक्सीजन भी स्वतंत्र रूप से बना। वायुमण्डल के अन्य घटक ज्वालामुखी के फटने पर बनते गए।
27. वनों के संरक्षण से क्या लाभ हैं ?
उत्तर – (i) भूमि की उर्वरता बनी रहती है। (ii) मृदा अ अपर नहीं होता है। (iii) वातावरणीय प्रदूषण दूर होता है। (iv) वृक्ष सुरक्षित रहते हैं। (v) वर्षा समय पर और समुचित होती है। (vi) वनों के संरक्षण से वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। (vii) वनों के संरक्षण तथा उनके उचित उपयोग से बहुत से औद्योगिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे— लाख, गोंद आदि ।
28. ध्वनी प्रदूषण क्या है ? यह किस प्रकार होता है ?
उत्तर – महानगरों में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ वातावरण को अत्यधिक दूषित करती हैं, जिसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण तीव्र ध्वनि अथवा शोर या कोलाहल है। तीव्र ध्वनि कानों को अप्रिय लगती ही है, मानव के वार्तालाप व व्यवहार में बाधा भी डालती है, इसे शोर या कोलाहल कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के निम्नांकित कारण हैं—(i) कारखानों की ध्वनि, (ii) जेट विमानों की ध्वनि, (iii) मोटर, ट्रक आदि वाहनों की ध्वनि, (iv) लाउडस्पीकर तथा अन्य वाद्य-यंत्रों से निकली ध्वनि, (v) बम फटने तथा पटाखे छूटने की ध्वनि (आकस्मिक ध्वनि) आदि।
29. ध्वनि प्रदूषण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ?
उत्तर – तीव्र ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण से हमारे ऊपर निम्नांकित प्रभाव हो सकते हैं – (i) श्रवण शक्ति का कम हो जाना, (ii) तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव, (iii) मानसिक तनाव, (iv) रक्तचाप बढ़ जाना, (v) हृदय रोगों की सम्भावना, (vi) थकान का अनुभव, (vii) अनिद्रा आदि।
30. अम्ल वृष्टि (acid rain) क्या है ? इसका कारण क्या है ?
उत्तर – मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न कर रहा है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उद्योगों से निकलने वाले धुएँ एवं रसायन जलवायु को दूषित कर रहे हैं। दहन इंजनों द्वारा प्रचालित वाहन तथा कारखाने वायु में सल्फर यौगिकों की बड़ी मात्रा मुक्त कर रहे हैं। ये यौगिक वर्षा जल में घुलकर जल को अम्लीय बना देते हैं, जो वाष्प बनकर वायुमंडल में चले जाते हैं। इन वाष्पों के संघनित होकर बरसने की क्रिया अम्ल वृष्टि (acid rain) कहलाती है।
अम्ल वृष्टि से पौधों, जीवों तथा ऐतिहासिक स्मारकों को हानि पहुँचती है।
31. भौम जल-स्तर किसे कहते हैं ?
उत्तर – धरती पर होने वाली वर्षा का कुछ भाग वाष्पित हो जाता है, कुछ भाग नदी, नालों में बह जाता है, इसका थोड़ा भाग भूमि में रिस कर अंदर पहुँचता है। मृदा कणों के बीच के स्थान रंध्राकाश (pore space) कहलाते हैं। ये रंध्राकाश वायु तथा जल दोनों से ही भरे होते हैं। परन्तु निश्चित गहराई के नीचे समस्त रंध्राकाश केवल जल से भरे रहते हैं। इस गहराई को भौम जल-स्तर (water table) कहते हैं ।
32. वन वर्धन किसे कहते हैं ?
उत्तर – वनों के संरक्षण के लिए या पुनः चक्रण के लिए अधिक मात्रा में पेड़-पौधे उगाना वन वर्धन कहलाता है। जुलाई-अगस्त में वन महोत्सव मनाया जाता है। इस समय अधिक मात्रा में पौधे लगाए जाते हैं।
33. प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास से जनसंख्या वृद्धि हुई है, क्यों ?
उत्तर – जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ अनेक आवश्यकताएँ भी उभर कर सामने आ रही हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक सम्पदाओं का ह्रास हो रहा है। प्राकृतिक समस्याएँ प्रचुर मात्रा में होते हुए भी सीमित है जबकि जनसंख्या चरम सीमा पर पहुँच गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी प्राप्त संसाधन सीमित हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि अधिक होती गई तो प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त सम्पदाएँ अपना संतुलन बनाए रखने में समर्थ नहीं होगी।
34. ऊर्जा संकट से क्या अभिप्राय है ? इस कथन की पुष्टि कीजिए।
उत्तर – प्रकृति में कुछ ऐसे साधन हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। जैसे— खनिज, कोयला, मिट्टी का तेल आदि। इन पदार्थों को हम ईंधन तथा ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। इन साधनों का प्रयोग हमें मितव्ययिता से करना चाहिए नहीं तो कुछ ही समय में ये प्राकृतिक स्रोत समाप्त हो जाएँगे और मानव जाति को भयंकर संकट का सामना करना पड़ेगा। इन सभी वस्तुओं का अभाव ऊर्जा संकट कहलाता है।
35. जैव पर्यावरण का निर्माण कैसे हुआ ? जैव तथा अजैव पर्यावरण किन कारणों से जनसंख्या को प्रभावित करते हैं ?
उत्तर – पर्यावरण वह भौतिक एवं जैव संसार है जिसमें हम रहते हैं। जैव तथा अजैव घटकों में प्रतिदिन परस्पर प्रक्रियाएँ होती रहती हैं। जैव पर्यावरण में समस्त पौधे, जन्तु, मानव आदि सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर अनुकूल परिस्थितियों के होने से एककोशिकीय जीव के रूप में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति सागर में हुई। इन्हीं एककोशिकीय जीवों से कालान्तर में अधिक जटिल बहुकोशिकीय तथा बड़े जीवों का विकास हुआ। सूक्ष्मजीव, पौधे तथा जन्तु सम्मिलित रूप से जैव पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
जैव तथा अजैव दोनों ही भिन्न कारणों से जनसंख्या के आकार को प्रभावित करके उनमें अनेक परिवर्त्तन प्रेरित करते हैं या कर सकते हैं। ये हैं— (i) पोषण उपलब्धता, (ii) उपलब्ध स्थान, (iii) अन्य जीवों के साथ पारस्परिक क्रिया, (iv) जलवायु ।
36. भारत के किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखें, जिनके विलुप्त होने का खतरा उपस्थित हो गया है।
उत्तर – भारत के दो जंतुओं के नाम इस प्रकार हैं जिनके विलुप्त होने का खतरा उपस्ि गया है—(i) बाघ, (ii) गैंडा।
37. वन्यजीव संरक्षण क्यों आवश्यक है ? वन्य जीव को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है?
उत्तर – वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता के कुछ पहलू इस प्रकार हैं— (i) प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने के लिए। (ii) जीन पूल की सुरक्षा के लिए ।
वन्यजीव का संरक्षण राष्ट्रीय पार्क तथा पशुओं और पक्षियों के लिए शरणस्थल बनाकर किया जा सकता है। पशुओं के शिकार करने की निषेधाज्ञा कानून पास करके भी इन्हें संरक्षित किया जा सकता है।
38. वायू प्रदूषण का लम्बे समय के बाद क्या प्रभाव होगा ?
उत्तर – यदि वायु प्रदूषण लम्बे समय तक होता रहा तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी जिससे अनेक हानियाँ होगीं जो निम्नलिखित हैं—(i) श्वसन संबंधी विकार पैदा होने लगेंगे। (ii) पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगेगी, क्योंकि CO2 इन्फ्रारेड (अवरक्त) किरणों को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देती है। (iii) तापमान बराबर बढ़ता जाएगा जिससे ध्रुवों और ग्लेशियरों की बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। (iv) बर्फ पिघलने से समुद्र तल बढ़ जाएगा और प्रबल ज्वार लहरें उठेंगी जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा। (v) हरा घर प्रभाव (Green house effect) उत्पन्न होने लगेंगे। (vi) अम्ल वर्षा (Acid rain) की संभावना बढ़ जाएगी। (vii) पत्थर कैंसर (Stone cancer) से चट्टान एवं पहाड़ियाँ क्षतिग्रस्त होने लगेंगी तथा (viii) काला बर्फ का गिरना (Black snow fall) शुरू हो जाएगा।
39. पर्यावरण प्रदूषित कब होता है ?
उत्तर – प्रकृति एक सीमा तक प्रदूषण को नियंत्रित रख सकती है। प्रकृति में वैसे प्राकृतिक साधन हैं जिनसे पर्यावरण को स्वच्छता प्रदान होती है। कभी किसी अकस्मात दुर्घटना से पर्यावरण इस कदर प्रभावित हो जाता है कि स्वच्छता के प्राकृतिक साधन उसे पुन: स्वच्छ कर संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकृति का संतुलन इस सीमा तक बिगड़ जाता है कि उसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता तभी प्रदूषण होता है अर्थात् पर्यावरण प्रदूषित कहा जाता है।
40. पर्यावरण को मानव ही प्रदूषित करता है कैसे ? कोई तीन उदाहरण दीजिए।
उत्तर – निम्न कारणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में मानव स्वयं जिम्मेवार है – (i) प्राकृतिक स्रोतों का आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषित होता है क्योंकि प्रकृति एक सीमा तक ही प्रदूषण को नियन्त्रित रख सकती है। (ii) अत्यधिक औद्योगीकरण से अनेक रसायनों तथा अपशिष्ट पदार्थों को नदी के पानी में बहा दिया जाता है। इस प्रदूषित पानी को सूक्ष्मजीव, शैवाल या अन्य प्राकृतिक साधन पूर्णतया स्वच्छ करने में असमर्थ होते हैं तथा परिणाम होता है प्रदूषण की वृद्धि। (iii) कारखानों द्वारा वाहनों द्वारा धुआँ तथा गैसों का छोड़ा जाना वायु को प्रदूषित करता है। उर्वरकों एवं कीटनाशकों जैसे रसायनों का फसलों पर छिड़काव आदि भी प्रदूषण को बढ़ाते हैं। उत्तर>
41. अपशिष्ट पदार्थ क्या है ? उनको किन-किन वर्गों में बाँटा जा सकता है ? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए।
उत्तर – अपशिष्ट पदार्थ मानव के विभिन्न कार्यकलापों के परिणाम से जो पदार्थ शेष बच जाते हैं उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं अपशिष्ट पदार्थों को दो भागों में बाँटा जाता है।
- जैव निम्नीकरणीय- ये पदार्थ कुछ जीवाणुओं द्वारा निराविषी पदार्थों में अवक्रमित हो सकते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण भी सम्भव होता है जैसे गोबर से गोबर गैस प्राप्त करना, जिससे ऊर्जा उत्पादित होती है। कम्पोस्ट का उपयोग भी जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों के पुनःचक्रण का उदाहरण है।
- जैव अनिम्नीकरणीय जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों को सरलता से निराविष नहीं किया जा सकता है जैसे ऐलुमिनियम के डिब्बे, प्लास्टिक, डी. डी. टी. आदि पदार्थ जो प्रमुख प्रदूषक हैं। जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों में अधिक हानिप्रद पदार्थ रेडियोएक्टिव अपशिष्ट पदार्थ है। ये अपशिष्ट पदार्थ कुछ ही समय में दूर-दूर तक फैल जाते हैं तथा पर्यावरण को प्रदूषित तथा विषाक्त बना देते हैं।
42. प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास में जनसंख्या वृद्धि का कितना हाथ है
उत्तर – जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ अनेक आवश्यकताएँ भी उभर कर सामने आ रही हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक सम्पदाओं का ह्रास हो रहा है। प्राकृतिक सम्पदा प्रचुर मात्रा में होते हुए भी सीमित हैं जबकि जनसंख्या चरम सीमा पर पहुँच गई है। बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अधिक करने लगी है। अन्तः दहन इंजनों द्वारा चलने वाले वाहन तथा कारखाने वायु में बड़ी मात्रा में सल्फर यौगिकों को मुक्त करते हैं। वर्षा के दौरान ये यौगिक जल में घुलकर अम्लीय वर्षा करते हैं। यह अम्लीय वर्षा या अम्लीय जल पौधों एवं ऐतिहासिक स्मारकों के लिए हानिकारक है।
43. तम्बाकू का धुआँ किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ?
उत्तर – तम्बाकू में निकोटिन होता है जो उत्तेजक तथा विष दोनों होता है। कुछ लोग सिगरेट, हुक्का, गड़गड़ा, चुरुट, सिगार, बीड़ी इत्यादि पीते हैं। इस तरह लोग अपने शरीर में तम्बाकू का अन्तर्ग्रहण करते हैं। तम्बाकू के लगातार सेवन के फलस्वरूप नाक, गला तथा फेफड़ों में धीरे-धीरे टार एकत्र हो जाते हैं जिसके कारण खाँसी तथा गले में खराश उत्पन्न होते हैं। तम्बाकू के सेवन से रक्तचाप अस्थायी रूप से बढ़ जाता है जिसके कारण हृदय पर दबाव पड़ता है और हृदय स्पंदने प्रभावित होता है। इसके लगातार सेवन से फेफड़ों में कैंसर होने की तथा हृदय गति रुक जाने की संभावना बढ़ जाता है। बीड़ी तथा सिगरेट के धुएँ में कार्बन मोनोक्साइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड गैस भी होती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। E
44. वायु एवं जल प्रदूषण किन-किन कारणों से होता है ?
उत्तर – औद्योगिक क्रान्ति से प्रदूषण में वृद्धि हुई है। कारखानों तथा वाहनों के धुएँ एवं गैसों से वायु प्रदूषित होती है। उर्वरकों तथा कीटनाशकों के फसलों पर छिड़काव द्वारा वायु तथा जल दोनों ही प्रदूषित होते हैं। ये रसायन वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों तक पहुँच जाते हैं तथा मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल एवं वायु को प्रदूषित करते हैं।
45. ऊर्जा प्रग्रहण क्या है ?
उत्तर – सूर्य की रोशनी में उपस्थित विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करने की क्रिया ऊर्जा-प्रग्रहण (Trapping of energy) कहलाती है। जीवमंडल में उपस्थित केवल हरे पौधे ही इस ऊर्जा को प्रग्रहित करने में सक्षम होते हैं। हरे पौधों की कोशिकाओं में हरे रंग का पदार्थ रहता है जिसे पर्णहरित (chlorophyll) कहते हैं। यही पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को प्रग्रहित करने में सक्षम होता है। प्रकाश-संश्लेषण क्रिया द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट अणुओं के रासायनिक बंधों में सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रूपांतरित होकर विभव ऊर्जा (Potential energy) के रूप में संचित रहती है। जब जन्तु पौधों को खाते हैं तो संग्रहित विभव ऊर्जा को ग्रहित करते हैं।
46. नदी तट पर कारखाना लगाने से उसके निकटवर्ती पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
उत्तर – नदी तट पर कारखाना लगाने से अनेक प्रकार के रसायन जल में मिलने लगेंगे। इससे जल प्रदूषित हो जायगा। कारखानों से निकलकर नदी में मिलने वाला गर्म मलवा जल के तापक्रम क बढ़ा देगा जिससे जल में मौजूद पौधे मर जायेंगे। इससे जल में COD (Chemical Oxygen Demand) एवं BOD (Biological Oxygen Demand) हो जायेगा। फलतः जलीय जन्तु ऑ लीजन के अभाव में मरने लगेंगे। प्रदूषित जल पीने, खाना बनाने, बॉयलरों इत्यादि के लिए अनु ग्युक्त है।
47. वनों का परिपूर्ण होना क्यों आवश्यक है ?
उत्तर – वनों का मृदा संरक्षण तथा वृष्टि से पारस्परिक घना सम्बन्ध है। यदि वृक्षों को काटने की दर उनकी वृद्धि से अधिक हो जाए तो वृक्षों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जाती है और क्षेत्र धीरे-धीरे रेगिस्तान भी बन सकता है।
वृक्ष वाष्पोत्सर्जन द्वारा विशाल मात्रा में जल मुक्त करते हैं। इस मुक्त जलवाष्प से बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है अर्थात् जल चक्रण में सहायक हैं। अतः वनों के परिपूर्ण होने से वातावरण संतुलित रहता है।
48. जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट तथा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों में अन्तर बताएँ। प्रत्येक के दो उचित उदाहरण दें।
उत्तर – जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट तथा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों में निम्नलिखित अन्तर हैं—
| जैव निम्नीकरणीय | अजैव निम्नीकरणीय |
| 1. ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है; जैसे—गोबर। | 1. ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें अहानिकारक पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है; जैसे— डी.डी.टी., प्लास्टिक आदि । |
| 2. ये पदार्थ जीवाणुओं एवं फफूँदी द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तन्त्र में सन्तुलन बनाए रहता है। | 2. ये पदार्थ बैक्टीरिया एवं फफूँदी द्वारा अपघटित नहीं होते। |
49. कृषि की नवीन विकास प्रक्रियाओं से हमारा पर्यावरण किस प्रकार दूषित हो रहा है ?
उत्तर –
- रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण फैल रहा है।
- रासायनिक कीटनाशी के अधिक उपयोग से प्राकृतिक जैव संतुलन प्रभावित हो रहा है।
- मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है।
- फसलों में नवीन बीमारियाँ हो रही हैं।
- रासायनिक उर्वरक की प्रतिक्रिया से जगह-जगह भूमि की लवणीयता बढ़ रही है तथा कहीं-कहीं उसके ऊपर होने के लक्षण प्रकट हो रहे हैं।
50. फसल – चक्रण ( फसल-आवर्तन) से क्या समझते हैं ?
उत्तर – इस प्रणाली में एक ही कृषिभूमि पर बदल-बदलकर अनुक्रम से एक से अधिक फसल उगाई जाती है, जैसे गेहूँ और मकई (मक्का) के बीच दलहन की एक फसल उगाना। इस प्रणाली. को अपनाने से मिट्टी में पोषक तत्त्वों का पुनः परिपूरण हो जाता है। हमें ज्ञात है कि दलहन (फलीदार पौधे) की जड़ की गाँठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी में स्थापित करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति पुनर्स्थापित हो जाती है।
51. पारिस्थितिकी – अनुकूल कृषि से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर – यह ऐसी कृषि प्रणाली है जिसके उपयोग से अधिक कृषि उत्पाद प्राप्त होने के साथ-साथ पर्यावरण के प्रदूषित होने की संभावना कम-से-कम होती है। पारिस्थितिकी – अनुकूल कृषि प्रणाली में रासायनिक उर्वरक के बदले कार्बनिक एवं जैव उर्वरक की सलाह दी जाती है। इसी प्रकार, पीड़क नियंत्रण के लिए रासायनिक कीटनाशी या पीड़कनाशी के स्थान पर एकीकृत पीड़क प्रबंधन (Integrated Pest Management, IPM) का उपयोग किया जाता है।
52. एकीकृत पौड़क प्रबंधन पीड़कों के नियंत्रण की श्रेष्ठ विधि है। कैसे ?
उत्तर – यह विधि वास्तव में पीड़कों की नियंत्रण विधि नहीं है, बल्कि यह पीड़कों के प्रबंधन की विधि है। इसका उद्देश्य पीड़कों को पूर्ण सफाया कर प्रकृति में जैविक असंतुलन उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि उनकी संख्या या घनत्व को इतना सीमित रखना है कि उनसे आर्थिक क्षति न हो। एकीकृत पीड़क प्रबंधन रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा अधिक सुरक्षित तथा कम खर्चीला है। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसके उपयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है।
53. जैव उर्वरक क्या है ?
उत्तर – कई सूक्ष्मजीवों, जैसे उत्तरकुछ बैक्टीरिया तथा कुछ शैवालों का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। कई बैक्टीरिया (जैसे राइजोबियम) वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्षमता रखते हैं। पौधे इस नाइट्रेट का उपयोग वनस्पति प्रोटीन बनाने में करते हैं।
एजोटोबैक्टर तथा क्लॉस्ट्रिडियम नामक बैक्टीरिया मिट्टी में मुक्तजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। धान के खेतों में बहुतायत में पाए जानेवाले नीलहरित शैवाल भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये सभी सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक कहलाते हैं।
54. मृदा में वायुमंडलीयू नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है ?
उत्तर – कुछ बैक्टौरिया, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर तथा क्लॉस्ट्रिडियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे बैक्टीरियाओं में से कई कुछ किस्म के पौधों की जड़ों में परजीवी के रूप में होते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया मुक्तजीवी के रूप में मिट्टी में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी में छोड़ देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है।
55. प्राकृतिक संसाधन की धारणीयता के दृष्टिकोण से मानवकृत रेशा का वस्त्र उत्पादन में क्या महत्त्व है ?
उत्तर – मानव की दो मूल आवश्यकताओं— भोजन एवं वस्त्र — में भोजन का महत्त्व वस्त्र से पहले है। चूँकि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन पूर्णत: मिट्टी पर ही निर्भर है, अतः वस्त्र के लिए वानस्पतिक रेशों (जैसे कपास) पर दबाव जितना कम होगा, खाद्यान्न उत्पादन के लिए उतना ही ज्यादा कृषिभूमि उपलब्ध हो पाएगी। इसी कारण से प्राकृतिक रेशों के विकल्प के रूप में मानवकृत रेशों का महत्त्व बढ़ गया है। वस्त्रों के निर्माण में मानवकृत रेशों के अधिकाधिक उपयोग से प्राकृतिक रेशों की केवल धारणीयता ही नहीं बढ़ती है, बल्कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषिभूमि भी ज्यादा उपलब्ध हो जाती है।
56. प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रमुख अधिनियमों का उल्लेख करें।
उत्तर –
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वायु ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
इन अधिनियमों के अंतर्गत पर्यावरण के विभिन्न अजैव अवयवों, जैसे जल, वायु, मृदा तथा जैव अवयव (विभिन्न वनस्पति एवं जंतु) को प्रदूषण से होनेवाले हानियों से बचाने तथा उनके संरक्षण हेतु प्रावधान हैं।
57. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख करें।
उत्तर –
- वन्य जीवों के शिकार को विनियमित करना।
- जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान जैसे क्षेत्रों को घोषित करना।
- वन्य जीवों से अवैध रूप से निर्मित वस्तुओं के व्यापार को रोकने की प्रक्रिया के लिए नियम बनाना।
- अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करनेवालों के लिए उचित दंड निर्धारित करना ।
- हरेक प्रांत में एक वन्य जीव सलाहकार बोर्ड (पर्षद) की स्थापना करना ।
58. मनुष्यों का पशुओं के प्रति क्रूरता के मुख्य कारण क्या हैं?
उत्तर –
- दुर्लभ पशु-वस्तुओं, जैसे शेर, बाघ, चीता, हिरण के खाल, हाथीदाँत गैंडा एवं हिरण के सींग, मृग-कस्तूरी आदि के लिए पशुओं का शिकार।
- संपन्न व्यक्तियों द्वारा अपने शौक एवं मनोरंजन के लिए वन्य पशुओं का शिकार।
- सर्कस में वन्य पशुओं द्वारा मनोरंजक करतब दिखाने के लिए उनपर किए गए अत्याचार।
- कई धार्मिक स्थलों पर पशुओं की बलि देना।
- वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए पशुओं पर अत्याचार ।
59. किसी वस्तु का क्रय करते समय उपभोक्ताओं को किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
उत्तर – किसी वस्तु को क्रय करने से पूर्व उपभोक्ताओं को निम्नांकित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।
- क्रय की वस्तु का उत्पादक या विक्रेता के द्वारा गुणवत्ता अनुरक्षित हैं या नहीं ?
- क्रय की जानेवाली वस्तु का मूल्य उचित एवं निर्धारित है या नहीं ?
- अगर वस्तु माप-तौल से क्रय की जानेवाली है, तो उक्त वस्तु माप-तौल सही है या नहीं ?
- अगर एक ही वस्तु का उत्पादन कई उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्रय की जानेवाली वस्तु का चुनाव सही किया जा रहा है या नहीं ?
60. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है तथा यह किस वर्ष से लागू हुआ ?
उत्तर – भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, एक अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। यह अधिनियम 1986 से लागू है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने तथा उससे उपभोक्ताओं को राहत दिलाने का प्रावधान है।
61. खाद्य अपमिश्रण के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव के कोई तीन उदाहरण दें।
उत्तर –
- सरसों के तेल में आर्जीमोन या कटैया के बीज के तेल का अपमिश्रण किया जाता है। ऐसे तेल के सेवन से ड्रॉप्सी नामक बीमारी होती है। इससे आमाशय तथा आँत दुष्प्रभावित होते हैं।
- मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से पीसी हल्दी में लेड क्रोमेट की मिलावट की जारी है। ऐसी हल्दी के सेवन से, विशेषकर बच्चों में मानसिक बुद्धि दुष्प्रभावित होने लगती है।
- अरहर की दाल में खेसारी की दाल की मिलावट होती है। खेसारी दाल के लंबे समय तक सेवन से लेथाइरिज्म नामक रोग होता है।
62. पारि-क्लब या इको-क्लब क्या है ? इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?
उत्तर – पर्यावरण संबंधी गतिविधियों के संपादन के लिए भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले के 100 स्कूलों में पारि-क्लब स्थापित करने की एक वृहत योजना कार्य कर रही है। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं
- पर्यावरण तथा इसकी समस्याओं से बच्चों को परिचित कराना।
- स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण शिक्षा का अवसर देना ।
- समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना को जागृत करने हेतु विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।
63. CNG क्या है ? इससे क्या-क्या लाभ हैं ?
उत्तर – CNG उच्चदाब वाली एक प्राकृतिक गैस है। इसका व्यवहार डीजल की जगह वाहनों को चलाने में किया जाता है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं
- इससे उत्सर्जित धुएँ में वायु प्रदूषक सल्फर तथा सीसे की मात्रा नहीं होती है।
- उत्सर्जित धुएँ में कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा विविक्त पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है।
- बेंजीन तथा अन्य जहरीले पदार्थों का निष्कासन अत्यंत कम मात्रा में होता है।
- CNG में घटिया पदार्थों का अपमिश्रण नहीं हो सकता है।
64. वर्षाजल का सीधे उपयोग के लिए संचयन की एक साधारण विधि का वर्णन करें।
उत्तर – किसी मकान की तिरछी छत पर गिरनेवाले वर्षाजल का संचयन कर सीधे उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए एक बाँस के लंबे टुकड़े को लम्बाई में, बीचोबीच चीरकर खुली नाली का स्वरूप दिया जाता है। छत को तिरछी सतह पर गिरनेवाले वर्षाजल को इस नाली में एकत्र किया जाता है। इस नाली से बहकर वर्षाजल सीधे संचयन पात्र में इकट्ठा हो जाता है। इस जल का उपयोग घरेलू कार्यों के लिए किया जा सकता है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
1. इस प्रणाली का पेयजल व्यवस्था (पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्र अथवा पठार क्षेत्र) से तुलना करें।
उत्तर – पूर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था –
- लद्दाख के क्षेत्रों में जिंक द्वारा जल संरक्षण “किया जाता है। जिसमें बर्फ के ग्लेशियर को रखा जाता है जो दिन के समय पिघल कर जल की कमी को पूरा करता है।
- बाँस की नलियाँ— जल संरक्षण की यह प्रणाली मेघालय में सर्दियों पुरानी पद्धति है। जल को बाँस की नालियों द्वारा संरक्षित करके उन्हें पहाड़ों के निचले भागों में उन्हीं बाँस की नालियों के द्वारा लाया जाता है। इसमें
मैदानी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था –
- तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा जल को बड़े-बड़े टैंकों में संरक्षित किया जाता है तथा जरूरत के समय उपयोग करते हैं।
- बावरियाँ – ये मुख्यतः राजस्थान में पाये जाते हैं। ये छोटे-छोटे तालाब हैं जो प्राचीन काल में बंजारों द्वारा पीने के पानी की पूर्ति के लिए बनाये गये हैं।
पठारी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था:
- भंडार—ये मुख्यतः महाराष्ट्र में पाये जाते हैं जिसमें नदियों के किनारों पर ऊँची दीवारें बनाकर बड़ी मात्रा में जल को संरक्षित किया जाता है।
- जोहड़ ये पठारी क्षेत्रों की जमीन पर पाये जाने वाले प्राकृतिक छोटे खड्ढे होते हैं। जो वर्षा जल को संरक्षित करने में सहायक होते हैं।
2. अपने घर में पर्यानुकूलित वातावरण बनाने के लिए आप उसमें कौन-कौन-से परिवर्त्तन सुझा सकते हैं।
उत्तर – निम्लिखित परिवर्त्तन लाकर हम अपने घर में पर्यानुकूलित वातावरण बना सकते हैं –
- हब बिजली के पंखे या बल्ब के स्विच बन्द करके विद्युत का अपव्यय रोक सकते हैं।
- लीक करनेवाले जल के पाइप या नल की मरम्मत करवाकर हम जल की बचत कर सकते हैं।
- हमें तीन R’s बनाये हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए।
- हमें पुनःचक्रण योग्य वस्तुओं को कूड़े के साथ नहीं फेंकना चाहिए।
- हमें चीजों (जैसे लिफाफे) को फेंकने की अपेक्षा फिर से प्रयोग में लाना चाहिए।
- हमें आहार को व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
3. क्या आप अपने विद्यालय में कुछ परिवर्त्तन सुझा सकते हैं जिनसे इसे पर्यानुकूलित बनाया जा सके ?
उत्तर – निम्नलिखित परिवर्त्तनों द्वारा हम अपने विद्यालय में पर्यानुकूलित वातावरण बना सकते हैं-
- हमें विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधे लगाने चाहिए।
- बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि फूल तथा पत्तियों को न तोड़ें।
- हमें जल का अपव्यय रोकना चाहिए।
- कमरों में ज्यादा-से-ज्यादा खिड़कियाँ बनानी चाहिए ताकि सूर्य की रोशनी अन्दर आये और कम-से-कम बिजली खर्च हो ।
- हमें कूड़ा-कचरा इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि चीजों का पुनः उपयोग करना चाहिए।
4. ऊर्जा के संसाधनों में कोयला की खोज एक महत्त्वपूर्ण सम्पदा सिद्ध हुई, इस कथन की पुष्टि करें।
उत्तर – औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख कारक कोयले की खोज थी। कोयला एक उच्च ऊर्जा देने वाला ईंधन है। कोयले का उपयोग भट्ठी में किया जाने लगा। जिससे छोटे-बड़े कल-कारखाने लगने लगे। कोयला के खोज के पहले लोहा का निष्कर्षण तथा लोहे का गलाना बहुत कठिन था। कोयला को जलाकर पानी से भाप बनाया जाने लगा तथा भाप ऊर्जा का उपयोग इंजन चलाने के लिए किया जाने लगा। इस प्रकार ताप इंजन का आविष्कार कोयले की खोज एवं उसमें निहित ऊर्जा एवं उसके उपयोग के कारण ही हो सका। भाप इंजन के आविष्कार से बड़े-बड़े रेलों तथा पानी के जहाजों को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ जिससे पालों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह गई। भाप इंजन की सहायता से यातायात के साधन सुलभ एवं त्वरित हुए। यातायात के साधन एवं उद्योगों के साथ-साथ कोयला ईंधन का उपयोग घर में खाना बनाने के लिए भी किया जाने लगा। कोयले की खोज एवं उपयोगिता इतनी महत्त्वपूर्ण है कि इसे काला हीरा (Black Diamond) की संज्ञा दी गई। अतः ऊर्जा के संसाधनों में कोयले की खोज एक महत्त्वपूर्ण सम्पदा सिद्ध हुई— यह कथन बिल्कुल सत्य है ।
5. संपोषित प्रबंधन क्या है ? इसके लिए कौन-से उपाय किये जाने चाहिए ?
उत्तर – प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रबंधन जिससे उनका अस्तित्व सदा बना रहे, सम्पोषित प्रबंधन कहलाता है। आजकल स्थानीय जनता प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति काफी जागरूक हो चुकी है तथा यत्र तत्र जन आन्दोलन भी हो रहे हैं।
सन् 1972 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के आराबाड़ी वन क्षेत्र में वन अधिकारी ए. के. बनर्जी द्वारा समन्वित वन प्रबंधन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना की विशेषताएँ इस प्रकार हैं –
- वन विभाग एवं स्थानीय जनता के सहयोग से 1272 हेक्टेयर क्षेत्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया।
- इसमें स्थानीय जनता को वनों की देखभाल हेतु रोजगार दिया गया।
- ईंधन के लिए लकड़ी एवं पशुओं के लिए चारे का उपयोग करने की अनुमति दी गई ।
- वनोत्पाद के 2.5 प्रतिशत के उपयोग का अधिकार स्थानीय किसानों को दिया गया।
- वन प्रबंधन की इस तकनीक से तथा इस तकनीक में जनभागीदारी से सन् 1982 तक साल के वन पुनर्जीवित हो गये और उनके उत्पाद का मूल्य 12.5 करोड़ तक बढ़ गया।
6. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत क्या हैं ? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं बायो गैस ऊर्जा की विवेचना करें।
उत्तर – कोयला एवं पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा स्रोतों के सीमित होने के कारण हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता है। आज समूचे विश्व में ऊर्जा के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास और भी उपयोगी है क्योंकि हमारे यहाँ इन स्रोतों का विपुल भंडार मौजूद है। फिर कोयला एवं पेट्रोलियम की तुलना में अपारंपरिक ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है और नवीकरणीय है अर्थात् इनका बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण हैं— सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्री लहरों की ऊर्जा, बायो गैस, फोटोवोल्टिक ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि। इन स्रोतों से अभी व्यावसायिक स्तर पर ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में अनुसंधान कार्य पूरी गंभीरता से चल रहे हैं। आगे हम ऐसे ही कुछ अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की चर्चा करेंगे ।
सौर ऊर्जा— सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा और सुलभ भंडार है। हालाँकि सूर्य से उपलब्ध ऊर्जा या धूप की मात्रा मौसम तथा दिन-रात के हिसाब से घटती-बढ़ती है किन्तु हमारे देश में पर्याप्त धूप उपलब्ध होती है। इस ऊर्जा का हम अपने रोजमर्रा के कामों में भी भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दो प्रमुख तरीके हैं—
1. सौर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करके एवं 2. सौर वितरित ऊर्जा को फोटोवोल्टिक विधि से सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलकर ।
सौर ऊर्जा के विविध उपयोगों में मुख्य हैं – खाना पकाने के लिए सौर कुकर का इस्तेमाल और संग्राहक द्वारा पानी गर्म करना, सौर सेलों या फोटोवोल्टीय सेलों द्वारा सूरज की रोशनी की सीधे बिजली में परिवर्तित करना और हीटर के माध्यम से तापीय वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पानी के खारेपन को दूर करना आदि ।
सौर कुकर- सूर्य से पैदा गर्मी का उपयोग सौर कुकर की सहायता से सीधे भोजन पकाने के लिए किया जा सकता है। सौर कुकर धातु का एक बक्सा होता है जो अन्दर से काला होता है ताकि वह गर्मी सोख सके और उसे बनाये रख सके। ढक्कन एक परावर्ती सतह होता है जो सूरज की गर्मी की परावर्तित करके बक्से में भेजता है। बक्से में काले बर्तन होते हैं जिनमें पकाने के लिए खाद्य सामग्री रखी जाती है।
पवन ऊर्जाभारत में प्राचीन काल से ही पवन ऊर्जा का प्रयोग पवन चक्कियों के रूप में किया जा रहा है। प्राचीन काल में इसका उपयोग पाल-नौकाओं के संचालन में किया जाता था लेकिन आज इसका उपयोग कृषि और कई उद्योगों में हो रहा है। चूँकि पवन ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रणाली कम लागत पर अधिक लाभ देने वाली है, इसलिए भारत सरकार पवन ऊर्जा के क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे रही है। 2002 के आँकड़ों के अनुसार हमारे देश में 1870 मेगावाट बिजली का उत्पादन विद्युत पवन टरबाइनों से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के एक गाँव उछैया में 853 एकड़ भूमि की सिंचाई पवन चक्कियों से होती है। ये पवन चक्कियाँ कम एवं तेज हवा में भी सफलतापवूक कार्य करती हैं।
पवन ऊर्जा का उपयोग नाव चलाने में किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिए भी किया जाता है।
जैसे- 1. अनाज की पिसाई के लिए पवन चक्की।
2. जल पम्प चलाने के लिए पवन चक्की ।
3. विद्युत उत्पन्न करने के लिए पवन चक्की।
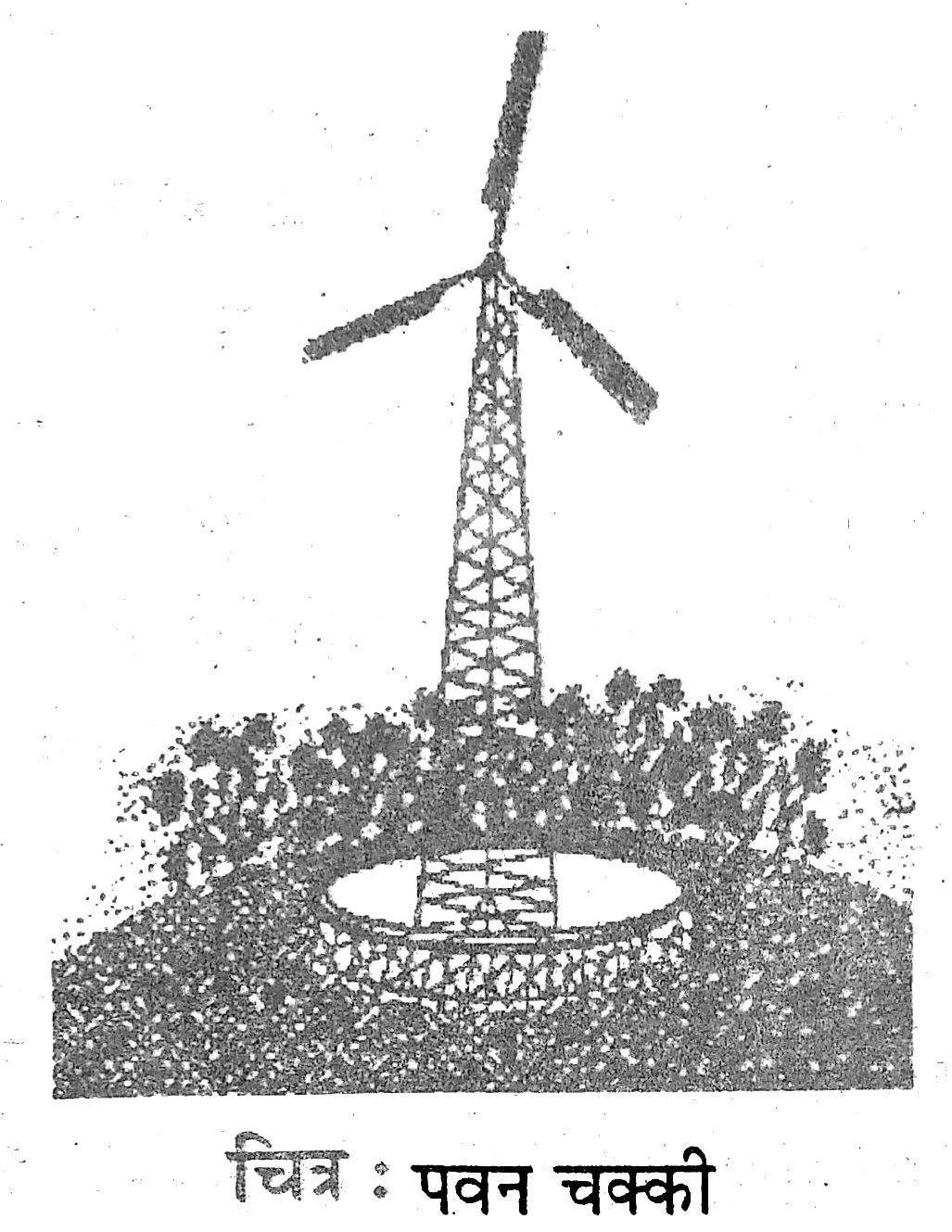
तमिलनाडु में बड़े-बड़े पवन संयंत्र लगे हैं जो 850 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। इस समय भारत संसार में पवन ऊर्जा का तीसरा बड़ा उत्पादक है।
बायो गैस (Bio-gas)–बायो गैस वनस्पतियों, पशुओं के मलमूत्र, अन्य व्यर्थ पदार्थ, घरेलू कूड़े-कचरे जैसे व्यर्थ पदार्थों से पैदा की जाती है। यह एक गैसीय मिश्रण है जिसमें मेथेन, कार्बन डाइ-ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा जलवाष्प मिली होती है। मेथेन ज्वलनशील गैस है जो आसानी से जलती है गैस के उपयोग होने के पश्चात् बचे पदार्थ खाद के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं। देहातों में बायो गैस संयंत्र काफी लोकप्रिय है। इस संयंत्र में गोबर डालकर गैस प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है।
बायो गैस एक स्वच्छ ज्वलनशील गैस है। वस्तुतः बायो गैस गैसों का मिश्रण है जिसमें लगभग 60 प्रतिशत मिथेन, 40 प्रतिशत कार्बन डाइ ऑक्साइड तथा बहुत अल्प मात्रा में अन्य गैसें होती हैं। यह विभिन्न जैव सामग्रियों, जैसे पशुओं के गोबर, मानवीय अपशिष्ट तथा बायोमास के अपघटन से प्राप्त होती है। इन जैव सामग्रियों का विघटन विशेष तकनीक पर विकसित किये गये बायो गैस संयंत्र में होता है। इस संयंत्र से न केवल उच्च कोटि का कार्बनिक उर्वरक प्राप्त होता है बल्कि स्वच्छ तथा धुआँरहित गैसीय ईंधन भी प्राप्त होता है।
7. पारिस्थितिकी अनुकूल कृषि से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर – वर्तमान समय में कृषि की नवीन विकास प्रक्रियाओं से हमारा पर्यावरण कई तरह से प्रभावित हुआ है। जैसे —
- रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक इस्तेमाल से प्रदूषण फैल रहा है।
- रासायनिक उर्वरक के ज्यादा इस्तेमाल से मृदा की लवणीयता बढ़ रही है जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है।
- रासायनिक पीड़कनाशी के अत्यधिक उपयोग से पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा हो रहा है।
- फसलों को नवीन बीमारियाँ हो रही हैं।
इन सभी कारणों से कृषि उत्पाद भी प्रभावित हो रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में अभी रासायनिक उर्वरक तथा पीड़कनाशी का उपयोग औसत से कम है, जिससे अभी तक कृषि पर इसके बुरे प्रभाव का असर नहीं है। फिर भी भविष्य में कृषि के इस स्वरूप से सचेष्ट रहने की आवश्यकता है। कृषि वैज्ञानिक अब कृषिकार्यों में कुछ संशोधन कर ऐसी कृषि प्रणाली के उपयोग की सलाह दे रहे हैं जिससे अधिक उत्पादकता के साथ-साथ पर्यावरण के प्रदूषित होने की संभावना कम-से-कम हो । ऐसी कृषि प्रणाली को पारिस्थितिकी – अनुकूल कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि प्रणाली में कार्बनिक एवं जैव उर्वरकों तथा पीड़क नियंत्रण के लिए एकीकृत पीड़क प्रबंधन (IPM) की सलाह दी गई है। इनके अतिरिक्त अच्छी पैदावार के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा समुन्नत किस्म के बीजों का विकास कर उनके उपयोग की भी सलाह दी गई है।
8. एकीकृत पीड़क प्रबंधन से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर – पीड़क कीटों के नियंत्रण के लिए कई विधियाँ अपनाई जाती हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित विधि रासायनिक पीड़कनाशी का उपयोग है। इसके अतिरिक्त कई अन्य विधियाँ, जैसे यांत्रिक, भौतिक तथा जैविक नियंत्रण आदि का भी उपयोग किया जाता है। इन सभी विधियों के अपने कुछ विशेष गुण एवं दोष होते हैं, जैसे रासायनिक पीड़कनाशी अत्यंत प्रभावशाली होता है। इसके परिणाम तुरंत दिखने लगते हैं। परंतु, रासायनिक पीड़कनाशी हानिकारक पीड़कों के साथ-साथ ऐसे लाभदायक जीवों का भी विनाश कर देते हैं, जो फसलों के लिए कई प्रकार से उपयोगी होते हैं। इस तरह, रासायनिक पीड़कनाशी के अधिक उपयोग से जैव असंतुलन पैदा होने का अंदेशा रहता है। रासायनिक पीड़कनाशी के अधिक उपयोग का दुष्परिणाम पर्यावरण पर भी होता है। इन्हीं कारणों से रासायनिक पीड़कनाशी के उपयोग में कमी लाकर एकीकृत पीड़क प्रबंधन को अपनाने की सलाह दी जाती है।
एकीकृत पीड़क प्रबंधन के अंतर्गत पीड़कों के नियंत्रण के लिए एक से अधिक नियंत्रण विधियों को उनके गुणों एवं अवगुणों के आधार पर सम्मिलित कर उनका उपयोग साथ-साथ किया जाता है। यह वास्तव में पीड़कों की नियंत्रण विधि नहीं है, बल्कि यह पीड़कों के प्रबंधन की विधि है। इसका उद्देश्य पीड़कों का पूर्ण नाश करना नहीं, बल्कि उनकी संख्या या घनत्व को इतना कम रखना है कि उसके कारण आर्थिक हानि न हो तथा पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। 1974 के प्रमुख बिंदुओं पर सके।
9. जल ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, विवरण दें।
उत्तर – यह विधेयक जनवरी 1974 में भारतीय संसद में पेश किया गया। संसद से पारित होने के बाद 23 मार्च, 1974 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गया। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन इसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है।
अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य –
- जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण तथा जंतु की स्वास्थ्यप्रदता बनाए रखना।
- इस उद्देश्य से केन्द्र एवं राज्यों में बोर्डों का गठन करना ।
- गठित बोडों के क्रियाकलापों को निर्धारित करना तथा उन्हें शक्ति प्रदान करना।
- अधिनियम के नियम का उल्लंघन करनेवालों के लिए दंड का प्रावधान करना।
इस अधिनियम के अनुसार, हर वैसे व्यक्ति (फैक्ट्री, संस्था या निकाय) को जो फैक्ट्री चलाता हो अथवा घरेलू कचरा बहाता हो, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य है। बोर्ड, जो इस अधिनियम के अंतर्गत एक कानूनी संस्था है, ऐसे व्यक्ति को तभी अनुमति या सहमति देगा जब ऐसा व्यक्ति घरेलू कचरे को या अपनी फैक्ट्री से निकलनेवाले बहिःस्राव को उपचारित करके बहाए !
इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए धारा 42-49 में सजा का प्रावधान है।
10. वर्मी कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं ? इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें।
उत्तर – नम मिट्टी में पाए जानेवाले साधारण केंचुआ की मदद से तैयार किया गया उर्वरक वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। केंचुआ मिट्टी में मिश्रित गोबर, सड़ी-गली खर-पतवार, पत्तियाँ, सड़े-गले फल तथा सब्जियाँ तथा उनके छिलके जैसे कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। फिर, इन पदार्थों के पोषक तत्त्वों को निगली मिट्टी के साथ गुदा के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकला यही काला, दानेदार मिट्टी जैसा पदार्थ वर्मी कंपोस्ट कहलाता है।
विशेषताएँ एवं लाभ —
- इसमें नाइट्रोजन स्थायीकर बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा में होते हैं।
- इसमें कार्बनिक पदार्थों के विघटन वाले एंजाइम भी होते हैं।
- अन्य जैविक उर्वरकों की अपेक्षा इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश तथा कार्बनिक अवयव की मात्रा अधिक होती है।
- इसके उपयोग से मृदा की रासायनिक गुणवत्ता में ह्रास नहीं होता है।
- इसके उपयोग से मृदा की नमी संचयन क्षमता बढ़ जाती है।
- इसके उपयोग से उत्पन्न उत्पादों के हानिकारक रासायनिक प्रभाव नहीं होते हैं ।
- इसके उत्पादन में रिहायशी घरों के आसपास बिखरी गंदगियों से स्वतः छुटकारा मिल जाता है तथा वातावरण स्वच्छ रहता है।
- इसे अत्यंत कम लागत से तैयार किया जा सकता है।
11. मानव तथा उसका पर्यावरण से सम्बन्ध का विवरण दीजिए। अथवा, पर्यावरण प्रदूषण के घटकों का वर्णन कीजिए ।
उत्तर – मानव तथा पर्यावरण का आपस में गहरा तथा अटूट सम्बन्ध है। मानव ही पर्यावरण को स्वच्छ या प्रदूषित करता है तथा उसका प्रभाव मानव को ही उसी रूप में प्रभावित करता है। समाज के लिए स्वच्छ तथा स्वास्थ्यवर्धक वातावरण बनाना मनुष्य पर ही निर्भर है।
मानव के क्रियाकलापों का अनियोजित होना पर्यावरण को अधिक हानि पहुँचाता है। महानगरों में ट्रकों तथा बसों से काला धुआँ, नदियों में नालों का गन्दा पानी तथा सड़कों पर बिखरा कूड़ा-करकट आदि महानगरों के पर्यावरण को दूषित करते हैं।
जनसंख्या में लगातार वृद्धि पर्यावरण को प्रदूषित करने का मुख्य घटक है अर्थात् पर्यावरण को प्रदूषित करने में मानव की प्रमुख भूमिका है। जनसंख्या बढ़ने से आवास, वस्त्र तथा खाद्य पदार्थों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है । इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक सम्पदाओं का क्षरण होता है। जैसे जंगलों का अत्यधिक काटा जाना, भूमिगत जल का अनियंत्रित उपयोग, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग, औद्योगीकरण आदि। ये सभी कारक किसी-न-किसी रूप में पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं।
जब प्राकृतिक साधन पर्यावरण को पुनः स्वच्छता प्रदान नहीं कर सकते तो प्रदूषण उत्पन्न होता है। औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा बिना नियोजित किए गए कारखानों आदि से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। अत्यधिक रसायनों का उपयोग भी इसी का एक घटक है । प्राकृतिक सम्पदाओं का अतिशोषण भी पर्यावरण के प्रदूषण को बढ़ावा देता है । औद्योगिक क्रान्ति से वायु तथा जल प्रदूषण होता है। अम्लीय वृष्टि, दहन इंजनों द्वारा प्रचलित वाहनों द्वारा अधिक मात्रा में सल्फर युक्त यौगिकों को मुक्त करने का परिणाम है। रसायन (ऐरोसॉल) के उपयोग द्वारा ओजोन सतह का अवक्षय हो रहा है।
मानव के विभिन्न क्रियाकलापों के परिणाम से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ आज पर्यावरण को प्रदूषित करने में सबसे आगे हैं। ये अपशिष्ट अत्यन्त घातक होते हैं तथा इनका प्रभाव दूर-दूर तक फैल जाता है। इनका निपटान आजकल विश्व स्तर की समस्या है। इनका पुनःचक्रण ही पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकता है।
अतः पर्यावरण को प्रदूषित करने में मुख्य भूमिका मनुष्य की है। साथ ही साथ प्रदूषित पर्यावरण का शिकार भी प्रमुख रूप से मानव ही है।
12. महानगरों में पर्यावरण स्तर के गिरने का कारण लिखिए।
उत्तर – महानगरों में पर्यावरण के स्तर के गिरने का निम्न कारण हो सकता (i) आवास की आवश्यकता पूरी करने हेतु अत्यधिक वृक्षों का काटा जाना, इस प्रकार पौधों के बिना पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहता। (ii) अत्यधिक औद्योगीकरण से चिमनियों द्वारा गन्दा धुआँ निकलना, अपशिष्ट पदार्थों का ठीक से निपटान न करना पर्यावरण स्तर को नीचे गिराते हैं। (iii) ट्रकों तथा बसों से निकलता काला धुआँ, नदियों का गन्दा पानी तथा सड़कों पर बिखरा कूड़ा-कटकर, अवशेष आदि से पर्यावरण निरन्तर दूषित हो रहा है।
ये सभी कार्यकलाप मिलजुलकर हमारे पर्यावरण के सभी घटकों; जैसे— वायु, जल तथा मृदा के साथ-साथ जीवित रहने के लिए आवश्यक जैव समुदाय को भी प्रदूषित करते हैं।
वृक्षों के काटने से जैव पदार्थों में समृद्ध मृदा की ऊपरी सतह वर्षा के पानी के साथ बहकर कूड़ा-करकट, अवशेष आदि से पर्यावरण निरन्तर दूषित हो रहा
लुप्त हो रही है। मृदा के इस प्रकार अपरदन के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है।
इन सब बातों को ध्यान में रखकर तथा वनों की उपयोगिता को देखते हुए वनों का परिपूर्ण होना अतिआवश्यक है। इन सबके अतिरिक्त पौधे जितने अधिक उगाए जाएँगे हमारा पर्यावरण उतना ही स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्धक होगा, क्योंकि पौधे ही हमारे प्रदूषित पर्यावरण को स्वच्छ कर सकते हैं।
13. जल एवं ध्वनि प्रदूषण के कारण एवं उनके प्रभावों को लिखें।
उत्तर – यदि नदी के समीप फैक्ट्री लगाई जाये तो रसायन तथा अन्य अपशिष्टों को नदी में निष्कासित होने से जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होने लगेगी। इसके अतिरिक्त लोग इसमें नहाते और कपड़े धोते हैं। इसका परिणाम यह है कि पानी गन्दा हो जाता है। सूक्ष्म जीवों, काई तथा अन्य किसी प्राकृतिक कारक द्वारा इसका शोषण नहीं किया जा सकता है। हानिकारक रसायन पानी में घुलकर अन्त में हमारे आहार – शृंखला में पहुँच जाते हैं।
शहरी जनसंख्या के पास आधुनिक घरेलू सामान उदाहरण के लिए मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, वाशिंग मशीन, कूलर तथा कंडीशनर आदि हैं। ये ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि करते हैं जिससे में स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। लाउडस्पीकर तथा धार्मिक स्थानों में हो रहे प्रवचन न तो केवल विद्यार्थियों और रोगियों को परेशान करते हैं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। धार्मिक स्थानों से ढोलक की आवाज, विवाह के जुलूस या नारों की आवाज, रेडियो की ऊँची आवाज, ट्रांजिस्टर, स्टीरियो, टेलीविजन, डिस्को, वी.सी.आर., एम्लीफायर आदि ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक समस्या है। इसके अतिरिक्त, जनसंख्या में वृद्धि मनुष्य के भौतिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है। शोर से अस्थायी तौर पर श्रवण शक्ति कम हो जाती है, दिल की धड़कन में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह जनसंख्या की वृद्धि से उनके पास वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हो गई है जिससे साधारण मनुष्य के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है।
14. जनसंख्या और प्रदूषण में क्या सम्बन्ध है ? स्पष्ट करें।
उत्तर – जनसंख्या बढ़ने से प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि प्रातः काल उठने के साथ ही मनुष्य प्रदूषण प्रारंभ कर देता है। प्राकृतिक स्रोत का दुरुपयोग मनुष्य आरंभ कर देता है। प्रकृति भी एक सीमा तक ही प्रदूषण को रोक पाने में सक्षम है। यदि कोई बस्ती ऊँची जगह पर है, तो वहाँ का गंदा पानी नीचेवाली बस्ती की ओर आकर जल प्रदूषण उत्पन्न करती है। फैक्टरी द्वारा उत्पन्न रसायन भी जल और वायुमंडलीय पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। मनुष्य के क्रिया-कलापों ने गंगा जल को भी प्रदूषित कर दिया है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे-जैसे आबादी बढ़ेगी प्रदूषण में वृद्धि होगी। ज्यादा जनसंख्या के लिए ज्यादा चीजों की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया जाता है। फलस्वरूप कल-कारखानों से प्रदूषित गैसें और मलवा ज्यादा मात्रा में निकलता है। इस प्रकार वातावरण ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही जंगलों एवं खेती योग्य भूमि पर कंक्रीट के जंगल लगाए जाने लगे। इमारती लकड़ी, कागज एवं अन्य सामानों की पूर्ति के लिए हरित प्रदेशों का ह्रास होता जा रहा है। पौधों की कमी से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होना लाजिमी है। प्रदूषण की समस्या प्राणियों के लिए हानिकारक है। अतः प्रदूषण की समस्या का समुचित समाधान होना चाहिए ।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here