बिहार-निर्माता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
बिहार-निर्माता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
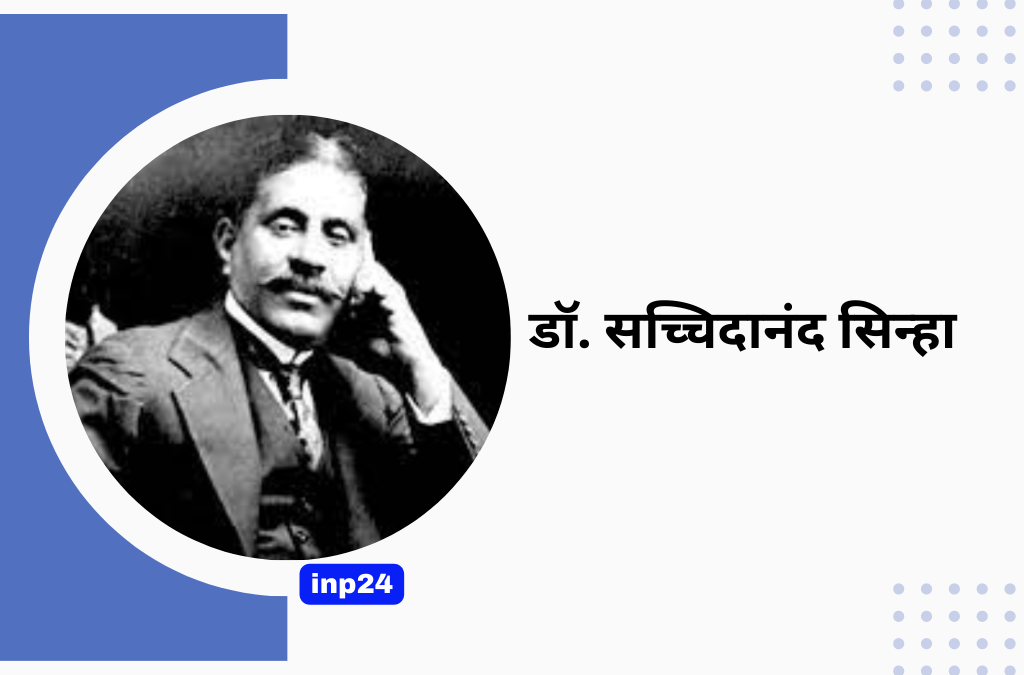
डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा की गणना आधुनिक बिहार के महापुरुषों में की जाती है। वह एक बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न व्यक्ति थे, जिन्हें एक महान् विधिवेत्ता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में आदर के साथ आज भी याद किया जाता है। इतिहासकार उन्हें ‘बिहार के बंगाल पृथक्करण आंदोलन’ की मुख्य धुरी मानते हैं। यह उन्हीं के अथक प्रयासों का नतीजा था कि 1 अप्रैल, 1912 को बंगाल प्रांत से अलग बिहार एवं उड़ीसा का एक नए प्रांत के रूप में गठन संभव हो पाया।
सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर, 1871 को आरा में हुआ था। उनके दादा बक्शी शिवप्रसाद सिन्हा मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में डुमराँव महाराज के यहाँ कार्य करते थे। शायद यही कारण था कि उनके पूर्वज लखनऊ से आकर डुमराँव के नजदीक मुरार गाँव में बस गए थे। उनके पिता रामयाद सिन्हा उत्तर-पश्चिमी प्रांत में कार्यपालक अधिकारी थे। परंतु सरकारी नौकरी उन्हें रास नहीं आई, बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर बनारस में वकालत शुरू की। शीघ्र ही उनका वकालत के पेशे में अच्छा नाम हो गया। कालांतर में तत्कालीन डुमराँव महाराज के सुझाव पर उन्होंने सन् 1865 में बनारस छोड़कर आरा में वकालत शुरू की और डुमराँव महाराज ने उन्हें अपना स्थायी अधिवक्ता नियुक्त कर लिया। आरा में ही उनकी मित्रता हरवंस सहाय से हुई।
सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मकतब में शुरू की, जहाँ उन्हें हिंदी एवं उर्दू का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। सन् 1877 में आरा के जिला स्कूल में प्रवेश लिया और अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषाओं का भी अध्ययन किया । यहीं पर उनकी दोस्ती अली इमाम एवं हसन इमाम के साथ हुई, जो जीवनपर्यंत बनी रही। उनकी इस मित्रता का ही परिणाम था, सन् 1887 में अली इमाम जब बैरिस्टरी की पढ़ाई करने इंग्लैंड जा रहे थे तो उनके मन में भी इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी की पढ़ाई करने का विचार आया। परंतु तत्कालीन परिवेश में वित्तीय कठिनाई के अलावा सामाजिक रूढ़ियाँ भी उनके इस विचार के कार्यान्वयन में बाधक थीं। उस समय किसी भी हिंदू के लिए समुद्र पार कर विदेश जाना अपनी जाति व धर्म से बहिष्कृत होना था। इसके अलावा अपने माँ-बाप के इकलौते पुत्र होने के चलते भी उन्हें घर से इजाजत मिलना कठिन था। कुछ समय के लिए उन्होंने पटना के टी.के. घोष एकेडमी तथा पटना कॉलेज में भी प्रवेश लिया, परंतु पिता के अनुरोध को देखते हुए वे कलकत्ता चले गए, जहाँ सिटी कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगा तथा सन् 1889 में अपना सबकुछ बेचकर और पिता के एक मित्र से 200 रुपए की मदद लेकर इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया।
लंदन में बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के साथ-साथ पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी सक्रियता दिखाई। यह उनकी योग्यता का ही परिणाम था कि जल्द ही वे ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। यहाँ पर उन्हें डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आर.एन. मधोलकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जॉर्ज यूल, चार्ल्स ब्रेडला, विलियम डिग्बी जैसे महान् नेताओं का सान्निध्य प्राप्त हुआ। इससे उनके मन में भी सक्रिय राजनीति में कार्य करने की महत्त्वाकांक्षा जाग्रत् हुई। जब सन् 1892 में दादाभाई नौरोजी इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो सच्चिदानंद सिन्हा ने उनके पक्ष में जमकर प्रचार कार्य किया ।
सच्चिदानंद सिन्हा के लंदन प्रवास ने बिहार की पहचान व संकट को भी समझने में मदद की। उनके मन में बिहार को बंगाल से अलग पहचान बनाने की बात बार-बार कचोटती थी। जब भी वहाँ के अंग्रेजों या भारतीय लोगों को परिचय देते हुए वह कहते कि वह बिहार के निवासी हैं तो लोग तुरंत उनसे पूछते कि कौन से बिहार का ? इसका कारण था कि तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मानचित्र में बिहार का अलग से एक प्रांत के रूप में अस्तित्व नहीं था। वह बंगाल प्रांत का हिस्सा था। 1893 में जब वह जहाज से वापस भारत आ रहे थे, तब भी उनके बिहारी होने की पहचान पर प्रश्न-चिह्न उभरकर सामने आया। बिहार में भी उन्हें अपने बिहारी भाइयों को ‘बंगाल सरकार के कर्मचारी’ के रूप में देखने पर भारी अफसोस हुआ। वह लिखते हैं- जब बिहार के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर उनकी गाड़ी पहुँची तो उन्होंने एक बिहारी सिपाही के कंधे पर बंगाल पुलिस का बैच लगा देखा। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया कि वह बिहार को बंगाल से अलग एक प्रांत का दर्जा दिलवाकर रहेंगे। पटना वापस लौटकर अपने मन की बात उन्होंने पत्रकार महेश नारायण से कही।
महेश नारायण ‘कायस्थ गजट’ के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार थे । वह भी पृथक् बिहार प्रांत के विचार के पोषक थे। इन लोगों के साथ नंदकिशोर लाल, कृष्ण सहाय, मजहरुल हक, इमाम बंधु भी आ मिले। इन सभी के एक साथ होने से बंगाल से बिहार के पृथक्करण आंदोलन को एक गति मिली। अपने विचारों को जन-जन तक पहुँचाने एवं सरकार को अपनी माँगों के न्यायोचित होने की जानकारी देने हेतु सन् 1894 के जनवरी माह से ‘बिहार टाइम्स’ का प्रकाशन शुरू किया। यह पत्र इस आंदोलन के प्रमुख मुखपत्र के रूप में उभरकर सामने आया। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने बिहार की बदहाली एवं बिहार के बंगाल से जुड़े रहने के दुष्परिणामों को सबके सामने रखा तथा बिहार के लोगों से आह्वान किया कि वे इस दलदल से मुक्त हों। ‘बिहार टाइम्स’ में प्रकाशित लेखों एवं आँकड़ों के द्वारा पृथक् बिहार की माँग को यथार्थ के धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा का मानना था कि बिहार बंगाल प्रांत का उपांग बनकर रह गया है। बंगालियों ने बिहार को अपना चारागाह बना लिया है। आधुनिक शिक्षा का बिहार में प्रसार नहीं होने दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों एवं अदालतों पर भी बंगालियों ने अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। उनके इस प्रयास को ठोस रूप प्रदान करने हेतु सन् 1894 में डिप्टी गवर्नर सर चार्ल्स इलियट को अलग बिहार के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इसी के कुछ समय पश्चात् जब अलेक्जेंडर मेकेंजी डिप्टी गवर्नर बनकर गया आए तो उन्हें भी इसी तरह का ज्ञापन सौंपा गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया।
सन् 1905 के बंगाल विभाजन से बिहार के पृथक्करण आंदोलन को एक नई दिशा मिली। इस विभाजन के स्वरूप का सच्चिदानंद सिन्हा सहित बिहार के राष्ट्रवादियों ने जमकर विरोध किया। सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने अखबारों में वैकल्पिक विभाजन की रूपरेखा देते हुए लेख लिखे । ‘हिंदुस्तान रिव्यू’ (Hindustan Review) में लिखे दो लेखों को आधार बनाकर उन्होंने एक पुस्तिका का प्रकाशन किया, जो सन् 1906 में ‘पार्टीशन ऑफ बंगाल’ और ‘सेपरेशन ऑफ बिहार’ शीर्षक से प्रकाशित हुई। परंतु बात नहीं बनी।
सन् 1906 में ही ‘बिहार टाइम्स’ का नाम बदलकर ‘बिहारी’ रखा गया। 1907 में महेश नारायण के निधन के पश्चात् ब्रह्मदेव नारायण ने सच्चिदानंद सिन्हा को इस प्रयास में अपना सक्रिय सहयोग दिया। वह पंडित मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू एवं मदनमोहन मालवीय जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के संपर्क में आए और उनसे पृथक् बिहार प्रांत के निर्माण का नैतिक समर्थन प्राप्त किया। 1908 में ही सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक, हसन इमाम, दीपनारायण सिंह जैसे नेताओं के सहयोग से ‘बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी’ का गठन किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा इसके कोषाध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1909 में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन (Bihar Provincial Conference) का दूसरा सम्मेलन उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने पृथक् बिहार के गठन पर जोर देते हुए कहा कि इस आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों की समान रूप से सक्रिय भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक स्वरूप प्रदान करेगी। बिहार में हिंदू एवं मुसलमानों के इस सौहार्द पर तत्कालीन समाचार-पत्रों (बंगाली, इंडियन मिरर इत्यादि) ने प्रशंसापूर्ण टिप्पणियाँ लिखीं।
सन् 1910 में वे बंगाल से केंद्रीय विधायिका सभा के लिए चुने गए। इस अवसर का उपयोग उन्होंने बिहार के लोगों की समस्याओं को केंद्रीय स्तर पर उठाने के लिए किया। जब लॉर्ड एस.पी. सिन्हा ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् के विधि सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया, तब उन्होंने गवर्नर जनरल से शिमला में मुलाकात के दरम्यान अली इमाम को इस पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की। यद्यपि प्रारंभ में अली इमाम ने इसके लिए किसी उत्सुकता का प्रदर्शन नहीं किया। परंतु जब श्री सिन्हा ने समझाया कि इससे पृथक् बिहार के गठन को सरकारी समर्थन हासिल करने में मदद मिलेगी तो वे विधि सदस्य बनने को तैयार हो गए। हालाँकि अली इमाम ने उनके इस उत्साही कदम को व्यंग्यात्मक स्वर में उन्हें ‘हठी स्वप्नदर्शी’ कहकर टालना चाहा। परंतु वास्तव में श्री सिन्हा की सोच सही साबित हुई। अली इमाम ने कार्यकारी परिषद् का विधि सदस्य बनकर गवर्नर जनरल के सान्निध्य का लाभ उठाते हुए उनसे बिहार प्रांत के गठन का आग्रह किया। आखिरकार 12 दिसंबर, 1911 को दिल्ली दरबार में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा पृथक् प्रांत के रूप में बिहार एवं उड़ीसा के गठन की घोषणा की गई। 22 मार्च, 1912 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई और 1 अप्रैल, 1912 को इस नए प्रांत का विधिवत् उद्घाटन हुआ। यह श्री सिन्हा के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण क्षण था ।
सन् 1912 में पृथक् बिहार प्रांत के गठन मात्र से सच्चिदानंद सिन्हा संतुष्ट नहीं थे। उन्हीं के मिले-जुले अथक प्रयासों से 1916 में पटना उच्च न्यायालय एवं 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पृथक् बिहार प्रांत के गठन के अलावा सच्चिदानंद सिन्हा ने तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब तक बिहार के सामाजिक परिदृश्य में बदलाव नहीं होगा, बिहार आधुनिकता के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। उनका पहला विद्रोह समुद्र पार कर विलायत जाकर पढ़ाई करने में ही दिखाई देता है। जब वह इंग्लैंड से वापस लौटे तो उनकी जाति के लोगों ने उन्हें प्रायश्चित्त करने को कहा। इसके तहत उनसे सामाजिक भोज आयोजित करने को कहा गया, जिसमें समाज के लोग उन्हें फिर से अपनी जाति में शामिल कर लेंगे। परंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर किसी भी प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार ने अपनी बेटी की शादी उनसे नहीं की। पर वह झुके नहीं और लाहौर में जाति से हटकर अपनी शादी की। उनकी पत्नी का नाम राधिका देवी था।
श्री सिन्हा का मानना था कि सामाजिक रूढ़ियों से लड़ने हेतु लोगों में बदलाव के प्रति जागरूकता पैदा करना जरूरी है। अत: अपने आदर्शों को ठोस आधार प्रदान करने हेतु समाचार-पत्र का सहारा लिया। 1899 में उन्होंने ‘कायस्थ समाचार’ और ‘हिंदुस्तान रिव्यू’ का प्रकाशन एवं संपादन प्रारंभ किया। इसके माध्यम से उन्होंने अपने प्रगतिशील विचारों को जनता तक पहुँचाना शुरू किया। जुलाई 1900 में उन्हें कायस्थ पाठशाला का सचिव भी बनाया गया। 1929 में अखिल भारतीय कायस्थ कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में अध्यक्षता करते हुए लोगों से सामाजिक रूढ़ियों से ऊपर उठकर कार्य करने का आग्रह किया।
बिहार के अलग प्रांत के रूप में गठन के पश्चात् 1912 में ही जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पटना के बाँकीपुर मैदान में आयोजित किया गया तो सच्चिदानंद सिन्हा को इसकी स्वागत समिति का सचिव मनोनीत किया गया। 1913 में उन्होंने बिहार के क्षेत्रीय परिवेश से बाहर निकलकर आगरा एवं अवध प्रॉविंशियल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। 1914 में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में यूरोपीय देशों का दौरा किया। 30 जुलाई, 1919 को उनकी पत्नी राधिका सिन्हा की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की स्मृति में 1924 में उन्होंने श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना की और बिहार में शैक्षिक प्रसार पर विशेष ध्यान दिया।
सन् 1919 में ही वह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए निर्वाचित हुए। इंडियन लेजिस्लेटिव एसेंबली के पहले डिप्टी प्रेसीडेंट के पद पर वह 1921 में भी चुने गए। जब बिहार एवं उड़ीसा प्रांत में द्वैध शासन अधिनियम लागू हो गया तो 1921 में ही वह गवर्नर के कार्यकारी परिषद् के सदस्य नियुक्त किए गए। यद्यपि नवंबर 1922 में उन्हें इस पद से मुक्त कर दिया गया।
एक कार्यकारी पार्षद के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा ने वित्त एवं जेल प्रशासन की जिम्मेदारी को कुशलता से सँभाला। राजनीतिक बंदियों के साथ व्यवहार को लेकर उनके सरकार के साथ मतभेद भी उभरे । राजनीतिक बंदियों की कमर में रस्सी बाँधने एवं उन्हें हथकड़ी पहनाने का विरोध किया।
सन् 1927 में अपने यूरोप प्रवास के दौरान जेनेवा में आयोजित इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उसी वर्ष लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को द्वैध शासन के कार्यपक्ष पर संबोधित किया। 1930 में उन्हें उड़ीसा बाउंडरी कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया। 1936 में उनको पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर-सरकारी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया, जिस पर वह 1944 तक कार्यरत रहे। 1937 में उन्हें पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्र से बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुना गया। इसी वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट्. की मानद उपाधि प्रदान की। 1946 में वह पुनः बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। 1946 में ही उन्हें भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के तौर पर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर उन्होंने सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। 14 फरवरी, 1950 को जब वह पटना में अस्वस्थ थे तो भारतीय संविधान को उनके हस्ताक्षर हेतु विशेष तौर पर पटना लाया गया, जहाँ उन्होंने हस्ताक्षर किया।6 मार्च, 1950 को बिहार के इस महान् सपूत का निधन हो गया। आधुनिक बिहार के गठन से लेकर उसके चौतरफा विकास तक उनके द्वारा किए कार्य हमेशा अनुकरणीय रहेंगे। अपने आदर्शों एवं मूल्यों से समझौता न करने की उनकी आदत ने हमेशा उन्हें भीड़ से अलग रखा।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here