चार्टिज्म | Chartism
चार्टिज्म | Chartism
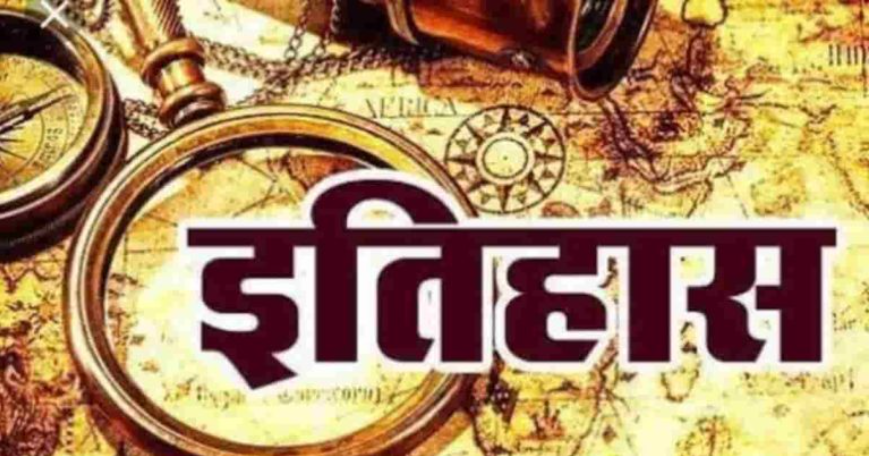
चार्टिज्म का अर्थ- मिस वाटसर्न ने चार्टिज्म की परिभाषा इस प्रकार दी है- “चार्टिज्म की उत्पत्ति का प्रमुख कारण था – प्राचीन सुधार आंदोलन, ओवन, टाम्पसन, हाज्सकिन एवं मनुष्यों का समाजवादी प्रचार और व्यापारिक संघ आंदोलन। “
चार्टिज्म का उदय एवं विकास का कारण
चार्टिज्म के उदभव का सामाजिक कारण- 19वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त था क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिये थे। वे उत्पादकों व्यवसायियों और व्यापारियों के रूप में कार्य करने के कारण धनी हो गये। दूसरी तरफ निम्न वर्ग के जिन व्यक्तियों से वे श्रमिकों का काम लेते थे, उनकी स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक बिगड़ गयी। अतः मध्य और निम्न वर्गों में भारी अंतर आ गया था और यह अंतर दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था । औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड के मध्यम और निम्न वर्गों का वास्तविक अर्थ में एक समुदाय था। वे निकट सम्पर्क में रहते थे। उनके पारस्परिक सम्बन्ध तनावपूर्ण थे।
औद्योगिक क्रांति ने दोनों वर्गों को एक-दूसरे से पृथक कर दिया। मध्यम और निम्न वर्गों के व्यक्ति दो स्पष्ट समूहों में बँट गये। इन समूहों को राष्ट्रों की संज्ञा देते हुए डिजराइलों ने 1845 में लिखा, दोनों वर्ग दो राष्ट्र हैं, जिनमें किसी प्रकार का सम्पर्क या सहानुभूति नहीं है और जो एक-दूसरे की आदतों, विचारों और भावनाओं से इतने अनजान हैं, मानों वे विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न देशों के निवासी हों ।
मजदूर वर्ग के कष्ट- इंग्लैंड में औद्योगिक और कृषि क्रांति ने देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी थीं। नवीन मशीनों के प्रचलन ने हाथों से कार्य करने वाले श्रमिकों की अधिकता के कारण उनकी पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गयी। उनका पारिश्रमिक पहले से कम हो गया। बैंथम के अनुयायियों ने श्रमिक वर्ग की इस पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता में सरकार की ओर से किसी भी हस्तक्षेप का विरोध किया। ‘अन्न अधिनियम’ ने अन्न के भावों में वृद्धि कर दी, जिससे एक ओर बड़े-बड़े जमींदार वर्ग पहले की तुलना में ज्यादा धनी तथा दरिद्र वर्ग पहले की तुलना अधिक दरिद्र हो गये। 1834 में ‘दरिद्र अधिनियम’ में संशोधन ने गरीबों की मुश्किलों और कष्टों में और अधि क बढ़ोतरी कर दी। उसका कारण यह था कि इस कानून के अंतर्गत राज्य की ओर से दरिद्रों को दी जाने वाली निःशुल्क मदद बन्द कर दी गयी ।
1832 के सुधार ऐक्ट के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग में असन्तोष- जनसाध कारण को उम्मीद थी कि सन् 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम देश के तत्कालीन सभी दोषों का निदान करेगा, परन्तु जनता की यह उम्मीद निर्मूल साबित हुई, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत केवल मध्यम वर्ग को ही मताधिकार मिला। श्रमिक वर्ग मताधिकार से वंचित रह गया। श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी थी। संसदीय सुधारों के लिए श्रमिक वर्ग ने मध्य वर्गीय लोगों के समान प्रयत्न किया था। श्रमिक जेलों में भी गये थे। उन्होंने अनेक कठिनाइयां भी सहीं। परन्तु जब
1832 में यह कानून पास हुआ तो उसके अन्तर्गत मध्यम वर्ग को मताधिकार मिला, परन्तु श्रमिक वर्ग उपेक्षित ही रहा। अतः उन्हें गहरा धक्का लगा। तत्कालीन सरकार ने भी इस वर्ग से उपेक्षित बर्ताव किया। सन् 1887 में लार्ड जान रसल ने घोषित किया कि 1832 का सुधार ऐक्ट सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाया गया अंतिम कदम था। इसके उपरान्त संसद में किसी अन्य सुधार अधिनियम के पास होने की उम्मीद न रही और न ही श्रमिक वर्ग की स्थिति में सुधार की कोई उम्मीद रही।
अतः चार्टिस्ट आंदोलन के अनुयायियों ने यह निश्चय किया कि उनकी कठिनाइयों और विपत्तियों का अंत सभी लोगों को मताधिकार मिल जाने से हो सकेगा। इस रास्ते से ही जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने की उम्मीद थी। असन्तुष्ट वर्ग ने लावेट तथा फीअरगस ओकोनल के नेतृत्व में एक संस्था बनायी। उसके द्वारा अपना एक कार्यक्रम बनाया गया, जिसके अनुसार उन्होंने जनता की मांगों का चार्टर तैयार किया। इन लोगों ने ‘नॉर्दन स्टार’ नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित करना शुरू किया।
चार्टिज्म के उदभव का राजनैतिक कारण- श्रमिक वर्गों को आर्थिक और सामाजिक स्थिति के साथ-साथ अपनी राजनैतिक स्थिति से भी असन्तोष था। यद्यपि 1832 का ‘सुधार अधिनियम’ उन्हीं के प्रयासों के कारण बना, पर उससे मध्यम वर्ग लाभान्वित हुआ था। निर्धन श्रमिकों को कोई फायदा नहीं हुआ था। उनको मतदान का अधिकार नहीं मिला, इससे उनमें अत्यधिक असन्तोष था। ट्रेवेलियन का कहना है, “श्रमिक वर्गों की राजनैतिक असमर्थता ने उनको इस बात की याद दिलाई कि दूसरे सुधार बिल की जरूरत थी।”
चार्टिज्म के उदभव का आर्थिक कारण- औद्योगिक क्रांति के कारण निम्न तथा श्रमिक वर्गों की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई थी, नवीन खोजों के कारण उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हो गई थी। देश में सम्पन्नता थी तथापि मजदूरों और कारीगरों की शिकायतें थीं कि उनकी स्थिति पूर्व की अपेक्षा अधिक खराब थी, उनको काम मिलने में कठिनाई थी, उनकी मजदूरी कम थी और उनके पास प्रतिदिन महंगे होने वाले अन्न को खरीदने के लिए धन की कमी थी। इसके अलावा उनकी शिकायत थी कि धन और उत्पादन की वृद्धि उन्हीं के परिश्रम के कारण हो रही थी, पर उन्हें भरपेट भोजन भी प्राप्त न हो पाता था।
चार्टिज्म के उदभव का अन्य कारण चार्टिस्ट आंदोलन के अन्य कारण निम्नलिखित थे—
(i) 1834 का ‘दरिद्र नियम’ (Poor Law), जिसके अनुसार श्रमिकों को सरकार से आर्थिक मदद बन्द हो गयी थी ।
(ii) देश के ‘अनाज-नियम’ जिनसे जमींदारों ने फायदा उठाकर अनाज का मूल्य अधिक कर दिया था।
(iii) उत्तर के औद्योगिक नगरों में शुरू होने वाला आंदोलन, जिसके द्वारा मजदूर कारखानों में केवल 10 घण्टे कार्य करने की मांग कर रहे थे।
लोक प्रपत्र चार्टिस्टों की मांग सूची
8 मई 1838 को ‘लंदन श्रमिक संघ’ (London Workingmen’s Association) ने अपनी मांगों की एक सूची तैयार कर ‘लोक-प्रपत्र’ में अंकित की। ये निम्नलिखित थे—
(i) संसद के सदस्यों को वेतन मिले।
(ii) गुप्त मतदान की प्रथा हो ।
(iii) समान निर्वाचन क्षेत्र हो ।
(iv) संसद की सदस्यता के लिए सम्पत्ति की योग्यता का अंत हो ।
(v) संसद का वार्षिक निर्वाचन हो ।
(vi) सभी वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को मताधिकार मिले। चार्टिस्टों ने इस ‘लोक प्रपत्र’ को तीन विभिन्न ‘आवेदन पत्रों’ के साथ 1839, 1842 और 1848 में संसद के सामने पेश किया। तीनों मौकों पर उनके ‘आवेदन पत्र’ अस्वीकार कर दिये गये।
चार्टिज्म के उद्देश्य
चार्टिज्म के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित थे—
ग्रेडनर (Gardner) के अनुसार- “चार्टिज्म का उद्देश्य यह था कि श्रमिक वर्गों को राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो जाए। जिससे वे अपनी दशा में सुधार कर सकें।”
रेम्जेम्योर (Ramsey Muir) के अनुसार “चार्टिज्म का उद्देश्य सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था की पूर्ण रूप से पुनसंरचना करना था। “
वुडवर्ड (Woodward) के अनुसार-“लोक प्रपत्र” के समर्थकों के दो समूहों के दो उद्देश्य थे- इंग्लैंड में ‘राजनैतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना तथा राजनैतिक शक्ति प्राप्त करके समाज की नवीन आर्थिक व्यवस्था करना । “
ट्रेवलियन (Travelyan) के अनुसार “चार्टिज्म का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक था । ” “
कुछ अन्य विचारकों के अनुसार, “आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दशाओं में आमूल-चूल परिवर्तन और समाज की पुनसंरचना करना । “
प्रथम आवेदन पत्र – 12 लाख 50 हजार व्यक्तियों द्वारा दस्तखत किया हुआ ‘प्रथम आवेदन पत्र’ बरमिंघम के एटवुड (Attwood) ने जुलाई 1839 में संसद के सामने पेश किया।
संसद ने उसे स्वीकार कर दिया। इससे चार्टिस्टों ने अपने को असहाय स्थिति में पाया। यद्यति उत्तर में विद्रोह नहीं हुआ, पर दक्षिणी वेल्स (South Wares) में विद्रोह भड़क उठा। लगभग 3 हजार सशस्त्र चार्टिस्टों ने न्यूपोर्ट (Newport) पर हमला कर दिया। उनका लक्ष्य अपने नेता विंसेंट (Vincent) को जेल से छुड़ाना था, पर सेना के आने पर वे भाग खड़े हुए।
आन्दोलन का अन्त – सरकार ने विद्रोहहियों को बुरी तरह कुचला। चार्टिस्टों की भीड़ को सेना द्वारा तितर-बितर कर दिया गया। कुछ प्रमुख चार्टिस्टों को गिरफ्तार कर कारावास या काले पानी का दण्ड दिया गया। लावेट और ओकानल को एक वर्ष के लिए बन्दी बनाया गया। बचे हुए विद्रोहियों में निराशा फैल गई। उन्होंने स्वयं को सरकार से लोहा लेने में अक्षम पाया। अतः उन्होंने स्वयं को पुनःसंगठित करने का कोई विचार नहीं किया। अगस्त, 1839 के अन्त तक चार्टिस्टों और उनके सम्मेलन का कोई चिह्न न रहा।
आन्दोलन का पुनः प्रारम्भ- यद्यपि चार्टिस्ट आन्दोलन की समाप्ति हो गयी थी, तथापि श्रमिक वर्ग अब भी इस भावना से प्रेरणा प्राप्त कर रहा था। उसने 1840 ई. में ‘राष्ट्रीय चार्टिस्ट संघ’ स्थापित किया। एक वर्ष उपरान्त लॉवेट और ओ-कॉनल ने कारावास से मुक्त होकर इस भावना को प्रबल बनाने का निश्चय किया। उन्होंने चार्टिस्टों को पुन: संगठित करने का कार्य शुरू किया। पर पिछले अनुभवों के आधार पर निश्चय किया। इस प्रकार चार्टिस्ज्म पुनर्जीवित हुआ, यद्यपि उसका स्वरूप भिन्न था।
द्वितीय आवेदन पत्र – सन् 1842 का वर्ष श्रमिकों के लिए अति संकट का वर्ष था। अतः चार्टिस्ट-आन्दोलन ने शीघ्र ही व्यापक रूप धारण कर लिया। अपनी 6 मांगों को लिखकर उन्होंने दूसरा आन्दोलन – पत्र तैयार किया। इसका स्वरूप राजनैतिक न होकर सामाजिक था। इस पर 30 लाख व्यक्तियों ने दस्तखत किये। आवेदन-पत्र संसद के सामने पेश किया गया। पहले की ही तरह संसद ने पुनः इसे अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर दंगे हुए। चार्टिस्टों ने राष्ट्रीय हड़ताल घोषित की। यार्कशायर तथा लंका शायर में पूर्ण हड़ताल रही । आन्दोलन में किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया। पर सरकार ने दमन-नीति का अनुसरण करके भारी संख्या में चार्टिस्टों को जेल भेज दिया और कुछ को देश से निष्कासित कर दिया। 1842 में चार्टिस्ट आन्दोलन प्रायः खत्म हो गया।
अन्तिम प्रयास- 1842 की घटना के उपरांत यह धारणा बन गयी कि चार्टिस्ट आन्दोलन का हमेशा-हमेशा के लिए अन्त हो गया था। 1848 ई. में फ्रांस में होने वाली क्रान्तिकारियों की सफलता से प्रेरित होकर चार्टिस्टों ने एक बार फिर स्वयं को संगठित किया। विशाल सभाएँ और विशाल प्रदर्शन आयोजित किये गये। ‘राष्ट्रीय सम्मेलन’ के सदस्य पुनः चुने गये। उन्होंने ‘तीसरा आवेदन-पत्र’ तैयार किया। इन सब कार्यों का ओकॉनल ने नेतृत्व किया। यह निश्चय किया गया कि 10 अप्रैल, 1848 को ‘तृतीय आवेदन-पत्र’ संसद के समक्ष पेश किया जायेगा।
तृतीय आवेदन-पत्र – 10 अप्रैल को ‘तृतीय आवेदन-पत्र को संसद में ले जाने कुछ हजार की संख्या में व्यक्ति ‘कैनिंगटन कॉमन’ नामक स्थान पर एकत्रित हुए। लगभग 5 लाख व्यक्ति एकत्रित होने की आशा थी, पर एकत्रित हुए केवल कुछ हजार । प्रधान सेनापति वैलिंगटन 1 लाख 7 हजार सैनिकों के साथ चार्टिस्टों का मुकाबला करने के लिए तैयार था। व्यक्तियों से कहा गया कि वे सभा कर सकते थे, पर अपने-जुलूस को संसद नहीं ले जा सकते थे। अतः सभा की गई और भाषण दिये गये। सभा खत्म होने के उपरान्त ओकॉनल अपने कुछ साथियों के साथ संसद की ओर चला। उसके पीछे तीन गाड़ियों पर लदा हुआ ‘आवेदन-पत्र’ था। वर्षा होने के कारण ओकॉनल के साथियों में से अनेक इधर-उधर भाग गये। अन्त में थोड़े से साथियों और ‘आवेदन-पत्र’ के साथ ओकॉनल ‘कॉमन-सभा’ में पहुँचा।
चार्टिज्म की असफलता के कारण
चार्टिज्म की असफलता के प्रमुख कारण निम्नवत् थे–
1. योग्य नेताओं का अभाव- वुडवर्ड (Woodward) के अनुसार चार्टिन्म के नेता न तो योग्य थे और न उनके पास आन्दोलन को सुचारू रूप से संगठित और संचालित करने के लिए समय था। उन्हें राजनीति का कोई ज्ञान भी नहीं था।
2. नेताओं में मतभेद- चार्टिज्म के नेताओं में मतभेद होने के कारण वे एक नीति का निर्धारण नहीं कर सके। चार्टिज्म दो दलों में बटा था। एक तरफ लावेट का दल शान्तिपूर्ण विधियों का प्रयोग करना चाहता था, तो दूसरी तरफ ओकॉनल का दल शक्ति का प्रयोग करना चाहता था।
3. विचारों की अज्ञानता- राबिन्सन (Robinson) का कहना है कि, चार्टिस्टों को स्वयं अपने विचारों का कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें यह ज्ञान न था कि वे क्या करने जा रहे थे? इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है- उनके एक जुलूस में से झंडे के ऊपरी भाग पर लिख हुआ था, “ईश्वर रानी की रक्षा करे” (“God save the Queen:”) और उसके नीचे शब्द थे, “क्योंकि कोई और रक्षा नहीं करेगा” “For nobody else will” I
4. शिकायतों का गलत निदान- चार्टिज्म नेता श्रमिक वर्गों की शिकायतों का निवारण नहीं कर सके। वस्तुतः उनकी मुख्य शिकायतें आर्थिक और सामाजिक थीं।
5. श्रमिकों में एकता का अभाव – इंग्लैंड के सभी श्रमिक वर्गों ने चार्टिस्ट आन्दोलन में भाग नहीं लिया। अनेक वर्ग ‘व्यापारिक संघों’ और ‘पारस्परिक सहयोग’ द्वारा अपनी स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे थे।
6. सम्पन्नता का आगमन – इंग्लैंड में दीर्घ काल से ‘अनाज-नियमों के कारण अन्न का अभाव था। 1846 में इन नियमों के निरस्त किये जाने से यह अभाव खत्म हो गया। चार्टिस्ट आन्दोलन का एक प्रमुख कारण महंगा अनाज था। अतः जब अनाज महंगा न रह गया, तब आन्दोलन का समाप्त होना अवश्यम्भावी था।
7. हिंसा का प्रयोग- चार्टिस्टों ने अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए हिंसा भी प्रयुक्त की । शान्तिपूर्ण विधियों से आन्दोलन करने का सम्भव है कि उनको सफलता मिलती। उनके बल प्रयोग के कारण अधिकांश जनता की उनके प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं रह गई ।
8. सरकार की नीति – ग्रीन (Green ) के अनुसार, सरकार ने चार्टिस्टों को कुचलने के लिए अति कठोर नीति का अनुसरण किया।
9. प्रार्थना पत्र पर जाली हस्ताक्षर – प्रार्थना पत्र पर पचास लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये जाने का दावा किया गया पर उनमें से आधे से अधिक हस्ताक्षर जाली थें हस्ताक्षर में कुछ नाम उदाहरणार्थ पगनोज (Pegnose), फ्लैटनोज (Flatnose) आदि हास्यास्पद और अद्भुत थे । इन जाली दस्ताखतों ने चार्टिस्ट आन्दोलन और उसके नेताओं को नैतिक रूप से बदनाम कर दिया।
10. मागें समय से पूर्व- चार्टिस्ट की मांगे समय से बहुत पूर्व की थीं, अतएव देश की अधिकांश जनता इन मांगों के द्वारा कोई सहानुभूति प्रदर्शित न कर सकी। जनता की इसमें किसी प्रकार की रूचि नहीं था। यह आन्दोलन पूरे राष्ट्र में रूचि और उत्साह उत्पन्न करने में असमर्थ रहा।
चार्टिस्ट आन्दोलन के परिणाम
चार्टिस्ट आन्दोलन के निम्नांकित परिणाम हुए—
1. जनता के कष्टों में कमी करना- यद्यति तत्कालीन प्रभावों को देखते हुए इस आन्दोलन को असफल कहा जा सकता है, पथापि जिन उद्देश्यों को लेकर इस आन्दोलन को शुरू किया गया था वह बाद में अन्य उपायों से पूर्ण हो गये। ‘दरिद्र अधिनियम’ के उचित प्रयोग से जनता के सभी कष्ट और विपत्तियों दूर हो गयीं। 1918 में सभी वयस्क पुरूषों और स्त्रियों को मताधिकार दे दिया गया। 1858 में संसद की सदस्यता के लिए सम्पत्ति की योग्यता खत्म कर दी गई। 1911 से संसद के सदस्य को वेतन दिया जाने लगा। 1872 में गुप्त मतदान की प्रथा शुरू की गई। 1855 में इंग्लैंड को समान निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। इस प्रकार चार्टिस्टों की 6 मांगों में से 5 मांगें पूरी की गयीं।
2. सभी वर्गों की शिक्षा – इस आन्दोलन ने अपनी विधियों और उद्देश्यों से इंग्लैंड के सभी वर्गों को शिक्षित किया। रेम्जेम्यारे के अनुसार, “चार्टिज्म ने श्रमिकों को शिक्षित करने का और भी अधिक कार्य किया। “
3. एकता की भावना – चार्टिज्म, इंग्लैंड के इतिहास में श्रमिकों का प्रथम संगठित आन्दोलन था। इसने कालान्तर में श्रमिकों में एकता और सहयोग की भावना को उत्पन्न किया। वे संगठित होकर सरकार और पूंजीपतियों पर अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए दबाव डालने लगे। एक होने के कारण उनको सफलता भी प्राप्त हुई।
4. टोरियों की प्रेरणा – चार्टिज ने टोरियों को प्रगति करने के लिए एक नई प्रदान की। पहले ‘डिजराइली के तरूण इंग्लैंड दल’ और बाद में ‘टोरी प्रजातन्त्र’ संगठित हुआ। इस प्रजातन्त्र के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार थे—
(i) कुलीन वर्ग द्वारा प्रजातन्त्र का संचालन,
(ii) औद्योगिकरण के दोषों का निवारण,
(iii) मध्यम वर्ग की प्रभुता का अन्त करना ।
5. ईसाई समाजवादियों के उपदेश- चार्टिस्ट आन्दोलन के प्रत्यक्ष प्रभाव ने ईसाई समाजवादियों को अपने उपदेश देने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रमुख समाजवादी-मॉरिस (Maurice), किंग्सल (Kingsley), ह्यूजेज (Hughes), लडलो (Ludlow) आदि थे।
6. श्रमिक वर्गों की स्थिति में सुधार- भविष्य में श्रमिक वर्गों की स्थिति में सुधार हुआ। इस आन्दोलन के फलस्वरूप कुछ वर्षों के उपरांत संसद का ध्यान इन वर्गों की ओर गया और उसने इनकी स्थिति को उन्नत करने के लिए विभिन्न अधिनियम पास किये, जैसे- कारखाना अधिनियम अनाज-नियमों की समाप्ति, खान अधिनियम और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम।
7. साहित्य पर प्रभाव- रेम्जेम्यारे का विचार है कि, चार्टिज्म का उस समय के साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा दरिद्रों के कष्टों को हुड (Hood) और मिसेज ब्राउनिंग (Mrs. Browing) ने अपनी कविताओं में जगह दिया। डिजराइली (Disraeli), मिसेज गेस्केल (Mrs-Graskell) और चार्ल्स किंग्सले (Charles Kingsley) ने निर्धनों की व्यथा को अपने उपन्यासों में चित्रित किया। कारलाइल (Carlyle) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकें “Chartism” और “Past Present” लिखीं।
उपसंहार- रेम्जेम्योर का कहना है कि “चार्टिज्म अपने तात्कालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा और यह अच्छा ही हुआ कि वह असफल हुआ, क्योंकि जनतन्त्र में अप्रशिक्षित व्यक्तियों की सत्ता सहसा स्थापित हो जाने से इंग्लैंड में निश्चित रूप से वैसी ही अनेक बुराइयां पैदा हो जाती है, जैसी फ्रांस में हुई थीं। यद्यपि चार्टिज्म असफल हुआ, पर उसने ब्रिटिश समाज के प्रत्येक दल और प्रत्येक विचारधारा के दृष्टिकोण और उद्देश्यों में महान् बदलाव कर दिया । “
अनाज अधिनियम
कृषि और कृषकों की रक्षा करने हेतु टोरी दल की सरकार ने सन् 1815 ई. में ‘अनाज-नियम’ लागू किया। इस नियम के अनुसार, जब तक इंग्लैंड में 1 क्वार्टर (Quarter) अनाज का मूल्य 80 शिलिंग से कम था, तब तक वहाँ विदेशी अनाज नहीं मंगाया जा सकता था। साउथगेट के शब्दों में, “यह उम्मीद की गयी कि एक क्वार्टर गेहूँ का मूल्य हमेशा 70 और 90 शिलिंग के मध्य ही रहेगा और यह दलील दी गयी कि गेहूँ कभी इतना सस्ता नहीं होगा कि किसानों को उसे उत्पन्न करने से न हो और न रोटी इतनी महंगी होगी कि निर्धन व्यक्ति खरीद न सकें । “
अनाज अधिनियम की आवश्यकता- इंग्लैंड में ‘अनाज नियम’ की जरूरत ‘वाटरलू के युद्ध’ के उपरान्त देश में शान्ति की स्थापना के परिणामस्वरूप महसूस की गयी थी। नेपोलियन के खिलाफ युद्ध के दौरान सैनिकों और औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप नगरों की बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन की अधिक मांग रही । अतः कृषकों ने उस अनुपजाऊ भूमि पर भी खेती की। ब्रिकी होती रही। युद्ध खत्म होने के उपरान्त उस अन्न की मांग बन्द हो गई क्योंकि विदेशों से अच्छा अनाज का मूल्य गिरने से किसान निर्धनता की ओर अग्रसर होने लगे। रेम्जेम्योर के शब्दों में, ‘‘कृषि को हानि हुई। अनाज का मूल्य अकस्मात 40 प्रतिशत कम हो गया और अनेक किसान बर्बाद हो गये । “
अन्य ‘अनाज नियम’- सन् 1815 ई. के ‘अनाज – नियम’ में सरकार सफल नहीं हो सकी। गेहूँ का मूल्य 70 और 90 शिलिंग के बीच में नहीं रहा। उदाहरणार्थ- सन् 1817 ई. में उसका मूल्य बढ़कर 188 शिलिंग और 1822 में घटकर 39 शिलिंग हो गया।
साउथगेट के शब्दों में किसान बर्बाद हो गये और अनेक फार्मों में कृषि कर्म खत्म हो गया। इसके लिए रोटी का मूल्य अकाल के समय का-सा रहा और निर्धन व्यक्तियों के अन्य कष्टों में भोजन का अभाव सम्मिलित हो गय।”
निर्धन तथा बेरोजगार जनता महंगाई के कारण दुःखी हो रही थी। ‘अन्न-नियम’ के पास हो जाने के कारण धनी और अधिक धनी तथा निर्धन और अधिक निर्धन हो रहे थे। देश में व्यापक असन्तोष की भावना व्याप्त थी।
कौब्डन तथा जान ब्राइट के प्रयासों के कारण एक अन्न नियम विरोधी लीग (Anti Corn Law League) की स्थापना की गई तथा अन्न नियम को भंग कराने के लिए आन्दोलन का उद्देश्य निर्धन जनता को सस्ती वस्तुएं प्रदान कराना था। भूमिपति संसद में परिश्रम करते रहे। सन् 1939-40 ई. में आन्दोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। लन्दन में 12 सप्ताह के अल्पकाल में ही 150 से अधिक सभाएँ आयोजित की गयीं। सन् 1839 ई. में लीग का चन्दा केवल 5 हजार पौंड था, परन्तु सन् 1844 ई. में यह बढ़कर 90 हजार पौंड हो गया। 1815 के पश्चात् खराब होने वाली फसलों ने कृषकों और दरिद्रों के दुःखमय जीवन को और अधिक दुःखमय बनाया।
उनकी रक्षा करने के लिए 1824 में कैनिंग (Canning) ने विदेशों से आयोजित अनाज पर ‘कर-निर्धारण विधि’ (Slidning Scale of Duties) की एक योजना बनाई, जिसके अनुसार, इंग्लैंड में अनाज का मूल्य 64 शिलिंग या इससे कम होने पर विदेशी अनाज पर 25 शिलिंग 8 पेंस आयात कर दिया जाता था। यह योजना 1841 तक चलती रही। 1841 में व्हिगों ने यह प्रस्ताव पेश किया टोरी और व्हिग दोनों ने स्वीकार किया कि देश के लिए ‘अनाज-नियम’ (Corn Laws) आवश्यक थे।
पोल और अनाज नियम- पोल का ‘संरक्षण’ में विश्वास था । वह स्वतन्त्र व्यापार का विरोधी था। पर वह अपने अनुभव और परिस्थितियों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता था। अतः वह शुरू में ‘अनाज – नियम’ का समर्थक था, पर धीरे-धीरे वह उसका विरोधी हो गया। साउथगेट का कथन है “1841 में उसने ‘अनाज-नियम’ के समर्थक के रूप में शक्ति प्राप्त की थी, पर जब उसने देखा कि उद्योग और कृषि का संरक्षण देश के सर्वोत्तम हितों के प्रतिकूल था, तब उसने महसूस किया कि परिस्थितियों की सर्वाधिक प्रबल मांग, सस्ता देश बनाना चाहिए।” 1841-42 में फसलें बहुत खराब हो गयीं और अनाज आयातित न होने के कारण रोटी का मूल्य 10 पैसे बढ़कर 1 प्रिंलिंग और 2 पैंसे हो गया।
महँगाई के फलस्वरूप, जनसाधारण का कष्ट देखकर पोल न ‘अनाज-नियमों से देश की कृषि, कृषकों, श्रमिक वर्गों और जमींदारों का अहित हो रहा है, तो उनको खत्म कर दिया जाना चाहिए, पर पोल का प्रधानमन्त्री के रूप में निर्वाचन ‘अनाज-नियमों’ का समर्थन करने के कारण हुआ था, अतः वह उनकी प्राप्ति करने में असमर्थ था। उसने आयात-कर-निर्धारण विधि’ कार्यान्वित की। इसमें यह व्यवस्था थी कि अनाज का मूल्य 73 शिलिंग या अधिक होने पर आयात कर 1 शिलिंग और 50 से 51 शिलिंग तक होने पर 20 शिलिंग आयात – कर लगाया जायेगा।
अतः अनाज के मूल्य में अधिकता होने पर आयात-कर में कमी और कम होने पर अधिक आयात कर लगाया गया। यद्यपि इस विधि से अनाज की मँहगाई की समस्या आंशिक रूप से सुलझी, पर पोल अथवा जनता को अधिक सन्तोष न हुआ। अतः पोल ने ‘अनाज-नियमों’ की समाप्ति करने का फैसला लिया। उसे इस दिशा में निम्नलिखित 3 अन्य कारकों से भी सहयोग प्राप्त हुआ—
1. उत्पादकों और मजदूरों की मांग,
2. अनाज-नियम ‘विरोधी संघ’ और
3. आयरलैंड का दुर्भिक्ष
1. उत्पादकों और मजदूरों की मांग- चूँकि अनाज का मूल्य अधिक हो गया था, अतएव उत्पादकों को श्रमिकों को ऊँची मजदूरी देनी पड़ती थी। वे ‘अनाज-नियमों’ को खत्म करके विदेशी अनाज की इंग्लैंड में स्वतन्त्रतापूर्वक आयात की मांग कर रहे थे, ताकि अनाज सस्ता हो जाये तथा उनको श्रमिकों को कम मजदूरी देनी पड़े।
2. अनाज नियम विरोधी संघ- ‘अनाज-नियम विरोधी संघ’ की स्थापना 1838 में लंकाशायर के कुछ मिल-मालिकों द्वारा मानचेस्टर (Manchester) में की गई थी। इस ‘संघ’ के सदस्य कहते थे कि ‘अनाज-नियमों ने देश में अनाज के मूल्य में वृद्धि कर संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी थी। वे इन नियमों की समाप्ति के साथ-साथ ‘स्वतन्त्र व्यापार’ का समर्थन कर रहे थे। रेम्जेम्योर के शब्दों में, “यद्यपि ‘संघ’ के वक्ताओं ने ‘अनाज-नियमों’ को अपने हमले का मुख्य लक्ष्य बनाया पर उतनी ही शक्ति से सार्वभौमिक स्वतन्त्र व्यापार की जरूरत का समर्थन किया। “
‘संघ’ के प्रबल समर्थक रिचर्ड कॉबडन (Cobden) और जॉन ब्राइट (John Bright) थे। ये दोनों मित्र जगह-जगह जाकर ‘अनाज- नियमों की समाप्ति एवं स्वतन्त्र व्यापार की उपयोगिता पर भाषण दिया करते थे।
कॉबडन ने 1841 में कॉमन-सभा की सदस्यता ग्रहण की। 1843 में ब्राइट भी कामन सभा का सदस्य बना। दोनों मित्रों ने समय-समय पर संसद के भाषण देकर पोल को अत्यधिक प्रभावित किया।
चार्ल्स विलियर्स (Charles Viliers) भी कॉमन सभा का सदस्य, ” स्वतन्त्र व्यापार’ का समर्थक और ‘अनाज – नियमों का विरोधी था। उसने 1838 से 1845 तक ‘अनाज- नियमों का विरोधा किया। उसे लार्ड ग्रे ( Lord Grey) और मिलनर गिब्सन (Milner Gibson) ने मद्द की।
3. आयरलैंड का दुर्भिक्ष- 1845 में आयरलैंड में आलू की फसल खराब हुई। 80 लाख निवासियों में 40 लाख अपने भोजन के लिए आलू पर निर्भर थे। अतएव 40 लाख व्यक्तियों को भोजन देना सरकार का कर्त्तव्य था। यह कार्य मुश्किल था। इंग्लैंड की अनाज की फसल भी खराब हो गई थी। इस कठिन कार्य का मुकाबला करने का पोल के सामने एकमात्र उपाय था, ‘अनाज नियमों’ की समाप्ति । पोल ने 13 अक्टूबर 1845 को अपने गृहमन्त्री सर जेम्स ग्राहम को लिखा, “मुझे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर प्रतिबन्धा लगाने के समान उपायों में तनिक भी विश्वास नहीं है। आयात पर लगे हुए प्रतिबन्धों की समाप्ति मात्र प्रभावपूर्ण उपाय है। “
पोल का त्याग-पत्र- पोल ने डाक्टर लियॉन नामक दो विशेषज्ञों को आयरलैंण्ड में अकाल से उत्पन्न होने वाली स्थिति की जाँच करने के लिए भेजा। उन्होंने आयरलैंड की स्थिति का भयंकर चित्र प्रस्तुत किया। अतएव पोल ने ‘अनाज – नियमों’ को समाप्त करने का निश्चय कर लिया पर पोल अपने निश्चय को अपने दल के विरोध के कारण क्रियान्वित नहीं कर सका। अल के द्वारा अत्यधिक विरोध किये जाने पर उसने 5 सितम्बर, 1845 ई. को इस्तीफा दे दिया।
“अनाज-नियम” समाप्ति की योजना “
पोल के त्यागपत्र देने के उपरान्त महारानी विक्टोरिया ने लार्ड जॉन रसल से मन्त्रिमण्डल का गठन करने का आग्रह किया, पर रसल इसमें सफल नहीं हो सका। अतः पोल ने पुनः प्रधानमंत्री का पद भार ग्रहण किया। 27 जनवरी, 1846 को पोल ने ‘अनाज नियम’ की समाप्ति की अपनी योजना कॉमन-सभा के समक्ष रखी। मैरियट के मतानुसार, इस योजना के सिद्धान्त निम्नलिखित थे—
(i) उत्पादकों के लिए सस्ते कच्चे माल का आयात, पर विदेशी प्रतिद्वन्द्विता से किसी प्रकार का संरक्षण नहीं ।
(ii) किसानों के लिए सस्ता बीज, पर विदेशी अनाज की प्रतिद्वन्द्विता से किसी प्रकार का संरक्षण नहीं ।
(iii) सबके लिए सस्ती विदेशी वस्तुएं । पोल ने कॉमन सभा के सदस्यों के समक्ष कहा कि ‘अनाज-नियमों की समाप्ति निम्न प्रकार की जायेगी—
1 फरवरी, 1849 के पश्चात् अनाज पर ‘आयात कर’ केवल 1 शिलिंग प्रति क्वार्टर के हिसाब से लिया जायेगा । 1 जनवरी, 1849 तक अनाज का मूल्य 48 शिलिंग के हिसाब से आयात कर लिया जायेगा।
‘अनाज-नियम’ की समाप्ति- पोल की ‘अनाज-नियमों’ की समाप्ति की योजना का उसके सदस्यों ने डिजराइली और लार्ड जार्ज बैंटिक की मदद से विरोध किया और उसके खिलाफ वोट दिया पर पोल ने उदार दल के सदस्यों का समर्थन प्राप्त कर ‘अनाज-नियमों’ को खत्म कर दिया। लार्ड सभा ने भी इस समाप्ति को स्वीकार कर लिया।
अनाज-नियम की समाप्ति के परिणाम
‘अनाज-नियम’ की समाप्ति के निम्नांकित परिणाम हुए—
1. राजनैतिक शिक्षा – ट्रेवियन (Travelyan) ने लिखा कि “अनाज-निमयों” को खत्म कर ‘अनाज-नियम विरोधी संघ’ (Anti-Cron Legue) ने इंग्लैंड के निवासियों को राजनैतिक शिक्षा प्रदान की। इंग्लैंड का प्रशासन जनतन्त्र की शिक्षा में और आगे बढ़ा। 1867 और 1884 के पश्चात् लाखों व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त हो गया।
2. मध्यम वर्गों की विजय – कॉबडन (Cobden) के अनुसार, ‘अनाज – नियम विरोधी-संघ’ (Anti-Corn Legue) मध्यम वर्गों का आन्दोलन था । ‘अनाज-नियमों’ की समाप्ति इस संघ और मध्यम वर्ग की विजय थी।
3. आर्थिक नीति में परिवर्तन- इंग्लैंड की आर्थिक नीति में महान् परिवर्तन हुआ। ‘संरक्षण’ (Protection) का अन्त कर ‘स्वतन्त्र व्यापार’ इग्लैंड की व्यापारिक नीति बनी। इंग्लैंड को उस प्रणाली से छुटकारा प्राप्त हुआ जिसने उसके व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था।
4. धन की वृद्धि – ‘अनाज-नियमों’ की समाप्ति से विदेश से आने वाला अनाज कर से मुक्त हो गया। इंग्लैंड में अनाज का भाव लगभग एक पीढ़ी तक एक समान ही रहा। ट्रलेलियन ने लिखा, “इंग्लैंड के देहात के मकान और फार्म इससे अधि क धनी, बसे हुए और सुखी कभी नहीं थे, जितने कि मध्य विक्टोरिया युग में थे। “
5. राजनैतिक परिणाम- ट्वेलियन ने लिखा, “अनाज-नियमों की समाप्ति प्रथम और द्वितीय सुधार बिलों के मध्य में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घटना थी। इसने अनुदार दल को भंग कर दिया और इस प्रकार व्हिगों को शक्तिसम्पन्न बनाया।”
व्यापारिक और औद्योगिक विस्तार- ‘अनाज- नियमों की समाप्ति के साथ उनके सम्बन्ध में चलने वाले झगड़ों की समाप्ति के फलस्वरूप देश में व्यापक उत्तेजना खत्म हो गई। व्यापार एवं उद्योग की ओर पूर्ण ध्यान दिया जाना शुरू हुआ। इसके फलस्वरूप व्यापारिक और औद्योगिक विस्तार हुआ। देश दिन-प्रतिदिन वैभवशाली होने लगा।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here