थॉमस हॉब्स के राजनीतिक दृष्टिकोण
थॉमस हॉब्स के राजनीतिक दृष्टिकोण
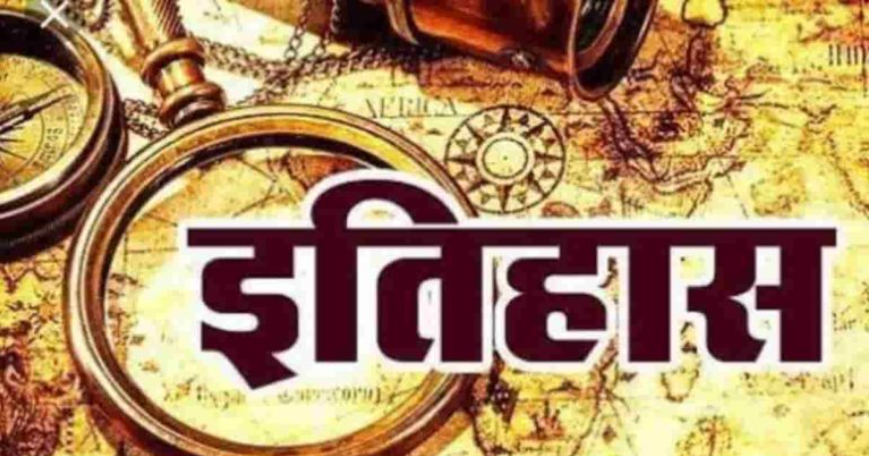
राजनीतिक दृष्टिकोण (Political View )
बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स के राजनीतिक दृष्टिकोण अथवा विचार को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है—
मानव का स्वभाव— मानव के स्वभाग के विषय में हॉब्स का मानना था कि, “किसी भी राजनीतिक समाज का अध्ययन मानव सभाव के अध्ययन से प्रारंभ होना चाहिए । ” इसके अलावा इनका यह भी मानना था कि मनुष्य स्वभाव से झगड़ालू, स्थार्थी, ईर्ष्यालु प्राणी है। मनुष्य सहानुभूति और खुशी का प्रदर्शन भी इन्हीं मौलिक गुणों के परिणामस्वरूप करता है। अगर एक व्यक्ति दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो इसलिए नहीं कि वह वास्तव में उस व्यक्ति के दुःख से दुःखी है बल्कि इसलिए दिखाता है कि वह उस व्यक्ति के दुःख से विचलित हो गया है और स्वयं इसलिए प्रसन्न है कि वह दुःख उसे नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य को हँसी, दूसरे की दुर्दशा या अपने कार्यों के परिणामस्वरूप आती है। इसके आगे इन्होंने यह भी लिखा है कि, “हँसी अच्छे स्वभाव की निशानी नहीं है। इसके आगे इन्होंने यह भी लिखा है कि, “हँसी अच्छे स्वभाग की निशानी नहीं है। यह या तो मनुष्य को अपने ही आनन्द योग्य कार्यों से प्राप्त होती है या दूसरे में किसी कमजोरी को देखकर जो स्वयं में नहीं आती है। ” हॉब्स मानव को असामाजिक प्राणी जानता है। हॉब्स मानव को चींटियों और मधुमक्खियों से भी गया गुजरा मानता है, क्योंकि चींटिया और मधुमक्खियाँ आपस में नहीं लड़ती, जबकि मानव आपस में लड़ता है l
मानव स्वभाव के संदर्भ में हॉब्स ने यह भी लिखा है कि, “मानव को वस्तुएँ आकर्षित लगती हैं या उसे अलगाव रहता है । आकर्षण की इच्छा को तृष्णा कहतें हैं, अलगाव को घृणा कहते हैं।” आदि मानव असभ्य एवं असामाजिक था. अतः इसे सामाजिक जीवन से कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल अपने स्वार्थ- पूर्ति के कारण सामाजिक व्यवहार में संघर्षपूर्ण बना रहा। व्यक्ति अपनी वस्तु को बनाये रखना चाहता है, दूसरों की वस्तुओं पर अधिकार करना चाहता है। मनुष्य अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। इसी कारण उसमें परोपकारी गुण का अभाव था। थॉमस हॉब्स का मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं। शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों की दृष्टि से प्रकृति ने सभी मनुष्यो को इतना बराबर बनाया है कि यद्यपि एक-दूसरे की अपेक्षा शारीरिक रूप से अधिक बलवान और बौद्धिक रूप से अधिक तीक्ष्ण हो सकता है, किंतु यदि सभी बातों को ध्यान में रखा जाये तो विभिन्न मनुष्यों के बीच अधिक अंतर नहीं है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि शारीरिक बल की दृष्टि से दूसरे मनुष्य की अपेक्षा निर्बल व्यक्ति मानसिक दृष्टि से अधिक बुद्धिमान, धूर्त और प्रपंची होता है और सामर्थ्य की समता के फलस्वरूप लक्ष्य प्राप्ति की आशा की समानता विकसित होती है। इसीलिए जब दो व्यक्ति एक ही वस्तु को प्राप्त करने के निमित्त प्रयत्नशील होते हैं, तब दोनों एक-दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। मानव स्वभाव के अन्तः विचार के सन्दर्भ में यह लिखा है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है तथा अधिकाधिक शक्ति स्वयं प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहता है । इसके अलावा इन्होंने यह भी लिखा है कि, “भय के आर्त्त और स्वार्थ साधन में चतुर व्यक्ति निरंतर शक्ति प्राप्त करने और प्राप्त शक्ति की वृद्धि में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए तो शक्ति आवश्यक है । “
सेबाइन ने हॉब्स के विचारों का समर्थन करते हुए यह लिखा है कि, “मानव प्रकृति की मूलभूत आवश्यकता आत्म-रक्षा है जिसे शक्ति की कामना से पृथक नहीं किया जा सकता। यह कामना भविष्य में भलाई के साधन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहती है, क्योंकि प्रत्येक सुरक्षा की मात्रा अधिक सुरक्षा चाहती है” हॉब्स महोदय ने मानव स्वरूप के विषय में यह लिखा है कि, “संपूर्ण मानव जाति शक्ति की शाश्वत् अतिश्रान्त इच्छा से प्रेरित है। इस लालसा का अंत मृत्यु के साथ ही होता है। इसका कारण यह नहीं है कि मनुष्य के पास इस समय जितनी प्रसन्नता है वह उससे अधिक प्रसन्नता चाहता है या कुछ कम शक्ति से उसका काम नहीं चल सकता। इसका कारण यह है कि मनुष्य के पास इस समय जीविका के जो साधन हैं और जितनी शक्ति है उससे अधिक प्राप्त किये बिना उसकी रक्षा का आश्वासन नहीं मिलता।”
हॉब्स के उक्त कथन का अवलोकन करने यह यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मानव को प्रत्येक ढंग की शक्ति, सम्पत्ति, पद और सम्मान की भूख है। क्योंकि ये सारी वस्तुएँ उस अपरिहार्य विनाश को रोकती हैं, जो किसी दिन प्रत्येक मानव पर छा जाता है।
प्रतिस्पर्धा, भय और पारस्परिक अविश्वास तथा वैभव यह तीनों तत्व सतत् संघर्ष के प्रमुख कारण हैं। हॉब्स का मानना है कि, “हम मानव स्वभाव में झगड़े के तीन मुख्य कारण देखते हैं- पहला प्रतिस्पर्धा, दूसरा भय और तीसरा वैभव। इनमें प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ के लिए परस्पर संघर्ष करते हैं। दूसरा कारण अर्थात् भय सुरक्षा के लिए तीसरा कारण यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यद्यपि मानव शांति का आकांक्षी है, किंतु वह सदैव दूसरों से भयभीत रहता है। सम्पत्ति की चाह और कीर्ति की प्यास भी नहीं छूटती । फलतः अपने साथियों के साथ वह सत्त संघर्ष में संलग्न रहता है। ” हॉब्स ने यह भी लिखा है कि मानव ऊपर से देखने में सभ्य, शिष्ट और सज्जनता की प्रतिमूति प्रतीत होता है, परन्तु मानव वास्तव में स्वार्थी है और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वह दूसरों का बड़े से बड़ा अहित कर सकता है।
हालांकि हॉब्स ने मानव स्वभाव को एक तरफ बुरा कहा है, तो दूसरी तरफ उसके अच्छे गुणों की कल्पना भी की है। हॉब्स का मानना है कि, “मनुष्य में कुछ ऐसी इच्छाएँ भी होती हैं जो उसे युद्ध के लिए नहीं अपितु शांति एवं मैत्री के लिए के प्रेरित करती हैं। आराम की इच्छा, ऐन्द्रिक सुख की कामना, मृत्यु का भय, परिश्रम से अर्जित वस्तुओं के भोग की लालसा मनुष्य को एक शक्ति की आज्ञा मानने हेतु मजबूर कर देती है, क्योंकि सामान्य शक्ति के नियंत्रण में रहकर ही मनुष्य की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है।
प्राकृतिक अवस्था— थॉमस हॉब्स महोदय ने माना कि मानव स्वभाव की भांति यह अवस्था भी सतत् युद्ध व संघर्ष की अवस्था थी, मानव मानव का दुश्मन था। प्रत्येक मानव को अन्य मानव से भय बना हुआ था।
प्राकृतिक अवस्था में केवल धोखाधड़ी और शक्ति ही मानव जीवन के मुख्य तत्व थे। हॉब्स ने लिखा है कि यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें शासक कानून तलवार का कानून था। इसलिए “मनुष्य का जीवन प्राकृतिक अवस्था में एकाकी, असहाय, कुत्सित, पाशविक और क्षणिक होता था।” इस प्रकार हॉब्स द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था “जिसकी लाठी उसकी भैंस ” वाली अवस्था थी। उसके अनुसार इस प्राकृतिक अवस्था में अधिकार, स्वतंत्रता या कानून यही था कि “प्रत्येक मनुष्य को अपनी जीवन रक्षा की पूरी स्वाधीनता है।” उस समय जीवन का नियम था, ‘‘प्रत्येक मनुष्य का केवल वही अपना होगा जिसे वह पास सकता है और तब तक के लिए ही जब तक वह उसे रख सकता है।” इस प्राकृतिक अवस्था का एक कानून था, “जिसे मार सकते हो, उसे तुम मारो और जो तुम लूट सकते हो उसे लूट लो।” हॉब्स द्वारा चिंतित प्राकृतिक अवस्था में उचित-अनुचित, न्याय व अन्याय का काई महत्व नहीं था, धोखा और शक्ति ही मुख्य गुण समझे जाते और मनुष्य का जीवन सदैव खतरे में था। इस अंधकारपूर्ण प्राकृतिक स्थिति में संस्कृति, सभ्यता, कला, विज्ञान जैसी विधाओं का विकास नहीं हो पाया था। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में अराजकता का बोलबाला था। मानव का जीवन सुरक्षित नहीं था। हॉब्स के शब्दों में, “ऐस समय में जब मनुष्य एक ऐसी शक्ति के बिना रहते थे जो उन्हें भयभीत बनाये रखे, वे उस अवस्था में रहते थे जिसे युद्ध कहा जाता है और वह ऐसा युद्ध होता है जो प्रत्येक मनुष्य की ओर से प्रत्येक मनुष्य के विरुद्ध होता है। ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, समुद्री – परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों, ज्ञान, समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता तथा मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाविक एवं क्षणिक होता है । “
प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम
प्राकृतिक अधिकार वह अधिकार कहलाता है जिसमें मानव को अपने जीवन की सुरक्षा हेतु कोई भी कार्य करने की पूरी छूट प्राप्त होती है। कोई भी मानव अपने जीवन को बनाये रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने या जान से मार डालने की स्वतंत्रता रखता है। टी. एच हक्सले ने ऐसे अधिकार को ‘शेर का अधिकार’ कहा है। जैसे शेर को अपना शिकार मारने की स्वतंत्रता है, वैसे ही मनुष्य को भी हिंसा और हत्या की पूरी स्वतंत्रता है, बशर्ते कि इससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके।”
परन्तु हॉब्स इस अधिकार के साथ-साथ कुछ प्राकृतिक नियमों को भी मान्यता देता है। इन प्राकृतिक नियमों का पालन करने से प्राकृतिक अधिकार प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण होता है। हॉब्स के अनुसार मानव के “प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबको एक-दूसरे की हत्या और लूटमान का अधिकार मिल जाता है जिससे जीवन सर्वथा असुरक्षित हो जाता है। लेकिन सभी व्यक्ति जीवन को सुरक्षित बनाये रखना चाहते हैं, अत: वे प्राकृतिक दशा में भी अपनी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कुछ नियम बना लेते हैं। इन नियमों का पालन करके मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में भी अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं ।
ये प्राकृतिक नियम के नियंत्रण हैं जो मनुष्य अनुभव द्वारा सीखता है और जिनहें वह अपने जीवन के लिए लाभदायक पाता है। प्राकृतिक नियम के सन्दर्भ में थॉमस हॉब्स का मानता है कि, “यह वह नियम है जो विवेक द्वारा खोजा गया है, जिसके द्वारा मनुष्य के लिए वे कार्य निषिद्ध हैं जो उसके जीवन के लिए विनाशप्रद हैं या जिनसे जीवन की रक्षा के साधनों का हरण होता है जिनके द्वारा उसके लिए उन कार्यों का न करना निषिद्ध है जिनसे जीवन की रक्षा होती है । ” परंतु ऐसे नियमों को कानून की संज्ञा देना सम्भव नहीं है, क्योंकि कानून तो संप्रभु की आज्ञा है। प्राकृतिक नियम मनुष्य को बाध्य करता है कि वह प्राकृतिक अवस्था में आत्मरक्षा के लिए इच्छानुसार कुछ भी करने की मिली हुई अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता का कुछ अंश त्याग दे, जिससे वह शेष स्वतंत्रता का अधिक निश्चित रूप से उपभोग कर सके। इस प्रकार प्राकृति नियम पूर्ण स्वेच्छाचारिता तथा अनुत्तरदायित्व के बीच एक कड़ी थी। इसी आधार पर हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम दोनों के मध्यस पाये जाने वाले भेद व अन्तर को बताते हुए यह लिखा है कि प्राकृतिक अधिकार अवस्था को निरंतर संघर्ष की स्थिति बना देते हैं जबकि प्राकृतिक नियम पर आचरण करके मनुष्य प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बच सकते हैं और आत्म-परीक्षण के उद्देश्य से सरलता से प्राप्त कर सकते हैं।
सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति
थॉमस हॉब्स महोदय ने जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वह आशाजनक न होकर बल्कि बड़ा निराशाजनक ही साबित होता है। उसकी मान्यता के अनुसार राजय की उत्पत्ति प्राकृतिक अवस्था की इसी दुःखमय स्थिति से हुई है। निराशापूर्ण और दु:खदायी जीवन से लोग ऊब जाते हैं। वे अपनी इस संघर्षमयी, नीच, अव्यवस्थित एवं पाशविक अवस्था को दूर करने की आवश्यकता समझते हैं तथा एकमत होकर समझौता करने के पक्ष में होते हैं। उनका विवेक उन्हें प्राकृतिक विधियों की उपयोगिता बताता है। अतः जीवन की सुरक्षा के लिए और भयंकर प्राकृतिक अवस्था से मुक्त होने के लिए वे एकत्रित होकर जो समझौता करते हैं, उससे राज्य का कल्याण एवं लाभ होता है।
हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सन्दर्भ में यह लिखा है कि राज्य एक सामाजिक समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। राज्य की स्थापना का वर्णन हॉब्स ने लेवियाथन में इस प्रकार किया है, “एक राज्य की स्थापना तब होती है, जब अनेक व्यक्ति एक-दूसरे के कार्यों को अपना कार्य समझेंगे जिसे उनके अधिकांश भाग ने अपना प्रतिनिधि चुना है, चाहे उनमें से किसी ने उसके पक्ष में मत दिया हो या विरोध में। इस समझौते का उद्देश्य यह है कि मनुष्य शांतिपूर्वक और दूसरों के विरुद्ध सुरक्षित रहे। इस तरह से जो भी चीज उत्पन्न होती है वह केवल रजामंदी से कुछ बढ़कर है। यह समस्त व्यक्तियों का वास्तविक इकाई में एकीकरण है जिसकी सिद्धि प्रत्येक के साथ समझौते द्वारा हुई है । “
यह समझौता इस प्रकार हुआ। हॉब्स का मानना है कि प्रत्येक ने एक सभा या व्यक्तियों के सम्मुख कहा, “मै अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपने सब अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों को स्वीकृति दोगे।” इससे आगे इन्होंने यह भी विचार दिया कि इस मर्त्यप्रभु (लेवियाथन) का इस रीति से जन्म होता है। वही वह मर्त्यप्रभु है जिसकी कृपा पर अनश्वर ईश्वर की छात्रछाया में हमारी शक्ति तथा सुरक्षा निर्भर है।
इस समझौते से सभी लोगों ने अपने सभी अधिकार एक व्यक्ति की सभा को दे दिये परन्तु वह व्यक्ति इस समझौते से सन्तुष्ट नहीं हुआ और वह निरंकुश सत्ता (संप्रभु) बना और समझौते में सम्मिलित सभी व्यक्ति उसकी प्रजा बने। इस संप्रभु को हॉब्स ने लेवियाथन का नाम दिया।
प्रभुसत्ता— हॉब्स ने प्रभुसत्ता सिद्धान्त का भी चित्रण किया जिस पर सामाजिक समझौते सिद्धान्त का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा। समझौते के परिणामस्वरूप उत्पन्न संप्रभु सर्वोच्च सत्ता, सम्पन्न और निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश कानून है और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। उसे जनता के जीवन को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार प्राप्त है तथा जनता को किसी भी प्रकार से उसे चुनौती देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। इस सन्दर्भ में हॉब्स का मानना है कि जनता का एक मात्र कायर्स संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वह आदेश ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों न हो। जनता के लिए उनका पालन करना ही न्यायपूर्ण और वैध है। संप्रभु को जनता की सम्पत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का भी अधिकार है, इसका प्रमुख कारण यह है कि जनता की सम्पत्ति और जीवन उसकी सत्ता से ही सुरक्षित नहीं है। अतः यदि प्रजाजन संप्रभु की आज्ञा का किसी भी रूप में विरोधा करते हैं, तो उनका यह व्यवहार अनुचित है। यहाँ तक कि एक संप्रभु की स्थापना कर लेने पर उसके स्थान पर दूसरे संप्रभु की स्थापना करना भी संविदा को भंग करना और पुनः प्राकृतिक स्थिति में पहुँच जाना होगा। इस दृष्टि से अत्याचारी शासक की हत्या करना भी हॉब्स को स्वीकार नहीं है ।
उन सभी संगठनों व संस्थाओं की हॉब्स आलोचना करता है जो सत्ता के अधिकार को सीमित करने का प्रयास करती हैं। वह शक्ति के पृथक्करण एवं मिश्रित शासन-व्यवस्था का भी विरोध करता है। उसका मत है कि ऐसी व्यवस्थाएँ अराजकता उत्पन्न करने वाली होती हैं। उसके अनुसार इंग्लैण्ड में उसके समयस में होने वाले गृहयुद्ध का यही कारण था, जिसका वजह से लोग यह सोचते थे कि सर्वोत्तम सत्ता राजा और संसद में बंटा हुआ है। अतः थॉमस हॉब्स प्रभुसत्ता को सम्पूर्ण अविभाज्य तथा असीम कहता है ।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता— वैयक्तिक स्वतंत्रता के सन्दर्भ में हॉब्स का मानना है कि व्यक्ति जिन कार्यों को सम्पन्न करने की इच्छा करता है, उन पर बाह्य प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। प्रभुसत्ता की असीम शक्ति का समर्थन करने के बाद हॉब्स ने निम्नलिखित क्षेत्रों में मानव को स्वतंत्रता दी है—
1. क्षेत्र तो आर्थिक समझौते का है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को क्रय-विक्रय करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।
2. क्षेत्र में प्रत्येक को अपने निवास स्थान, भोजन और व्यापार चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है।
3. क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार बच्चों को शिक्षा दिलाने की स्वतंत्रता है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान कर अखण्ड प्रभुसत्ता का समर्थक हॉब्स सर्वग्राहिता के आरोप से मुक्त हो गया है।
संप्रभु की अवज्ञा का अधिकार— हॉब्स ने निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यक्ति या मानव को संप्रभु की अवज्ञा का अधिकार दिया है—
1. यदि संप्रभु किसी व्यक्ति को दूसरों की हत्या करने का आदेश देता है, तो ऐसे आदेश को न मानने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को है।
2. कोई व्यक्ति कुछ अवस्था विशेष में सेना में भर्ती होना अस्वीकृत कर सकता है और डरपोक होने पर प्राण रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग सकता है।
3. यदि संप्रभु किसी व्यक्ति को ऐसी आज्ञा दे कि वह अपने को मार डाले, अपने अंगों को पीड़ित करे। यदि कोई दूसरा उस पर आक्रमण करे तो प्रतिरोध न करे अथवा भोजन, वायु, चिकित्सा आदि से परहेज करे, तो ऐसी आज्ञा को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता प्रत्येक मानव को है।
4. कोई भी व्यक्ति अपने उन दोषों को मानने से इन्कार कर सकता है, जिसके कारण उसकी जान व प्राण जाने की सम्भावना है।
शासन— हॉब्स शासन के तीन भेद बताये हैं जिसमें पहला यदि प्रभुसत्ता एक व्यक्ति में निहित हो तो राजतंत्र होता है। दूसरा यदि कुछ व्यक्तियों में निहित हो तो कुलीनतंत्र और तीसरा समाज के सब व्यक्तियों में निहित हो तो लोकतंत्र होता है। अत: इन तीनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई शासन नहीं होता। प्रभुसत्ता को अविभाज्य मानने के कारण वह मिश्रित संविधान व्यवस्था का घोर विरोधी है। इन तीनों में हॉब्स राजतंत्र को निम्नलिखित कारणों से अधिक उपयुक्त मानता है—
1. राजतंत्र में यद्यपि अपने कृपापात्रों को धन और अधिकार देने की प्रवृत्ति होती है, परंतु लोकतंत्र में यह समस्या सबसे अधिक पायी जाती है, क्योंकि इनमें शासकों की संख्या अधिक होने से उनके कृपापात्र भी बढ़ जाते हैं।
2. राजतंत्र में राजा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से किसी स्थान पर गुप्त रूप से मंत्रणा कर सकता है, क्योंकि वह अकेला व्यक्ति होता है। अन्य प्रकार के राज्यों में शासकों का एक समुदाय होने से ऐसा होना संभव नहीं है।
3. राजतंत्र में शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, हालांकि उत्तराधिकार में नाबालिग या उत्तराधिकारी की दृष्टता मानसिक खराबी के कारण गड़बड़ी हो सकती है पर समुदाय का वर्ग के शासन में स्वार्थी की दौड़ इतनी अधिक होती है कि एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धा में राज्य का विनाश हो जाता है।
4. राजतंत्र में राजा तथा राज्य का वैयक्तिक और सार्वजनिक हित एक होता है। राजा के धन और कीर्ति की वृद्धि राज्य की सम्पत्ति और यश को बढ़ाने वाली होती है।
5. राजतंत्र में शासन की स्थिरता और स्थायित्व अधिक होता है। मनुष्य का स्वभाव बड़ा चंचल होता है, यदि कई व्यक्तियों अथवा लोकतंत्र का शासन होगा, तो इसमें अधिक व्यक्तियों के कारण अत्यधिक चपलता और अस्थिरता रहेगी। एक व्यक्ति के हाथ में शासन रहने से अस्थिरता अधिक नहीं बढ़ पाती।
कानून— हॉब्स का मानना है कि सम्प्रभुता का स्वरूप वैधानिक संप्रभुता का स्वरूप है, अतः उसका संप्रभु कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं है। कानून को परिभाषित करते हुए हॉब्स महोदय ने लिखा है कि, “वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है, जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। ” अतः उसकी संप्रभुता दूसरों को आदेश देने की शक्ति है। उनका मानना है कि, “कानून संप्रभु का आदेश है।” इस प्रकार हॉब्स कानून की विधिशास्त्रीयस व्याख्या करता है और राज्यादेशों के अतिरिक्त और किसी को कानून नहीं मानता। यह प्राकृतिक कानून, रीति-रिवाज और दैवी कानून को कानून के रूप में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका कहना है कि ये सब इसीलिए समाज में कानून के रूप में मान्य होते हैं, क्योंकि उन्हें संप्रभु का समर्थन प्राप्त होता है। संप्रभुता के समर्थन की अनुपस्थिति में कानून के रूप में इसका कोई स्थान नहीं होता है।
राज्य और चर्च— थॉमस हॉब्स महोदय चर्च को राज्य के नियंत्रण में रखने के पक्षधर थे। स्वतंत्र चर्च के होने का अर्थ है राज्य का प्रतिद्वन्द्वी होना जबकि प्रभुत्व पूर्ण राज्य में ऐसा नहीं हो सकता। हॉब्स ने धार्मिक सत्ता को पूर्णतः राजसत्ता के वंशवर्ती माना है और संप्रभु के कानूनों के ऊपर, शक्तिधारक के रूप में, बाइबिल के नियमों को अस्वीकार किया है। उसने घोषित किया था कि, “यदि धार्मिक विधि-निषेधों, धार्मिक पुस्तकों के सिद्धांत, धर्म तत्वों और चर्च शासन को कोई सत्ता प्राप्त होती है, तो वह प्रभु के द्वारा अधिकृत होती है।” “
थॉमस हॉब्स महोदय ने सार्वभौम जैसी अवधारणा को स्वीकार करते हुए यह लिखा है कि चर्च राज्य के अंतर्गत अनेक निगमों की भाँति है, जिसका एक प्रधान होता है और वह प्रधान राज्य का संप्रभु है । वह धारणा को पूर्णतया भ्रामक मानता है कि चर्च ईश्वर का राज्य है, जिसकी संप्रभुता राज्य की संप्रभुता से पृथक होती है। हारमोन का मानना है कि, “विभिन्न संगठनों में से जो कि राज्य के साथ शक्ति प्रतियोगिता कर सकते हैं, चर्च प्रमुख अपराधी संगठन है । “
हॉब्स महोदय ने लिखा है कि धर्म का आधार अदृष्ट शक्ति का भय है। मनुष्य शाश्वत नरक के भय से काँपता है और आध्यात्मिक सत्ता उसकी इस
कमजोरी का फायदा लेती है। अतः राज्य को इस खतरे से अपनी तथा प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। जो अदृष्ट शक्तियाँ राज्य द्वारा स्वीकृत हैं उनसे भय करना धर्म है और जो अदृष्ट शक्तियाँ राज्य द्वारा स्वीकृत नहीं है उनसे भय का नाम अंधविश्वास है। हॉब्स के अनुसार धर्म ग्रंथ की व्यवस्था करने का एक मात्र उचित अधिकार शासक को ही है राजकीय विधि और दैवी विधि में कोई विरोध नहीं दैवी विधि वही है जिसकी संप्रभु व्याख्या करे। इस प्रकार हॉब्स धर्म को पूर्णरूप से कानून एवं सत्ता के अधीन रखने के पक्ष में था।
व्यक्तिवाद— वास्तव में हॉब्स निरंकुशतावाद का पोषक था परन्तु इस वाद को एक सर्वाधिक राज्य का सिद्धांत नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन घोषित किया है और कहा है कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति की सुरक्षा है। इस तरह हॉब्स पहला विचारक है जिसने व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार को सर्वोपरि सिद्ध किया और यह कहा कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के इस अधिकार की रक्षा करने के लिए हुई है। अतः हॉब्स निरंकुशतावाद की पोषक हाने के साथ-साथ आन्तरिक रूप में व्यक्तिवादी भी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेबाइन का कथन है कि, “संप्रभु की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत जिसके साथ सामान्यता हॉब्स का नाम जोड़ा जाता है, वास्तव में उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक था । ” प्राकृतिक अवस्था में व्यापत अराजकता की स्थिति जिससे की मनुष्य का जीवन निरंतर कष्टमय बना रहता था, का अंत एक सुदृढ़ और निरंकुश सत्ता के द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए वह पूर्णतया व्यक्ति को राज्य की निरंकुशता के अधीन कर देता है। लेकिन यह अधीनता राज्य के हितों को साधने के लिए नहीं वरन् व्यक्ति के हित-साधन के लिए है। मैक्सी के शब्दों में, “हॉब्स का लेवियाथन केवल संप्रभुता के सिद्धांत का और राज्य को एक साधन के रूप में मानने का ग्रंथ नहीं है, वह व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है । “
इस प्रकार हॉब्स की सत्ता व राज्य मानव हेतु और उसका निर्माण लोगों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया और जो निरंकुश सत्त उसके द्वारा उसे प्रदान की गई है उसका उद्देश्य व्यक्तिगत सुरक्षा की प्राप्ति है, क्योंकि हॉब्स यह स्पष्ट कहता है कि अगर संप्रभु सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हो तो नागरिक उसके प्रति अपनी राजभक्ति और निष्ठा को समाप्त कर उसे सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नयी सत्ता को सौंप सकते हैं।
हॉब्स का निरंकुशवाद में लोचकता भी थी। लोग कानून के संरक्षण में स्वतंत्रता को व्यवहार में लाते हैं इन्होंने विधियों का उद्देश्य प्रजाजन के संपूर्ण कार्यों पर रोक लगाना नहीं है बल्कि केवल “उनका निर्देशन करना एवं उन्हें इस तरह रखना है कि वे अपनी अनियंत्रित इच्छाओं, जल्दबाजी अथवा अविवेक के कारण स्वयं को ही आघात पहुँचा लें। विधि उस बाड़े के समान है जिसे यात्रियों को रोकने के लिए नहीं प्रत्युत सन्मार्ग पर रखने के लिए खड़ा किया जाता है।”
अत: हॉब्स ने निरंकुश सत्ता का समर्थन मानव के भय हेतु किया है और इसलिए उसके संबंध में यह कहना उचित है कि वह निरंकुशतावादी होते हुए भी पूर्णत: व्यक्तिवादी हैं डनिंग ने उसकी इस विशेषता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि “उसके सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूलाधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है।”
हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धान्त की आलोचना— हॉब्स के द्वारा रचित ग्रन्थ ‘लेवियाधन’ के विषय में क्लैरेण्डन ने अपना विचार इस प्रकार प्रस्तुत किया है “मैंने कभी कोई पुस्तक ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह विश्वासघात और धर्मद्रोह भरा हो।” हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धान्त की विभिन्न आलोचना हुई जो निम्नलिखित हैं—
(1) मानव स्वभाव की आलोचना— हॉब्स ने मानव के एकाकी पक्ष का चित्रण किया है, जहाँ मानव स्वार्थी, झगड़ालू है उसमें आसुरी प्रवृत्ति है वहाँ उसमें प्रेम, दया, सहानुभूति, सामाजिकता आदि तत्त्व भी पाये जाते हैं। यदि मानव सिर्फ झगड़ालू होता तो वह अब तक लड़-झगड़ कर समाप्त हो गया होता।
(2) प्राकृतिक अवस्था की आलोचना— हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वह यर्थात न होकर काल्पनिक है। इसका इतिहास में प्रमाण नहीं मिलता है। यदि सर्वोत्तम की विजय का सिद्धांत समाज में प्रचलित रहता तो सिर्फ शक्तिशाली ही जिन्दा रहते। मनुष्य प्राकृतिक रूप से समूह बनाकर रहने वाला प्राणी है वह अकेला जीवित नहीं रह सकता है।
(3) समझौता अतार्किक और असंगत— अशिक्षित लोगों ने कैसे इस बात को जाना कि समझौते द्वारा राज्य बनाया जाए तो हमारी समस्याएँ हल हो जायेंगी, जबकि उस समय तक राज्य का नाम भी नहीं था। जंगली मानव का अचानक सामाजिक बनना और उसकी प्रवृत्ति का समझौतावादी होना अतार्किक है। वॉहन ने ठीक लिखा है कि, “जिस प्रकार एक हब्शी अपना रंग नहीं बदल सकता, उसी प्रकार एक रक्त पिपासु व्यक्ति जिनका वर्णन हॉब्स ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में किया है, शांतिप्रिय श्रमिक नहीं बन सकता।” हॉब्स का मानना है कि मनुष्यों ने अपने सारे अधिकार ‘लेवियाथन’ को प्रदान कर दिये जो समझौते का पक्ष नहीं था। फिर भी उसे असीमित सत्ता सौंपी गयी जो जनता के प्रति उदासीन थी। वह बदले में व्यक्तियों को कुछ भी नहीं देता, यह असंगत लगता है। यह समझौता समझौते की भावना के स्थान पर समर्पण की भावना प्रदर्शित करता है।
(4) समझौता एकपक्षीय नहीं हो सकता— थॉमस हॉब्स ने यह स्पष्ट किया था कि व्यक्तियों ने समझौता करके अपने अधिकार को संप्रभु को सौंप दिये और संप्रुभ समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ गलत है, क्योंकि समझौता सदैव दो पक्षों में होता है।
(5) समझौते का आधार उचित नहीं— हॉब्स ने यह माना कि मानव ने स्वार्थ और अपराजकता के भय से समझौता किया। राज्य जैसी उच्च संस्था के लिए ये आधार अनुचित है। राज्य का आधार अनुमति, सद्भावना, सहयोग, सामाजिक हित की भावना स्पष्ट करता है।
(6) राज्य का कार्य पुलिस राज्य तक ही सीमित नहीं— हॉब्स के शब्दों में राज्य के प्रमुख कार्य आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण से देश को बचाना है तथा राज्य का नैतिक, भौतिक, शिक्षा और संस्कृति के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। इस सन्दर्भ में गूच महोदय ने लिखा है कि ‘लेवियाथन’ केवल अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है जो अपने हाथ में डण्डा लिए है…. उसका राज्य अनिवार्य बुराई है, दबाव का यंत्र है स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता का अपरिहार्य साधन नहीं है।
(7) स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन— हॉब्स की निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन अत्यधिक भयंकर है क्योंकि शासक पर कोई नियंत्रण न होने से जनता की स्वतंत्रता जीवन, सम्पत्ति, अधिकार कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। यह समझ में नहीं आता कि व्यक्तियों ने स्वयं इसे कैसे स्वीकार कर लिया ? हॉब्स की आलोचना करते हुए लॉक महोदय ने यह लिखा है कि, “हॉब्स हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि “मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि वे जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों की शरारतों से बचने के लिए शेरों द्वारा निगला जाना अधिक सुरक्षित समझते हैं। “
(8) राज्य तथा सरकार में समता— हॉब्स ने राज्य और सरकार दोनों में कोई भेद स्पष्ट नहीं किया है। उसने राज्य के साथ-साथ सरकार के प्रति विद्रोह को भी अनुचित माना है। विलोबी ने लिखा है कि, “राज्य और सरकार में अंतर न मानना हॉब्स की सबसे बड़ी भूल है । “
(9) जनता द्वारा आलोचना— हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धान्त की आलोचना जनता द्वारा भी किया गया है, क्योंकि इसमें जनता के अधिकारों को संप्रभु की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। लॉस्की के शब्दों में, “हॉब्स ने अधि कारों का जो कानूनी दृष्टिकोण पेश किया है, वह राजनीतिक दर्शन के लिए अपर्याप्त है। “
(10) पादरियों द्वारा आलोचना— सामाजिक समझौता सिद्धान्त की आलोचना पादरियों द्वारा भी किया गया, क्योंकि इसमें राज्य को दैवी संस्था स्वीकार न करके समझौते द्वारा निर्मित संस्था माना गया। “
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here