गृह युद्ध के कारण (Causes of the Civil War )
गृह युद्ध के कारण (Causes of the Civil War )
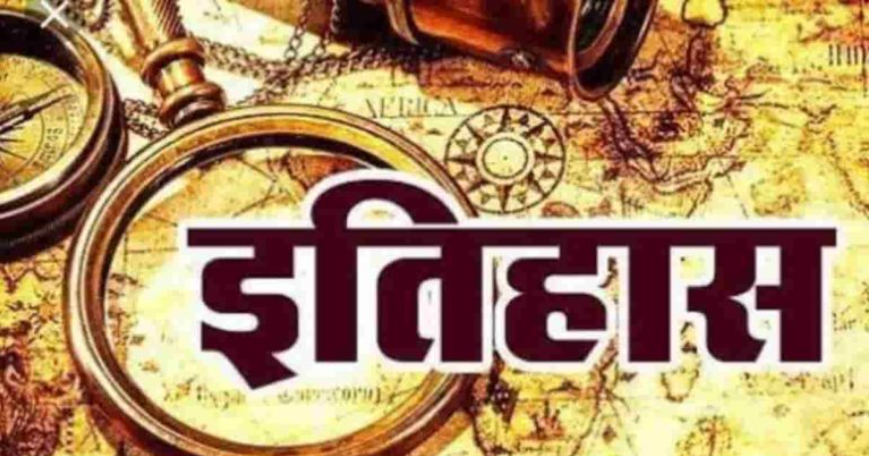
इंग्लैंड में चार वर्षों (सन् 1642 ई. सन् 1646 ई.) तक चले गृहयुद्ध के मौलिक कारणों के विषय में सभी इतिहासकार का एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गृहयुद्ध एक धार्मिक एवं राजनीतिक संघर्ष था। वस्तुतः यह धर्म की आड़ में राजनीतिक और वैधानिक स्वतंत्रता का संघर्ष का मूल कारण सम्प्रभु शक्ति के अस्तित्व का था । वास्तविक सम्प्रभुता राजा में निहित रहे या राजा और संसद दोनों में सम्मिलित रूप से रहे, यही मूल प्रश्न था । विश्वप्रसिद्ध इतिहासकार रास महोदय का मानना है कि युद्ध जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नहीं लड़ा गया था। यद्यपि राजा के विपक्ष में इंग्लैण्ड का काफी प्रभावशाली वर्ग था, तथापि यह कहना अनुचित होगा कि इंग्लैण्ड के राजा ने निरंकुश सत्ता के खिलाफ आवाज उठायी थी। वस्तुतः गृहयुद्ध का कारण संसद के एक शक्तिशाली वर्ग का अपने में विभाजित हो जाना था। युद्ध में संसद के सदस्य और प्यूरिटन दल दोनों एक साथ मिल गए थे, जिसका नेतृत्व पीम और हेम्पडन जैसे शक्तिशाली नेता कर रहे थे, जबकि राजा की ओर से हाइड, फॉकलैंड जैसे संसद के प्रभावशाली सदस्य थे। दोनों पक्षों के बीच कुछ ऐसे धार्मिक मतभेद उत्पन्न हो गये थे। जिसने राजनीतिक मतभेदों को और भी तेज कर दिया था। इन मतभेदों का अन्त करना मात्र युद्ध ही एक विकल्प रह गया था, क्योंकि युद्ध ही राजा के विरूद्ध उन्हें एकता दे सकता था।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध का प्रमुख कारण राजा और प्रजा या राजा और संसद का झगड़ा मात्र नहीं था, बल्कि स्वयं संसद और प्रजा के एक शक्तिशाली वर्ग के पारस्परिक मतभेद थे, जिन्हें समाप्त करने के लिए राजा के विरुद्ध युद्ध करना एक साधन बनाया गया था। अतः इंग्लैंड को अधिकांश जनता युद्ध के प्रति उदासीन थी। चार वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में जनता की सहभागिता कुछ खास नहीं थी।
अतः गृहयुद्ध प्रारंभ होने का कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, बल्कि इसके अनेक कारण जिम्मेदार थे। राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आदशों के सम्बन्ध में राजा के समर्थकों और संसद के समर्थकों के दृष्टिकोण में काफी अन्तर था। दिनोंदिन परिस्थितियाँ बिगड़ती चली गयीं और दोनों ही पक्ष युद्ध के लिए कृतसंकल्प हो चले। इस प्रकार गृहयुद्ध के अनेक कारण थे, जिन्हें हम सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक इन दो भागों में बांट सकते हैं—
सैद्धान्तिक कारण-गृहयुद्ध के सैद्धांतिक कारण निम्नवत थे—
(i) राजा किस आधार से शासन कर सकता है,
(ii) राजा के विशेषाधिकार क्या हैं ? और
(iii) राज्यसत्ता कहाँ निवास करती है ?
व्यावहारिक कारण – गृहयुद्ध के व्यावहारिक कारणों में निम्नलिखित प्रमुख थे—
(i) विदेशी आक्रमण के भय की समाप्ति ।
(ii) जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम की विदेशी नीति की असफलता।
(ii) समाज के विभिन्न वर्गों के पास धन की वृद्धि जबकि राजा के पास धन की कमी मतभेदों में वृद्धि और पारस्परिक प्रतिद्वंदिता।
(iv) दोनों शासकों में अनुभव की कमी एवं नवीन सुधारों की मांग को समझने, पूरा करने या टालने की क्षमता का प्रभाव।
उपर्युक्त वर्णित गृहयुद्ध के कारणों के अलावा इसके अन्य कारण भी जिम्मेदार थे, जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं—
(1) आयरलैंड का विद्रोह— अक्टूबर, 1641 ई. में आयरिश कैथोलिकों ने लगभग पांच हजार प्रोटेस्टेंटो को मौत के घाट उतार दिया। विद्रोहियों ने यह अफवाह भी फैला दी कि चार्ल्स का भी इस घटना में प्रमुख हाथ था। अतः देश के प्रोटेस्टेट का खून खौलने लगा। साथ ही संसद भी राजा के कैथेलिक विरोधी नीति से परिचित हो गई।
(2) पाँच नाइटों का मामला— चार्ल्स प्रथम का विवाह फ्रांस की कैथोलिक राजकुमारी से हुआ था। अतः इंग्लैंड में यह अफवाह फैल गई कि रानी यूरोप से सैनिक मदद लेकर संसद को कुचलवा देगी, अत: चार्ल्स की भाँति उनकी रानी भी संदेह के घेरे में आ गई। कॉमन्स सभा के पाँच सदस्यों ने रानी के कार्यों की आलोचना की थी। उत्तेजित होकर राजा ने स्वयं सैकड़ों सैनिकों के साथ सभा भवन को घेर लिया, उससे पूर्व ही ये सदस्य गण सभा भवन से भाग निकलने में सफल हो चुके थे। इस घटना में संसद सदस्य उत्तेजित हो उठे और अन्त में गृहयुद्ध की ज्वाला भड़क उठी।
(3) चार्ल्स प्रथम का व्यक्तिगत शासन— गृहयुद्ध का एक प्रमुख कारण चार्ल्स प्रथम का व्यक्तिगत शासन भी जिम्मेदार था। चार्ल्स ने लगातार 11 वर्षों तक बिना प्रजा की स्वतंत्रता एवं संसद के सम्मान को गहरी चोट पहुँचायी थी। चार्ल्स प्रथम अपने निरंकुश शासन के जरिए एक बार पुनः देश में दैवी अधिकार के सिद्धांत को पुनर्स्थापित करना चाहता था, अतः देश की प्रति की आशा में बैठी जनता के असंतोष को चार्ल्स ने अपने व्यक्तिगत शासन के जरिए और भी भड़का दिया। स्कॉटलैंड के नेताओं से गुप्त समझौता किए जाने के कारण राजा संसद एवं प्रजा के संदेह के घेरे में आ गया।
(4) निवेदनों की अस्वीकृति— 4 जून सन् 1641 ई. को 19 निवेदन के रूप में संसद ने राजा के समक्ष कार्य कारिणी, न्याय, चर्च एवं सेना के नियंत्रण के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा इस प्रस्ताव को राजा ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के उपरान्त राजा केवल नाम मात्र का शासक रह जाता। इस प्रस्ताव की अस्वीकृति के साथ ही दोनों पक्षों के बीच गृहयुद्ध की आग भड़क गयी।
(5) राजा का चरित्र— ट्यूडर वंशीय शासकों की भाँति स्टुअर्ट वंश के राजाओं के समक्ष कोई आंतरिक एवं वैदेशिक समस्या नहीं रह गई थी । वाणिज्य एवं व्यापार में वृद्धि होने से इंगलैण्ड काफी सम्पन्न हो गया था। दूसरी ओर चार्ल्स प्रथम जिद्दी और अदूरदर्शी था। उन्होंने सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए आवश्यकता से अधिक बुद्धिमता का परिचय दिया। अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण वे शासन के अधिकारी वर्ग को भी संतुष्ट रखने में असफल सिद्ध हुए।
अन्ततः राजा के प्रबल विरोधियों ने व्यक्तिगत शत्रुता को धार्मिक एवं संवैधानिक रूप देकर परिस्थिति को इतना संगीन बना दिया कि राजा और संसद दोनों के मध्य संघर्ष होना स्वाभाविक हो गयसा।
(6) मिलिशिया बिल— गृहयुद्ध में भाग लेने के पूर्व राष्ट्रीय सेना पर नियंत्रण रखना जरूरी था। इसी उद्देश्य से संसद ने मिलिशिया बिल पास किया, जिसे राजा ने स्वीकार नहीं किया। अतः दोनों पक्ष अब युद्ध की तैयारी में पूर्णत: जुट गये।
(7) चार्ल्स प्रथम के सलाहकार— गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण करने में चार्ल्स प्रथम के सलाहकारों का भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। उसके धार्मिक मामलों के सलाहकार विलियम लॉर्ड कैथोलिकों का कट्टर पोषक था। अत: Court of Star Chamber और Court of High Commission में प्यूरिटनों को कुचला जाने लगा जिससे इंग्लैंड में अराजकता में वृद्धि होने लगी। लॉर्ड के भाँति चार्ल्स के असैनिक मामलों के सलाहकार वेण्टवर्थ को अपना कोपभाजक बना डाला। इस तरह चार्ल्स अपने दोनों विवादास्पद व्यक्तित्व वाले सलाहकारों के कारण अपनी प्रसिद्धि को गवां बैठा । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गृहयुद्ध तैयार करने में चार्ल्स प्रथम के सलाहकारों की भूमिका महत्वपूर्ण थी।
(8) सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव— स्टुअर्ट कालीन संसद सदस्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे जिसके कारण वे हठी और अकृतज्ञ थे। स्टुअर्ट राजाओं ने जब देश के धनाढ्यों पर प्रहार करना शुरू किया तो स्वभावतः वे संसद सदस्य राजा के प्रति काफी नाराज हो गए और प्राचीन करों को पुनः लागू करके राजा ने धनी एवं माध्यम वर्ग की सहानुभूति खो दी। विरोध करने वालों को जेल की हवा तक खानी पड़ी। संसद भी अनुचित करों का विरोध करने के लिए कृत संकल्प थी, क्योंकि इसे वह अपने अधिकार का अपहरण व शोषण मानती थी। इस प्रकार आर्थिक प्रश्न प्रजा राजा और संसद के बीच निरन्तर संघर्ष का एक प्रमुख कारण बना।
गृहयुद्ध का प्रमुख कारण इंग्लैण्ड में हुए नवीन धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव भी था। इंग्लैंड के समाज में ट्यूडरकाल से ही कुलीनों के विभिन्न वर्ग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। उनमें धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक सम्मान के प्रश्न पर एक दूसरे के मध्य मतभेद व्याप्त था । एकमात्र राजा का विरोध ही उनहें संगठित कर सकता है। इस प्रकार उनकी पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा से जो सामाजिक तनाव पैदा हो रहा था, उसने भी गृहयुद्ध का मार्ग खोलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संसद में उनके सदस्यों की संख्या बढ़ जाने की वजह से संसद को राजा से संघर्ष करने का एक साधन बना लिया।
(9) राजा के विशेषाधिकार और संसद की सुविधा का प्रश्न— ट्यूटर कालीन संसदों ने ही राजाओं को विशेषाधिकार देने और उन्हें निरंकुश शासक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, परन्तु राजा के निरंकुश के विरोध की शक्ति ट्यूडर कालीन संसद में नहीं थी। दूसरी ओर राजा ने भी अपने विशेषाधि कारों का प्रयोग संसद की प्रतिष्ठा एवं जनहित को देखते हुए किया। अतः तत्कालीन राजा और पार्लियामेंट दोनो के मध्य कोई विरोध पैदा नहीं हुआ था, लेकिन स्टुअर्ट कालीन राजाओं ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग अध भीरता पूर्वक करना प्रारंभ किया। उन्होंने जनता पर नये-नये करों का बोझ लादना शुरू किया और वे न्यायिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। मंत्रियों को नियुक्ति एवं पदच्युति में भी राजा स्वतंत्र होने लगे। इसके अलावा राजाओं ने संसदीय चुनाव और संसद की कार्यवाही तक सुविधा पर भी प्रश्नचिन्ह लगा देते थे। राजा की एक स्वेच्छाचारिता न तो संसद की मर्यादा के अनुकूल थी और न जनहित के हित में ही फलतः संसद अपने अधिकार की रक्षा के लिए काफी जागरूक हो गयी और इन्हें जन समर्थन भी प्राप्त होने लगा। ऐसी स्थिति में दोनों ही पक्षों हेतु अपनी-अपनी सर्वोपरिता सिद्ध करना आवश्यक प्रतीत होने लगा और वे युद्ध हेतु उत्साहित हो गये।
(10) धार्मिक मतभेद— स्टुअर्ट काल में राजा और संसद के बीच परस्पर धार्मिक मतभेद का होना भी गृहयुद्ध का एक प्रमुख कारण था। चर्च का प्रधान राजा ही होता था जिसके कारण धर्म-सुधार राजा के द्वारा ही सम्भव था। अतः प्यूरिटन वर्ग द्वारा राजा के समक्ष धर्म-सुधार का प्रस्ताव रखा गया, जिसे जेम्स प्रथम ने अस्वीकार कर दिया और अन्त में प्यूरिटनों में व्यापक असंतोष व्याप्त हो गया। अब वे संसद के माध्यम से ही अपने धर्म की रक्षा करने के पक्ष में थे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सौभाग्यवश उन दिनों संसद में प्यूरिटनों का ही बोलबाला था। अतः स्वाभाविक रूप से संसद के सदस्य विशप-व्यवस्था के विपक्ष में थे। इंग्लैंड में स्थापित चर्च-व्यवस्था को मिटाने के प्रश्न पर संसद के सदस्य दो सशक्त दलों में बंट गये । यद्यपि संसद के दोनों सदनों द्वारा धर्म- सुधार विल पास नहीं हो पाया, परन्तु इससे संसद की एकता भी भंग हो गयी और गृहयुद्ध होने के लक्षण दिखाई देने लगे। इस प्रकार धार्मिक मतभेद गृहयुद्ध का एक प्रमुख कारण बना।
(11) महान विरोधी पत्र— आयरलैंड के विद्रोह से पार्लियामेंट का राजा के प्रति विश्वास उठ चुका था। अतः उग्रवादियों ने एक महान विरोध-पत्र तैयार किया जिसमें राजा के दुष्कर्मों की सूची, संसद के सुधार और शासन तथा चर्च सम्बन्धी सुधार योजनाओ पर प्रकाश डाल गया था। इस विरोध पत्र के प्रश्न पर संसद में जोरदार बहस हुई। अन्ततः राजा के पक्षधर शक्तिशाली हो गये और अनेक उपायों से संसद के सदस्यों को दबाने का प्रयास करने लगे।
गृहयुद्ध में चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध संसद की विजय के कारण
गृहयुद्ध में चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध संसद की विजय का उल्लेख निम्नवत बिन्दुओं में दिया जा रहा है—
1. चार्ल्स प्रथम की पराजय का सबसे प्रमुख कारण उसकी निरंकुशता थी। उनका 11 वर्षीय अनियंत्रित शासनकाल समाज के निम्न एवं मध्यम वर्ग की जनता के लिए अत्यन्त ही उत्पीड़न था। इसलिए चार्ल्स को गृह युद्ध में आम जनता का सहयोग नहीं मिला।
2 चार्ल्स की सेना के अपेक्षाकृत संसद की सेना में कई योग्य सैन्य अधिकारी थे।
3. राजा की तुलना में युद्ध – संचालन के लिए संसद के पास आय का स्रोत अधिक था। संसद ने समय-समय पर नये-नये कर लगाकर अपनी आय में काफी वृद्धि कर ली थी। यद्यपि राजा की आय के साधन बहुत कम थे। गरीबो का समर्थन प्राप्त होने के कारण वह कोई नया कर नहीं लगा सकता था।
4. बन्दरगाहों पर संसद का अधिकार होने से उसे बाहरी सहायता मिलने में कठिनाई नहीं हुई, जबकि राजा को बाहरी देशों से किसी प्रकार की मदद नहीं प्राप्त हुई।
5. क्रामवेल को नयी आदर्श सेना और ‘बाल मुड़े हुए सैनिकों को संगठित करके संसद की शक्ति में वृद्धि कर दी।
6. संसद के पक्ष में बहुत से राजनीतिज्ञ थे, जिस कारण उसे स्कॉटलैंड से सैनिक सहायता प्राप्त हो सकी थी। यद्यपि राजा को भी आयरिश सहायता प्राप्त थी, किन्तु स्कॉटलैंड की तुलना में उसकी ताकत बिल्कुल नहीं थी।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here